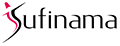लोकगाथा और सूफ़ी प्रेमाख्यान-परशुराम चतुर्वेदी
 Sufinama Archive
June 25, 2020
Sufinama Archive
June 25, 2020
हिन्दी के सूफ़ी-प्रेमाख्यानों का विषय प्रारम्भ से ही लोक-कथाओं जैसा रहता आया था। अतः इन्हें साहित्यिक लोकगाथा मान लेने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। तदनुसार इसके लिए अनेक उपयुक्त लक्षण भी निर्दिष्ट किये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, कहा जा सकता है कि मुल्ला दाऊद से ले कर ईसवी सन् की बीसवीं शताब्दी के कवि नसीर तक सभी ने अपनी-अपनी कृतियों के लिए या तो अपने समय में प्रचलित उन लोक-कहानियों को चुना है जिन्हें लोक-साहित्य का अगभूत होने के कारण लोक-मानस की सृष्टि तक कहा जा सकता है अथवा ऐसी कहानियों के मूल-सूत्र या ढाँचे या वर्णन-शैली मात्र का ही उपयोग कर लिया है। प्रत्येक दशा में उन्होंने इस बात का प्रायः बराबर ध्यान रखा है कि उस कथा को कोई न कोई लोकानुमोदित रूप ही प्रदान किया जाय। इसमें संदेह नहीं कि ऐसी रचनाओं को प्रस्तुत करते समय उन्होंने अपनी कल्पना का भी न्यूनाधिक प्रयोग अवश्य किया होगा और कम से कम उनके पात्रों और स्थानों का नाम-निर्देश करते समय तो उन्होंने बहुत कुछ स्वतंत्रता से भी काम लिया होगा। परन्तु इसके काऱण उनमें कोई विशेष अन्तर नहीं लक्षित होता और न केवल उतने के ही आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि उनमें कोई नवीनता आ गयी है। उनमें विभिन्न कथा-रूढ़ियों का समावेस लगभग पहले जैसा ही होता चला जाता है, चमत्कारपूर्ण प्रसंगों को प्रायः पूर्ववत् ही स्थान मिलता आता है, कई अंधविश्वासों को लगभग उसी प्रकार उदाहृत किया जाता है तथा ऐसी अति-प्राकृतिक बातों का विशद वर्णन भी होता आता है जिन्हें केवल जनसाधारण में ही प्रश्रय मिल सकता है। इसके सिवाय उनके द्वारा किये गये नायकों के असीम साहस एवं ऐश्वर्य के प्रदर्शन, नायिकाओं के अनुपम सौंदर्य के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन तथा विविध घटनाओं के वैचित्र्यपूर्ण विवरण भी इस बात की ही ओर संकेत करते जान पड़ते हैं। अतएव हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम उन साहित्यिक लोकगाथाओं के वास्तविक स्वरूप के विषय में भी कुछ विचार कर लें ।
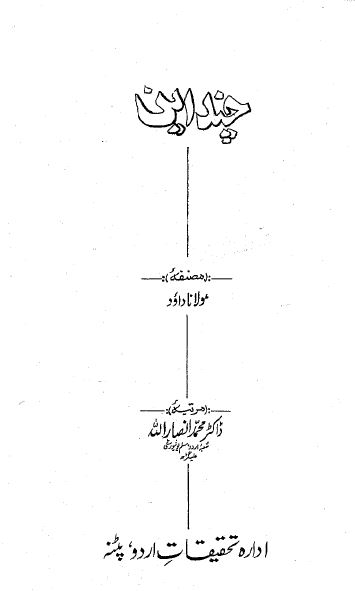
लोकगाथा और बैलेड
‘लोकगाथा’ शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ अधिकतर अंग्रेजी शब्द ‘बैलेड’ के स्थान पर किया जाता रहा है जिसका अर्थ होता है कोई ऐसा काव्य-रूप जिसमें एक सरल कथा केवल साधारण छन्दों द्वारा कह दी गयी हो। ऐसी रचनाएँ प्रायः छोटी-छोटी हुआ करती है। इनमें कथात्मकता के साथ-साथ गीतात्मकता भी पायी जाती है। साधारणतः इनका प्रचार मौखिक रूप में ही चलता आया है। वास्तव में ऐसी रचनाएँ हमें उस प्राचीन कहानी-साहित्य का स्मरण दिलाती हैं जो मानव-मसाज की प्रारम्भिक दशा में प्रचलित रहा होगा। प्रायः ऐसी लोक-गाथाओं के मूल रचयिताओं का पता नहीं चला करता और इसीलिए ये लोक-मानस की उपज तक ठहरा दी जाती हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में यह अनुमान भी किया जा सकता है कि पीछे चल कर कतिपय लोकप्रिय कवि भी ऐसी रचनाओं का निर्माण करने लगे हों। किसी एक ही कथा का देशकालानुसार भिन्न-भिन्न प्रकार से रूपान्तर होने के कारण उसकी अनेक बातें प्रायः घटती बढ़ती भी चली गयी होंगी। यदि कभी किसी दरबारी कवि ने उसकी रचना की होगी तो स्वभावतः उसमें दरबारी जीवन से सम्बद्ध विशिष्ट व्यक्तियों के नाम भी जुड़ गये होंगे। इसके सिवाय रचयिता कवियों के प्रमुख उद्देश्यों के आधार पर भी ऐसी रचनाओं में कुछ न कुछ अन्तर का आ जाना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए, यदि गायक कवि का अभीष्ट किसी के शौर्य को प्रधानता देने का रहा होगा तो उसकी लोकगाथा वीरगाथा बन गयी होगी, यदि किसी प्रेमी-हृदय का परिचय देने का रहा होगा तो वह प्रेमगाथा बन गयी होगी, यदि किसी स्त्री के सतीत्व को महत्व देने का रहा होगा तो वह सतीगाथा बन गयी होगी, तथा यदि केवल भाग्य के फेर का प्रभाव दरसाना रहा होगा तो वह नियतिगाथा बन गयी होगी। परन्तु इसके कारण उनके सामान्य काव्य-रूप में कोई विशेष अन्तर नहीं आ पाया होगा। अधिकतर जन-साधारण में ही उनका प्रचार होते आने के कारण उनमें सदा केवल वैसे ही प्रसंगों का समावेश किया जाता रहा होगा जिनकी ऊपर चर्चा की जा चुकी है। साहित्यिक लोकगाथा (literary ballad) का नाम केवल इसी प्रकार की लोकगाथाओं को दिया जाता आया है।
पँवारा
परन्तु ऐसी दशा में यह आपत्ति की जा सकती है कि यदि ‘लोकगाथा’ शब्द को हम अंग्रेजी शब्द ‘बैलेड’ का अर्थबोधक मानते हैं तो फिर इसके लक्षणों में हमें उसके लघुता, सरलता और गेयत्व आदि जैसे मान्य गुणों की भी गणना करनी चाहिए। किन्तु यदि हम ऐसा मान कर चलते है तो इसका प्रयोग किसी सूफ़ी प्रेमगाथा के लिए तो कम से कम कभी नहीं किया जा सकता। इन रचनाओं में हमें न तो कभी आकार-लाघव की ओर किया गया यत्न ही दीख पड़ता है, और न वाह्य प्रसंगों की वृद्धि में कमी ला कर इनमें जटिलता न आने देने की कोई चेष्टा ही, कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि इसके विपरीत ही प्रयास किया गया है। इसलिए ‘बैलेड’ शब्द का अर्थ हिन्दी में व्यक्त करने के लिए यदि हम चाहें तो ‘गाथागीत’ या ऐसे ही किसी अन्य शब्द का व्यवहार कर सकते हैं। इसके लिए हिन्दी का ‘पँवारा’ शब्द भी उपयुक्त नहीं ठहरता। क्योंकि उसके साथ ‘विस्तार’ का भी जो अर्थ जुड़ा हुआ है वह ‘बैलेड’ की प्रकृति के विरुद्ध जा सकता है। इस ‘पँवारा’ शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द ‘प्रवाद’ से लायी जाती है जिसका अभिप्राय लोकापवाद, बातचीत, काल्पनिक या पौराणिक कथा आदि के रूपों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार यह ‘बैलेड’ की अपेक्षा ‘लोकगाथा’ का ही कहीं अधिक समानार्थक सिद्ध किया जा सकता है। मंझन कवि की ‘मधुमालती’ में जहाँ उसके नायक मनोहर द्वारा अपनी प्रेमपात्री के प्रति कहलाया गया है, “तुम्हारा रूप और मेरा विरह-दुख ये जोनों देश-देशान्तरों तक पहुँच कर पँवारा बन गये हैं, अर्थात् इन दोनों के विषय में लंबी चर्चाएँ की जाने लगी हैं”, वहाँ पर यह शब्द इसी अर्थ का सूचक हो सकता है। परन्तु जहाँ तक पता चलता है, यह साधारणतः केवल किसी ऐसी लोकगाथा की ही ओर संकेत करता है जिसे उपर्युक्त गाथा की संज्ञा दी जाती है। इस दूसरे अर्थ में ही इसका प्रयोग मराठी भाषा के ‘पोवाड़ा’ तथा गुजराती के ‘पँवाड़ो’ जैसे शब्दों के रूपों में भी किया जाता दीख पड़ता है। इसका प्रयोग कभी स्पष्ट रूप में किसी ‘प्रेमगाथा’ के लिए भी किया गया नहीं सुना जाता। मनोहर के मुख से कहलाये गये उक्त वाक्य से भी केवल इतना ही ध्वनित होता है कि दोनों प्रेमियों के सम्बन्ध में ‘विस्तृत चर्चा’ ही प्रचलित है, न कि कोई ‘प्रेमगाथा’ भी। फलतः ‘लोकगाथा’ अंग्रेजी के ‘बैलेड’ से अधिक व्यापक अर्थ सूचित करता प्रतीत होता है और यह ‘पँवारा’ का भी ठीक समानार्थक नहीं जान पड़ता।
रोमांस साहित्य
‘लोकगाथा’ कही जाने वाली रचनाओं का निर्माण स्वभावतः लोक-भाषा में हुआ करता था जिससे उसमें लोक-तत्व की प्रतिष्ठा और भी अधिक सरल थी। इस दृष्टि से विचार करने पर यह अनुमान कर लेना असंगत न होगा कि इसका विकास कदाचित् उसी प्रकार हुआ होगा जिस प्रकार ‘रोमांस’ साहित्य का मध्यकालीन यूरोप में और विशेषतया फ्रांस में हुआ था। अंग्रेजी का ‘रोमांस’ (romance) शब्द वस्तुतः प्राचीन फ्रेंच शब्द ‘रोमाँ’ (Romans) का प्रतिनिधित्व करता है जिसका मूल अर्थ फ्रेंज भाषा अथवा उसमें रचित वे कविताएँ होती थीं जिनका सम्बन्ध ऐतिहासिक वृत्तान्तों से रहता था। उस शब्द का प्रयोग अधिकतर उन देशों की भाषाओं के लिए भी होता आ रहा था जो मूलतः रोमन शासन के अधीन रहते आये थे तथा जिनका मूल-स्रोत लैटिन भाषा रह चुकी थी। कहते हैं कि ईसवी सन् की बारहवीं शताब्दी तक फ्रांस का पूरा साहित्य लैटिन भाषा में रचा जाता था। जब इसके लिए वहाँ की लोक-भाषा का भी प्रयोग किया जाने लगा और इसका विषय ऐतिहासिक वृत्त बन गया तो ऐसी कृतियों को भी उक्त ‘रोमाँ’ नाम ही प्राप्त हो गया। वहॉ आज भी इस शब्द का प्रयोग सम्भवतः ऐसे साहित्य के ही लिए किया जाता है जिसे अंग्रेजी में ‘नॉवेल’ (novel) तथा हिन्दी में ‘उपन्यास’ कहा करते हैं। इनका एक दूसरा रूपान्तरित शब्द ‘रोमांस’ (Romance) आजकल सभी प्रकार के कल्पना-प्रधान साहित्य के लिए प्रयुक्त होने लगा है। वैसे कदाचित् रोमाँ-साहित्य के रचयिताओं की यह धारणा आरम्भ से ही रही कि इसमें कुछ रोचक प्रसंगों का भी समावेश किये बिना इसे यथेष्ट लोकप्रियता नहीं मिल सकती। इसी कारण उन्होंने इसमें ऐतिहासिक वृत्तों के अतिरिक्त पौराणिक कथाओं, लोकवार्ताओं तथा अन्धविश्वासों को भी स्थान देना आरम्भ किया जिसका एक परिणाम यह हुआ कि इनकी ऐतिहासिकता नष्ट होने लग गयी। वास्तव में उस मध्यकालीन समाज की दृष्टि में इतिहास, पौराणिक कथा और काल्पनिक साहित्य के बीच का कोई अन्तर भी स्पष्ट न था। इन कृतियों में अदिकतर दैव पर भरोसा प्रकट किया जाता था और साधु-वृत्तिक कठोर जीवन को महत्व दिया जाता था। उनके चमत्कारों का उल्लेख किया जाता था और भक्ति-भाव के प्रदर्शन में अधिक से अधिक आवेश से काम लिया जाता रहा। इसी प्रकार उस युग के विशिष्ट पात्रों को ऐसे रूपों में चित्रित किया जाता था जिन्हें शूरवीर (chivalrous) कहा जाता है। ऐसी रचनाओं के नायकों का प्रेम सदा अपना कोई विशिष्ट आदर्श लिये रहता था जिसके अनुसार किसी विहित नियम का पालन भी आवश्यक था और जिसका सम्बन्ध न तो यौन-प्रवृत्ती मात्र से था, न जिसे उतना सेवा-मूलक ही कहा जा सकता था। उसमें ऐसी ही सारी बातों का एक मधुर सम्मिश्रण आ जाया करता था जिस कारण ए. बी. टेलर ने उसे ‘कृत्रिम साहित्यिक प्रेम’ (artificial literary love) तक की संज्ञा दे डाली है तथा उसका एक विश्लेषणात्मक परिचय देने का भी यत्न किया है। ऐसे रोमांसों के विषय में उस लेखक ने यह भी कहा है कि इनकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती, प्रत्युत इनके विषय में केवल कुछ अनुभव मात्र किया जा सकता है। कुछ इस प्रकार समझ लिया जा सकता है कि इनके पात्र सर्वसाधारण से कहीं दूर रहने वाले होंगे तथा इनके सम्बन्ध की घटनाएँ भी इस भौतिक जगत् से कहीं ऊपर घटती रही होंगी।

भारतीय सूफ़ी प्रेमाख्यान
हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ भी उपर्युक्त साहित्यिक लोकगाथाओं की रचना करने वाले कुछ इसी प्रकार सोचते रहे होंगे। बल्कि यहाँ ऐसे साहित्य का विषय ऐतिहासिक की अपेक्षा पौराणिक या कथात्मक अधिक होते चलने के कारण उन रचनाकारों के लिए ऐसा करना और भी स्वाभाविक बनता गया होगा। इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यानों के रचयिताओं के सामने कोई ऐसा आदर्श भी उपस्थित हो जिसका अनुसरण करना उन्हें स्वाभाविक जान पड़ता हो। यह विशेषतः उस युग तक प्रचलित उन विशिष्ट अपभ्रंश तथा प्राकृत आख्यानों के रूप में रहा होगा जिनमें से कुछ की रचना का उद्देश्य धार्मिक प्रचार भी रहा हो। सूफ़ी कवियों ने अपनी रचनाओं का ढाँचा अधिकतर इन्ही के अनुरूप खड़ा किया होगा। इन्हीं के आधार पर अनेक प्रचलित कथा-रूढ़ियों का भी उपयोग किया होगा जिस कारण उनकी रचनाओं के अन्तर्गत ये सारी बातें आपसे आप आ गयी होंगी जो इनके लिए सामान्य समझी जा सकती थीं। परन्तु ऐसा करते समय उनका ध्यान सम्भवतः उन फ़ारसी सूफ़ी प्रेमाख्यानों की ओर भी अवश्य आकृष्ट हुआ होगा जिनका निर्माण अधिकतर निज़ामी (मृत्यु सन् 1203 ई.) के समय से होने लगा था और जिनकी कुछ बातों को अपने यहाँ समाविष्ट कर लना उनके लिए स्वाभाविक भी था। उन्होंने इनमें से किस ओर से कितना ग्रहण किया और उस पर कहाँ तक अपनी कल्पना का प्रयोग किया, ये बातें ऐसी है जिनपर अभी तक पूरा अनुसन्धान नहीं किया जा सका है, न इस रोचक प्रश्न को अभी उचित महत्व प्रदान किया गया है। अतएव अभी केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उत्तरी भारत के हिन्दी सूफ़ी प्रेमाख्यानों के लिए कोई न कोई पूर्व-प्रचलित भारतीय रचनादर्श वर्तमान रहने के कारण फ़ारसी-साहित्य का उन पर प्रभाव उतना नहीं पड़ सका जितना दक्खिनी हिन्दी की ऐसी रचनाओं पर पड़ा।
उत्तरी और दक्खिनी सूफ़ी प्रेमाख्यान
परन्तु इसका परिणाम भी केवल इसी रूप में लक्षित होता है कि दक्खिनी हिन्दी के सूफ़ी प्रेमाख्यानों का वाह्य रंग-ढंग उत्तरी भारत की ऐसी रचनाओं से बहुत कुछ भिन्न जान पड़ता है और भाषा-शैली, काव्यरूप एवं छंद-प्रयोग जैसी बातों में वे एक दूसरे के समान नहीं हैं। जहाँ तक वर्ण्य विषय तथा दोनों के कवियों के मूल उद्देश्य का प्रश्न हैं, उनमें बहुत अधिक अन्तर नहीं है। दक्खिन वाले शामी संस्कृति और शामी आदर्शों द्वारा अवश्य अधिक प्रभावित है और उनमें कभी-कभी इस्लामी कट्टरता तक दीख पड़ने लगती है। किन्तु अपनी रचनाओं के अन्तर्गत लोक-तत्व की प्रतिष्ठा करते समय से कभी उत्तर वालों से किसी प्रकार भिन्न नहीं जान पड़ते। ऐसी बातें इन दोनों क्षेत्रों में न केवल भारत से, अपितु अरब एवं ईरान जैसे पश्चिमी देशों से भी ग्रहण कर ली जाती हैं और उनका यथास्थल उपयोग कर लिया जाता है। इनमें यदि कभी प्राचीन बेदुइन अरबों के प्रेम की स्वच्छन्दता दीख पड़ती है तो उसके साथ ही ईरानी प्रेम की आध्यात्मिकता भी दृष्टिगोचर होती है और इन दोनों का संयोग अत्यन्त मनोरम रूप ग्रहण कर लिया करता है। इसके सिवाय जब कभी ये किसी निजन्धरी कथा को अपनाते हैं अथवा उनका अधूरा प्रयोग भी करते हैं तो ये भरसक यही चाहते हैं कि उन्हें उनके मौलिक रूपों में ही चित्रित किया जाय तथा इसके द्वारा अपने पाठकों में कौतूहल की वृद्धि की जाय। परन्तु ऐसा करने में वे एक ही पद्धति नहीं अपनाते। ‘सबरस’ का रचयिता दक्खिनी कवि मुल्ला वजही जहाँ पात्रों और घटनाओं के चित्रण में तथा मूल आदर्शों के निकट बने रहने में विशेष सजगता प्रदर्शित करता है, वहीं ‘हंस जवाहर’ का उत्तरी कवि क़ासिमशाह ऐसा न कर इस प्रकार के वर्णनों पर भारतीय रीति-परम्पराओं की छाप तक डालने लगता है। फिर भी यहाँ पर प्रश्न केवल यह नहीं है कि ऐसी रचनाओं का विषय कहाँ तक अपने मूल आधार का अनुसरण करता है अथवा किस मात्रा में वह मानव-समाज के किसी स्तर-विशेष का प्रतिनिधित्व करता या उसके अनुकूल पड़ता है। यहाँ पर तो हमें यह देखना है कि कहाँ तक ऐसी रचनाओं का विषय स्वभावतः कोई न कोई ऐसा रूप ग्रहण कर लेता है जिसका आकार-प्रकार साधारण जन-मसाज की मानसिक प्रयोगशाला में निर्मित कहा जा सकता हो, और जिसका चित्रण भी साधारण लोक-कथाओं के अनुकूल पड़ सकता हो। इस दृष्टि से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि इन सूफ़ी प्रेमाख्यानों को साहित्यिक लोकगाथा की कोटि में रखना कदाचित् अनुचित न कहा जाएगा और इस बात को उक्त दोनों प्रकार की रचनाओं द्वारा प्रमाणित भी किया जा सकता है।
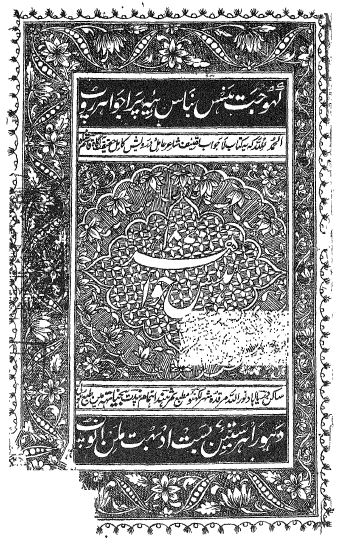
बीसवीं शती का सूफ़ी प्रेमाख्यानः ‘प्रेमदर्पण ’
इस सम्बन्ध में यहाँ पर इनता और भी कहा जा सकता है कि मध्यकालीन यूरोप के रोमांस-साहित्य का एक रूप जहाँ आज की ‘नॉवेल’ कही जाने वाली ऐसी रचनाओं में भी विकसित हो चुका है जिनका उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्य का यथार्थवादी प्रतिपादन रहा करता है, वहाँ दूसरी और हिन्दी के सूफ़ी प्रेमाख्यानों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रेमदर्पण नाम की आज से केवल 45 वर्ष पूर्व निर्मित रचना में भी हमें ऐसी कोई बात लक्षित नहीं होती। इसका कवि नसीर अपने लिए प्रसिद्ध नबी यूसुफ और उसकी प्रेमिका जुलेखा का कथानक चुनता है, उसके आरम्भ में अन्य आराध्यों के प्रति श्रद्धा-भाव प्रकट करने के साथ पौराणिक महापुरुष ख्वाज़ा खिज्र का उल्लेख करता है, तथा ऐनुल अहदी नामक अपने पीर की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है और उसके सम्बन्ध में यहाँ तक कह डालता है कि ‘जिस पानी को वे फूँक देते थे वह केवड़े का जल बन जाया करता था।’ वह बतलाया है कि स्वयं उसे भी ऐसी जल की एक बूँद प्राप्त हुई थी जिसकी सुगन्धि की स्मृति उसे बनी रही। इस रचना के अन्तर्गत कतिपय अन्य ऐसे आत्मकथात्मक प्रसंग अवश्य आ गये हैं जिनका रूप आधुनिक लग सकता है। यदि इसकी तुलना इससे सवा सौ वर्ष पहले इसी विषय पर लिखे गये शेख़ निसार के प्रेमाख्यान ‘यूसुफ़ ज़ुलेखा’ के साथ की जाय तो उस दशा में भी ऐसा अन्तर कुछ न कुछ अवश्य हो जाएगा, किन्तु केवल उसी के कारण इसकी परम्परागत रचना-शैली में कोई स्पष्ट विकास लक्षित नहीं होने पाता, प्रत्यूत ऐसा लगता है कि अभी तक वही पुराना टकसाल काम देता चला आ रहा है जिसकी स्थापना सम्भवतः इससे लगभग छह सौ वर्ष पूर्व हुई थी।
पता नहीं, ‘प्रेमदर्पण’ के बाद भी कोई सूफ़ी प्रेमाख्यान लिखा गया है या नहीं। अतः हमारे पास ऐसा अन्य कोई साधन नहीं है जिसके आधार पर ऐसी रचनाओं के भविष्य का अनुमान लगाया जा सके। उपलब्ध सामग्री पर विचार कर केवल उसके मूल्यांकन से अथवा भावी मानव-समाज के लिए उसकी उपोयगिता पर विचार किया जा सकता है। हिन्दी-भाषा मे इसके निर्माण की परम्परा का आरम्भ उस समय हुआ जब कि हिन्दी में एक ओर केवल फुटकल रनचाओं का और दूसरी ओर पौराणिक ग्रन्थों के अनुवाद- जैसे तथा अपभ्रंश के ‘चरिउ’ या ‘रासो’ के अनुकरण पर प्रबन्ध-कथा का निर्माण किया जा रहा था। इनमें से चरिउ-काव्यों में उनके नायकों के जीवन की घटनाएँ विस्तार के साथ दी जाती थीं। उनके वंश-परिचय, वाल्यावस्था, तीर्थ-भ्रमण, शास्त्राभ्यास, शासन-कार्य, सम्मान एवं देहान्त जैसे विषयों का समावेश कर के, ग्रन्थ का उपसंहार दे दिया जाता था। किन्तु रासो ग्रन्थों के अन्तर्गत अधिकतर उन्हीं बातों की चर्चा की जाती थी जिनका उनके जीवन में विशेष महत्व होता था। इसके सिवाय इन दोनों प्रकार की रचनाओं के अंग-विभाजन में भी कुछ तर होता था, क्योंकि प्रथम श्रेणी की रचनाओं का विभाजन जहाँ सर्गो, संघियों एवं कांडों में पाया जाता है, वहाँ द्वितीय को ठवणि, वाणि आदि में। कभी-कभी तो इनकी अभिनेयता को दृष्टि में रखते हुए इनका विभाजन विभिन्न ‘ढालों’ में भी कर दिया जाता था। गुजराती-लेखक केशवराम शास्त्री के अनुसार बन्ध की दृष्टि से विचार करने पर ऐसे बृहत्काव्यों के केवल दो ही प्रकार मिलते हैं- पहला कड़चा, मासा, ढवणि या ढालयुक्त गेय ‘रासा’ काव्य और दूसरा क्रमबद्ध ‘पवाड़ों’ जिसमें मुख्यतया चौपाई और बीच-बीच में क्वचित् अन्य छंद भी आ गये हों। यह बहुत कुछ हिन्दी के उत्तरी सूफ़ी प्रेमाख्यानों-सा भी लगता है। शास्त्री जी ने अपनी एक पुस्तक में गुजराती साहित्य के अन्तर्गत लोक-कथानकों की चर्चा करते समय किसी भीम कवि की ऐसी ही ‘सदयवत्स कथा’ नामक रचना तथा हीरानंद के ‘विद्याविलास पवाड़ो’ का भी परिचय दिया है। दोनों काव्य मुल्ला दाऊद की ‘चन्दायन’ के समसामयिक जान पड़ते हैं। इनमें से प्रथम का रचना-काल सं. 1466 (सन् 1401 ई.) दिया गया है और दूसरे का सं. 1485 (सन् 1428 ई.) जो सन् 1379 ई. के कुछ ही पीछे आते हैं। शास्त्री जी ने इन दोनों के पहले विजयभद्र सूरि की रचना ‘हंसराज बच्छराज चउपई’ (रचना-काल सं. 1411 अर्थात् सन् 1384 ई.) तथा असाइत नायक-रचित ‘हंसाउलि’ (रचना-काल सं. 1417 अर्थात् 1360 ई.) की भी चर्चा की है जो ‘कथासरित्सागर’ की किसी कथा पर आधारित है।
प्राचीन कथा-रूढ़ियाँ
हिन्दी के इन सूफ़ी प्रेमाख्यानों की रचना के पहले से ही कुछ कथा-रूढ़ियाँ प्रचलित थी जिनका उपयोग अधिकतर लोकगाथाओं में होता आ रहा था और जिन्हें इनके पूर्वर्ती रासो-ग्रन्थों में भी स्थान मिलता आ रहा था। प्रसिद्ध चन्द बरदायी की रचना ‘पृथ्वीराज रासो’ के लिए कहा जाता है कि उसमें ऐसी कथा-रूढ़ियों का प्रवेश उसके प्रारम्भिक रूप की रचना के समय से ही होने लगा होगा, किन्तु यह प्रवृत्त पीछे क्रमश और भी अधिक बढ़ती चली गयी। इसी प्रकार ऐसे रासों-ग्रन्थों में, जिन्हें उनके नायकों के शौर्य-प्रदर्शन के कारण ‘वीरगाथा’ का नाम दिया जाता है, ऐसे अनेक प्रेम-प्रसंगों का भी समावेश किया जाने लगा जिनमें श्रृंगार-रस की अभिव्यक्ति पर्याप्त मात्रा में रहा करती थी और जिन्हें यदि मूल ग्रन्थ से पृथक् कर के कोई स्वतंत्र रूप दे दिया जाय तो एक साधारण ‘प्रेमगाथा’ पुकारा जा सकता है। इनमें प्रदर्शित प्रेमाकर्षण, विरह-वेदना, प्रेमिका के लिए किये गये यत्न और मार्ग में पाये जाने वाले वैसे ही अनेक अंशो के साथ की जा सकती है। जहाँ तक प्रचलित कथा-रूढ़ियों की बात है, इनका समावेश हम उन रचनाओं में भी पाते हैं जिनका उद्देश्य तो प्रत्यक्षतः है जैन-धर्म के माहात्म्य का वृत्तान्त, किन्तु जिनमें प्रासंगिक रूप में प्रेमकथाएँ भी आ जाया करती है। उदाहरण के लिए, ‘ब्रजभाषा के अद्यावधि प्राप्त ग्रंथों में सबसे प्राचीन’ अग्रवाल कवि-रचित ‘प्रद्युम्न-चरित’ (रचना-काल सं. 1411 अर्थात् सन् 1354 ई.) को लिया जा सकता है। इसकी कथा-वस्तु का आधार पौराणिक ठहराया जा सकता है, किन्तु इसके अनेक प्रसंग, जैसे बचपन में ही नायक का माता-पिता से बिछुड़ जाना, अनेक स्त्रियों का उसके प्रति आकृष्ट होना, उसका अनेक साहसिक कार्य करना तथा अन्त में विवाह कर के घर वापस आना आदि, कथा-रूढ़ियों से ही लगते हैं। ऐसी बातें सूफ़ी प्रेमाख्यानों में भी कभी-कभई बहुत विस्तार से पायी जाती है। ‘प्रद्युम्न-चरित’ के नायक को श्रीकृष्ण एवं यादवों के विनाश का समाचार सुन कर जिनेन्द्र से दीक्षा लेना और कठिन तप करना पड़ता है और तब कहीं उसे कैवल्य-पद की प्राप्ति हो पाती है। यह बात सूफ़ी कवियों की दृष्टि में अनावश्यक अवश्य है।
प्रेम-साधनाः प्राक्-सूफ़ी और सूफ़ी
हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यानों में हमे प्रेम-साधना का जो उदाहरण मिलता है उसे सभी ने बहुत महत्व दिया है और यह बात बहुत कुछ निर्विवाद-सी है कि प्रेमा-भक्ति का ऐसा उत्कृष्ट रूप अन्यत्र कहीं कदाचित् ही उपलब्ध हो। इसीलिए अनेक लेखकों की तो यह धारणा-सी बन गयी है कि भारतीय भक्ति-साधना की प्रेम-लक्षणा धारा का काव्य सूफ़ी आदर्श का ही अनुसरण करने वाली होगी। परन्तु यदि हम भारतीय भक्ति के प्रेम-परक पक्ष पर विचार करते हुए उसके मूल स्रोत का पता लगाने का यत्न करें तो हमारे लिए सहता कोई ऐसा मत प्रकट कर देना तर्क-संगत नहीं जान पड़ेगा, न उस दशा में सूफ़ी प्रेम के अन्तर्गत हम कोई नितान्त मौलिक नवीनता ही देख पाएँगे। कम से कम वैष्णव भक्तों द्वारा कल्पित रासलीला की भावन तथा प्रमुख आलवारो की प्रेमा-भक्ति इसके उदाहरण है। यही नहीं, ‘बृहदारण्यक’ जैसी पुरानी उपनिषद् में याज्ञवल्क्य कहते हैं, “स्वयं वह परमात्मा (अकेला) रममाण नहीं हुआ और इसी से एकाकी पुरुष रममाण नहीं होता, उसने दूसरे की इच्छा की। वह, जिस प्रकार परस्पर आलिंगित कोई स्त्री और पुरुष होते हैं वैसे ही परिमाण वाला हो गया और उसने अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर डाला।” ऐसा लगता है कि यह ‘रमणेच्छा’ उस प्रेमावेगपरक भक्ति का आद्य रूप है जिसने आगे चल कर रासलीला की प्रक्रिया में पूरी अभिव्यक्ति पायी। रासलीला की भावना में हमें न केवल क्रीड़ा एवं विनोद मात्र का ही अंश उपलब्ध होता है, प्रत्युत् उसके साथ इसमें हमें उस विरहौत्सुक्य के भी दर्शन होते हैं जिसके कारण श्रीकृष्ण के अकस्मात् अन्तर्हित हो जाने पर उनकी प्रेमिका गोपियाँ उनका क्षणिक विरह भी सहन नहीं कर पाती और सर्वथा अधीर और बावली बन कर इधर-उधर भटकने लग जातीहैं। उन्हें उस ‘बेहोशी’ का भी उवलम्ब नहीं मिल पाता जिसकी दशा में किसी प्रेमी या प्रेमिका को ला कर उसे किंचित् अवकाश प्रदान करने की चेष्टा प्रायः सूफी कवियों द्वारा की गयी देखी जाती है। इसी प्रकार यदि सूफ़ी कवियों के प्रेमी एवं प्रेमिकाओं का प्रेम-भाव उनके किसी पूर्वकालीन मूल सम्बन्ध पर आश्रित माना जाता है तो यहाँ हमारी दृष्टि उपर्युक्त भारतीय धारणा की ओर चली जाती है जिसके अनुसार उन प्रेमिकाओं का प्रेम-पात्र (परमात्मा श्रीकृष्ण) किसी दिन अकेला ‘रममाण’ न हो पाया होगा। इस कारण यहाँ पर भी ‘दैवीपन’ कम कठोर नहीं सिद्ध होता, न हमें यह उससे किसी प्रकार कम अनिवार्य ही लगता है। अतएव किसी वैष्णव की प्रेमा-भक्ति भी, जो रासलीला की भावना का आधार ले कर चलती है और उसकी मधुरोपासना में परिणत होती है, तत्वतः उस इश्क़-हक़ीक़ी की ही कोटि की हो सकती है जो किसी सूफ़ी साधक के यहाँ इश्क़-मजाज़ी के माध्यम से आरम्भ हो कर अन्त में पूर्ण विकास पाता है। प्रेमादर्श की यह स्थिति सहज और स्वाभाविक है और इशके लिए किसी वैवाहिक सम्बन्ध की योजना भी अपेक्षित नहीं। यहाँ न तो परकीया और स्वकीया के अन्तर का कोई प्रश्न उठा करता है न जार एवं धर्मपति के बीच कोई भेद-भाव ही रह जाता है।
निष्कर्ष
जिस समय हिन्दी के सूफ़ी प्रेमाख्यानों की रचना आरम्भ हुई उस समय तक उनके रचियताओं के लिए ऐसी अनेक बातें प्रस्तुत की जा चुकी थीं जिनका वे किसी न किसी रूप में बड़ी सरलता से उपयोग कर सकते थे। क्या कथा-वस्तु, क्या काव्य-रूप, क्या रचना-शैली और कथा-रूढ़ियों जैसी सामग्री, इनमें से कदाचित् किसी के भी लिए उन्हें न तो कोई सर्वथा नवीन मार्ग निर्मित करने की आवश्यकता थी और न अधिक प्रयास ही करने की। जहाँ तक ऐसी रचनाओं के लिए प्रचलित अवधी भाषा के प्रयोग की बात है, हमें पता है कि इस ओर भी कुछ न कुछ कार्य आरम्भ हो चुका था। उनके लिए केवल इतना ही करना शेष था कि यथासम्भव पूर्वागत परम्पराओं का ही अनसुरण करते हुए उस जनप्रिय माध्यम के द्वारा एक ऐसे साहित्य का सूत्रपात कर दें जो न केवल रोचक ही हो बल्कि जिसके द्वारा उनके मत-प्रचार का कार्य भी अग्रसर किया जा सके। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्हें न तो किसी पण्डित-समाज की शरण लेनी थी न किसी के साथ तर्क-वितर्क करने जाना था। वैसे लोगों के प्रति व्यवहार करने का काम तो उनके सहधर्मी एवं संरक्षक शासकों के सिपुर्द था जो चाहे प्रलोभन चाहे प्रताड़न द्वारा अपनी ओर से मनमानी भी कर सकते थे और जिनेक ऊपर इसके विरुद्ध कोई अंकुश भी नहीं हो सकता था। परन्तु सूफ़ी कवियों का काम उनसे कई बातों में भिन्न समझा जा सकता था और वह एक समझौते-जैसा भी था। ये किसी ऐसे मत का परिचय देना चाहते थे जिसकी अनेक बातें सब किसी को प्रत्यक्षतः मान्य एवं स्वीकृतव्य लगें और जिनका मूल आधार एक मात्र परमात्मा तथा उसके प्रति स्वाभाविक प्रेम-भाव होने के कारण बिना आपत्ति के अपनाया जा सके। ऐसी दशा में इसके लिए किसी लोकगाथा को माध्यम बनाना सोने में सुगन्धि डाल देने अथवा किसी अमृत-जैसे अलभ्य पदार्थ को जन-सुलभ पात्रों में ढाल कर सर्वसुलभ बना देने के समान था। स्वभावतः इसे सभी ने पसन्द किया होगा। अतएव इस प्रकार की रचना-शैली की नवीनता यही है कि इसके द्वारा गूढ़ आध्यात्मिक तत्व को भी सुबोध बना देने की चेष्टा की गयी है तथा साथ ही प्रेम-तत्व के उस रूप का निरूपण भी किया गया है जिसके व्यापक क्षेत्र में एक बार प्रवेश पा जाने पर हमारे जीवन में काया-कल्प की दशा लायी जा सकती है तथा भूतल एवं स्वर्ग का भेद-भाव तक दूर किया जा सकता है। इन प्रेमगाथाओं के माध्यम से सूफ़ियों के लिए जन-सम्पर्क स्थापित करना बहुत सरल हो गया और इनकी रचना द्वारा हिन्दी में एक ऐसे साहित्य का सृजन भी आरम्भ हो गया जिसने उसके वाङ्मय की समृद्धि में बहुत बड़ी सहायता की।
साभार – हिन्दुस्तानी पत्रिका अंक -२, खंड -२३, वर्ष -१९६२
Guest Authors
- Aatif Kazmi
- Absar Balkhi
- Afzal Muhammad Farooqui Safvi
- Ahmad Raza Ashrafi
- Ahmer Raza
- Akhlaque Ahan
- Arun Prakash Ray
- Balram Shukla
- Dr. Kabeeruddin Khan Warsi
- Faiz Ali Shah
- Farhat Ehsas
- Iltefat Amjadi
- Jabir Khan Warsi
- Junaid Ahmad Noor
- Kaleem Athar
- Khursheed Alam
- Mazhar Farid
- Meher Murshed
- Mustaquim Pervez
- Qurban Ali
- Raiyan Abulolai
- Rekha Pande
- Saabir Raza Rahbar Misbahi
- Shamim Tariq
- Sharid Ansari
- Shashi Tandon
- Sufinama Archive
- Syed Ali Nadeem Rezavi
- Syed Moin Alvi
- Syed Rizwanullah Wahidi
- Syed Shah Shamimuddin Ahmad Munemi
- Syed Shah Tariq Enayatullah Firdausi
- Umair Husami
- Yusuf Shahab
- Zafarullah Ansari
- Zunnoorain Alavi