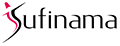अल-ग़ज़ाली की ‘कीमिया ए सआदत’ की तीसरी क़िस्त
 Sufinama Archive
March 12, 2020
Sufinama Archive
March 12, 2020
द्वितीय उल्लास (भगवान् की पहचान)
पहली किरण
शरीर और संसार की वस्तुओं पर विचार करने से भगवान् की पहचान
सन्तों का यह वचन प्रसिद्ध है और उन्होंने यही उपदेश दिया है कि जब तुम अपने-आपको पहचानोगे तभी निःसन्देह भगवान् को भी पहचान सकोगे। प्रभु भी कहते हैं कि जिसने अपने आत्मा और मन को पहचानना है उसी ने भगवान् को भी पहचाना है। इसका कारण यह है कि मनुष्य का हृदय दर्पण के समान है। अतः जो पुरुष इसमें विवेकदृष्टि से देखता है उसे भगवान् का दर्शन प्रत्यक्ष भासने लगता है। तथा सभी लोग जो अपने को तो देखते हैं किन्तु भगवान् को नहीं देख पाते, इसका कारण यह है कि जिस प्रकार सन्तों ने अपने आपको देखना कहा है उस प्रकार वे अपने को नहीं देखते। अतः जिस दृष्टि के द्वारा हृदय-दर्पण में भगवान् की झाँकी की जा सकती है उस दृष्टि का खुलना बहुत आवश्यक है। परन्तु बहुत लोगों की बुद्धि तो इस भेद को समझ ही नहीं सकेगी, इसलिये जिस प्रकार सभी से हृदयंगम कर सके उसी प्रकार इस विषय का वर्णन करता हूँ।
सबसे पहले मनुष्य को अपने स्वरूप की स्थिति से भगवान् की सत्ता का भी निश्चय करना चाहिये तथा अपने गुणों से ही भगवान् के गुणों की भी पहचान कर लेनी चाहिये। उसे देखना चाहिये कि जिस प्रकार इस शरीर और इन्द्रियवर्ग पर जीव की आज्ञा वर्तती है उसी प्रकार सम्पूर्ण जगत् श्रीभगवान् के अनुशासन में चल रहा है। मनुष्य यह देखे कि कितने समय से मैं विद्यमान हूँ, उससे पहले तो मेरा नाम या रूप कुछ भी नहीं था। साथ ही इस बात पर भी विचार करे कि मेरी आदि-उत्पत्ति का बीज तो वीर्य ही है, जो जल की एक मलिन बूँद ही है। उसमें बुद्धि, श्रवण, नेत्र, शिर, हाथ, पैर, रसना, अस्थि, नाड़ी या त्वचा कुछ भी न था। बस, केवल सफेद जल ही था। उसी से इस शरीर में अनेकों आश्चर्य उत्पन्न हो गये! सो ये सब क्या शरीर ने स्वयं ही बना लिये है, या इनका बनाने वाला कोई और है। अच्छा, यदि यह स्वयं ही सब कुछ बना लेता है तो अब तो यह मनुष्य बुद्धि और इन्द्रिय आदि सभी अंगों से सम्पन्न है, किन्तु एक बाल भी नहीं बना सकता, फिर जिस अवस्था में यह केवल वीर्य की एक गन्दी बूँद के ही आकार में था उस समय कैसे बना सकता था? इस प्रकार अपनी उत्पत्ति पर विचार करने से यह मनुष्य सहज ही में अपने उत्पत्तिकर्ता प्रभु को पहचान सकता है।
और जब यह मनुष्य अपने आश्चर्यमय अंगों की ओर देखे तो इसे सहज ही में भगवान की विलक्षण बुद्धि का परिचय मिल सकता है। साथ ही वह देखेगा कि प्रभु ऐसे समर्थ है कि जिस प्रकार जिस वस्तु को उत्पन्न करना चाहें उसी प्रकार कर सकते हैं। भला इससे बढ़कर उनके बल का और क्या वर्णन किया जा सकता है कि उन्होंने जल की एक मिलन बूँद से ऐसा सुन्दर शरीर रच डाला और उसमें ऐसी आश्चर्यमयी इन्द्रियाँ बना दीं। इस प्रकार यदि यह मनुष्य अपने स्वभावों और इन्द्रियों के कर्मों को परखने लगे, तो वह यह जान सकेगा कि भगवान् ने एक-एक अंग कैसे महत्व के बनाये हैं। इस शरीर के हाथ, पाँव जिह्वा, नेत्र और दाँत आदि बाह्य तथा हृदय, मन एवं प्राण आदि आन्तरिक अंगों की उत्पत्ति और विशेषताओं के द्वारा वह इन्हें उत्पन्न करने वाले भगवान् की विद्या को समझे और देखे कि उनकी विद्या कैसी असीम और सम्पूर्ण पदार्थों को विषय करने वाली है कि उनसे कोई भी वस्तु छिपी नहीं रह सकती। यदि सारे बुद्धिमान् मिलकर विचार करे और किसी अंग को अन्य प्रकार से बनाना चाहें तो अन्त में वे उसे उसी रूप में रखना सबसे अच्छा मानेंगे जिसमें कि उसे भगवान् ने बनाया है, उसका कोई दूसरा रूप न्हें उचित न जान पड़ेगा।
अब इस बात को स्पष्टतया समझने के लिये कुछ अंगों की रचना पर विचार किया जाता है। पहले दाँतों को लीजिये। इनमें अगले दाँतों के सिरे तीखे बनाये गये हैं, जिससे कि वे आहार को पकड़ कर उसके खण्ड-खण्ड कर दे। फिर जो इधर-उधर की दाढ़े हैं वे अपने चौड़े सिरों से चक्की की तरह आहार को पीसती है। चक्की में बीच की नली द्वारा जैसे अनाज इकट्ठा रहता है उसी प्रकार रसना ग्रास को इकट्ठा करके दाँतों के नीचे दबाती रहती है। जिह्वा के नीचे ही एक सरोवर-सा है, जिससे लार ले कर वह ग्रास को भिगोती रहती है। यह भिगोना भी आवश्यकता के अनुसार होता है, जिससे ग्रास सूखे नहीं और कोमल होकर कण्ठ से नीचे उतर जाय। अब, सारे बुद्धिमान मिलकर भी यदि भगवान् की इस आश्चर्यमयी रचना से किसी अन्य प्रकार की रचना करनी चाहें तो इससे बढ़कर नहीं बना सकते। अतः भगवान् ने जैसा बना दिया है उसी में सबसे बढ़कर भलाई और सुन्दरता है। देखो, हाथ में पाँच अँगुलियाँ है, इसमें चार का स्वभाव तो एक है और पाँचवाँ जो अँगूठा है उसका स्वभाव कुछ दूसरे प्रकार का है। इसकी लम्बाई कम है, यह सब अँगुलियों के ऊपर घूम सकता है और उनके काम में सहयोग दे सकता है। सब अँगुलियों में तीन-तीन जोड़ है, किन्तु अँगुठों में दो हैं। अतः यह इतना दृढ़ है कि जब आवश्यकता हो तभी सब अँगुलियों को समेट कर मुट्ठी बाँध लेता है और उसे खोल भी सकता है। यह कभी हाथ को सिकोड़ लेता है और कभी फैला देता है, यही तरह-तरह के शस्त्रों का प्रयोग करता है और कभी हाथ को पात्र की तरह बना लेता है। तात्पर्य यह है कि हाथों की सारी क्रिया अँगूठे के द्वारा ही सिद्ध होती है। अब यदि सारे बुद्धिमान् मिलकर विचार करे कि पाँचों अँगुलियाँ समान होनी चाहिये, अथवा तीन एक ओर और दो दूसरी ओर होनी चाहिये, अथवा छः या चार होनी चाहिये, अथवा अँगुलियों में तीन-तीन जोड़ न रहकर किसी अन्य प्रकार से रहना चाहिये- तो उनकी ये सारी कल्पनाएँ अनुपयुक्त और असुन्दर रहेगी। अतः भगवान् ने जिस अंग को जैसा बनाया है वह उसी प्रकार पूर्ण है। इससे सिद्ध हुआ कि जीव को उत्पन्न करने वाले प्रभु की विद्या इसके शरीर एवं सभी पदार्थों में भरपूर है और वे सम्पूर्ण जगत् को जानने वाले हैं।
इसी प्रकार इस शरीर के जितने भी अंग है उन सब में ऐसे ही विचित्र गुण और रहस्य भरे हुए हैं। उन्हें जो पुरुष जितना-जितना समझता है उतना-उतना भगवान् की कारीगरी को देखकर चकित होता है। अतः इस पुरुष को अपने अंगों का निरीक्षण करते हुए अपने आहार, वस्त्र और पृथ्वी आदि निवास स्थानों पर भी विचार करना चाहिये। तथा आहार की उत्पत्ति के साथ जो मेघ, पवन और शीत-उष्ण आदि का जो सम्बन्ध रखा गया है उसे भी परकना चाहिये। देखो, भगवान् ने खानियाँ कैसी आश्चर्य रूप बनायी है, जिनसे लोहा-ताँबा और अनेकों धातुएँ निकलती है और उनके द्वारा अनेकों शस्त्र बनाये जाते हैं। इन शास्त्रों की विद्या और कारीगरी भी अपार है। यदि विचार किया जाये तो संसार में इन सभी पदार्थों की आवश्यकता थी, इसी से श्रीभगवान् ने कृपा करके पहले से ही इन्हें उत्पन्न कर दिया। अहा ! इन्हें उन्होंने कैसी युक्ति से बनाया है और इनमें से एक-एक में कितने-कितने गुण रखे हैं! यदि प्रभु इन्हें पहले ही से न रचते तो मनुष्य तो यह भी नहीं समझ सकते थे कि हमें अमुक पदार्थ चाहिये, उसे हम भगवान् से माँग ले। अतः उन्होंने मनुष्य के आवश्यकता हम भगवान् से माँग ले। अतः उन्होंने मनुष्य के आवश्यकता अनुभव करने और माँगने से पहले ही सब वस्तुएँ उत्पन्न कर दी है और जीवों को इनका उपयोग करने की विद्या दे दी है। इससे भगवान् की परम कृपालुता का परिचय मिलता है और इस संसार पर उनकी जो ऐसी अहैतुकी करुणा है उसे देख-देखकर सब संत आश्चर्यचकित होते है। इसी पर महापुरुष ने कहा है कि जैसे बालक पर माता-पिता की दया होती है उससे भी कहीं बढ़ कर प्रभु की सम्पूर्ण जीवों पर कृपा है।
इस प्रकार हमें जीव की उत्पत्ति से भगवान् की सत्ता का, इसके अंगोपांगों की रचना से उनके पूर्ण सामर्थ्य का तथा इन अंगों के जो नाना प्रकार के गुण और कार्य है उन्हें देखकर प्रभु की महती कृपा का परिचय प्राप्त होता है। इस मनुष्य को कार्य करने के लिये और इस शरीर के सौन्दर्य की दृष्टि से जितने पदार्थों की आवश्यकता थी वे सभी भगवान् ने दिये हैं, कोई भी वस्तु उससे छिपा कर नहीं रखी। इस प्रकार विचार करने से प्रभु की परम कृपा पहचानी जाती है। और इसी दृष्टि से अपने-आपको पहचान को भगवान् की पहचान की कुंजी कहा गया है।
दूसरी किरण
भगवान् की शुद्धता और निर्लेपता की पहचान
इस प्रकार तुम्हें अपने स्वरूप की सत्ता से भगवान् के स्वरूप का तथा अपने गुणों से भगवान् के गुणों का तो परिचय हो ही गया। अब तुम उनकी शुद्धता और निर्लेपता का तात्पर्य समझने का भी प्रयत्न करो। शुद्धता का तात्पर्य यही है कि हमारे मन में जो कुछ संकल्प होता है उसमें तो कुछ-न-कुछ स्थूलता रहती ही है, किन्तु भगवान् उससे सर्वथा शून्य है। अर्थात् उनका वास्तविक स्वरूप संकल्प का विषय नहीं हो सकता। इसके सिवा वे देश और काल से भी सर्वथा निर्लिप्त है। यद्यपि ऐसा कोई स्थान नहीं है जो उनकी सत्ता से रहित हो, तथापि उनके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वे अमुक स्थान में रहते हैं। इस निर्लेपता की पहचान भी अपने ही स्वरूप में हो सकती है। पहले में कह चुका हूँ कि यह जीव चैतन्य स्वरूप है, अतः मन में संकल्प में उस का कोई रंग-रूप नहीं भासता। इसके सिवा वह अमर्यादा, अखण्ड और अरूप भी है और जो वस्तु मर्यादा एवं रूप से रहित होती है उसका स्वरूप संकल्प के अन्तर्गत कभी नहीं आ सकता क्योंकि जिस वस्तु को नेत्रों द्वारा देखा हो अथवा जिसके समान कोई और वस्तु देखी हो उसी का स्वरूप संकल्प के द्वारा जानने की प्रवृत्ति होती है। तात्पर्य यह है कि वस्तु के विषय में जो ऐसी जिज्ञासा हुआ करती है कि वह कैसी है? उसका रूप-रंग कैसा है? उसकी मर्यादा क्या है अर्थात् वह कितनी लम्बी-चौड़ी है? चैतन्यस्वरूप परमात्मा के विषय में ऐसे किसी भी प्रकार के संकल्प का अवकाश नहीं है।
अब, यदि तुम यह प्रश्न करो कि तो फिर वह कैसा है और इस पदार्थ का कोई रंग या रूप ही नहीं उसको सत्य भी कैसे कहा जा सकता है?- तो ऐसा कहना ठीक नहीं। तुम अपने विषय में ही विचार करो, तुम्हारा जो पना चैतन्यस्वरूप है उसकी भी तो कोई मर्यादा या परिमाण नहीं है, उसके स्वरूप का भी तो वर्णन नहीं हो सकता। किन्तु ऐसा होने पर भी यदि तुम अपनी निर्लेपता को समझ सकते हो तो भगवान् के विषय में भी यही समझो कि उनकी निर्लेपता तुम्हारी निर्लेपता से भी बढ़कर है। लोग जो इस बात को सुनकर आश्चर्य मानते हैं और कहते हैं कि जिसका कोई रूप-रंग न हो उसे सत्यस्वरूप कैसे जाने, सो विचार करके देखें तो वे स्वयं भी तो रूप-रंग से रहित और सत्यस्वरूप ही है। यही नहीं, यदि यह मनुष्य विचार करे तो इसे अपने भीतर ही ऐसे अनेकों गुण मिलेंगे जो रूप-रंग से रहित हैं। क्रोध, प्रेम, पीड़ा और सुख-दुःख ये सभी अरूप है। अतः अरूप पदार्थ कैसे सत्य हो सकता है- यह प्रश्न व्यर्थ ही है। यदि मनुष्य राग, सुगन्ध और स्वाद के आकार देखना चाहे तो उन्हें भी तो नहीं देख सकता। इसका कारण यह है कि रूप-रंग की खोज भी मन के संकल्प द्वारा होती है और संकल्प में उसी की मूर्ति स्पष्टतया आ सकती है जिस पदार्थ को नेत्रों द्वारा देखा हो। अतः संकल्प तो नेत्रों द्वारा देखे हुए पदार्थ को ही ढूँढ़ता है। शब्द भी श्रवणेन्द्रिय का ही विषय है, उस तक भी नेत्र की पहुँच नहीं है और न वह उसका कोई रूप-रंग ही देख सकता है। तथा जिस प्रकार शब्द का स्वरूप नेत्रेन्द्रिय की गति से परे है उसी प्रकार रूप-रंग तक श्रवणेन्द्रिय की पहुँच नहीं हो सकती। इस प्रकार अन्य सब इन्द्रियों के विषय भी भिन्न-भिन्न है। नसे भी विलक्षण वे पदार्थ है जिनका ज्ञान केवल बुद्धि से ही होता है, वे किसी भी इन्द्रिय के विषय नहीं होते, अतः इन्द्रियगोचर कहे जाते हैं। परन्तु इस रहस्य को पुरुषार्थ और युक्ति द्वारा समझा जा सकता है। अन्य ग्रन्थों में इसका बहुत विस्तार है, इसलिये यहाँ इसका इतना ही वर्णन पर्याप्त है।
यहाँ हमें मुख्यतया तो यही कहना था कि यह मनुष्य अपनी अरूपता और निराकारता के द्वारा भगवान् की अरूपता और निराकारता को पहचाने। साथ ही यह भी निश्चय करे कि जिस प्रकार रूप-रंग से रहित जीव रूप-रंग युक्त शरीर का राजा है और शरीर उसके द्वारा शासित देश के समान है, उसी प्रकार सम्पूर्ण सृष्टि का स्वामी भगवान् अरूप एवं अनाकार है तथा यह सम्पूर्ण जगत् जो स्थूल और साकार है, उसकी आज्ञा में बर्तता है। इसके सिवा पहले यह कहा जा चुका है कि भगवान् किसी भी स्थान विशेष से बँधे हुए नहीं है। इसी प्रकार यह जीव भी शरीर के हाथ, पाँव या शिर आदि किसी अंगविशेष में नहीं रहता, क्योंकि ये अंग तो सभी खण्डाकार है, और चैतन्यस्वरूप जीव अखण्ड है। अखण्ड वस्तु भला खण्डाकार में कैसे समा सकती है? ऐसा होने पर तो वह भी खण्ड-खण्ड हो जायेगी। अतः यह बड़ा आश्चर्य है कि यद्यपि जीव की सत्ता से बाहर कोई भी अंग नहीं है, सब उसकी सत्ता और आज्ञा के अधीन हैं, तथापि उसे किसी एक स्थान में नहीं कह सकते। इसी प्रकार वे प्रभु भी सम्पूर्ण सृष्टि के स्वामी और निर्लेप हैं, उन्हें पृथ्वी, आकाश या पाताल किसी भी एक स्थान में नहीं कहा जा सकता, तथापि सारा जगत् उन्हीं की सत्ता से विद्यमान है और उन्हीं के अधीन है। अतः भगवान् की शुद्धता और निर्लेपता का पूरा-पूरा रहस्य तभी जाना जा सकता है जब जीव के यथार्थ स्वरूप का बोध हो। प्रभु ने भी कहा है कि मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार रचा है। किन्तु धर्मशास्त्रों में इस रहस्य को गुप्त ही रखा है।
तीसरी किरण
भगवान् और जीव के साम्राज्यों का वर्णन
इस प्रकार भगवान् के स्वरूप, गुण और अरूपता को तुमने समझा तथा उनकी निर्लेपता का भी तुम्हें परिचय हुआ। इससे अब यह भी आवश्यक हो जाता है कि तुम उनके साम्राज्य का भी ज्ञान प्राप्त करो। अतः अब तुम्हें यह श्रवण करना चाहिये कि वे किस प्रकार अपने साम्राज्य का संचालन करते हैं, किस प्रकार समस्त देवताओं को अपनी आज्ञा में चलाते हैं और देवता लोग किस लिये उनके आदेश का अनुवर्तन करते हैं? साथ ही यह भी समझना चाहिये कि भगवान् संसार के कार्यों को किस प्रकार पूरा करते हैं, किस प्रकार भगवद्धाम से उनकी आज्ञा भूलोक में आती है, कैसे वे नक्षत्रमण्डल का संचालन करते हैं, किस प्रकार उन्होंने भूलोक के जीवों की प्रवृत्तियाँ देवताओं के अधीन रखी है और किस प्रकार उनके द्वारा सम्पूर्ण जीवों का पालन-पोषण होता है? इस विद्या के द्वारा भगवल्लीला का परिचय प्राप्त होता है। ग्रन्थों में इसका वर्णन बड़े विस्तार से किया जाता है।
किन्तु यह विद्या भी अपने-आपको पहचानने से ही प्राप्त हो सकती है। जब तक तुम्हें इस बात का ज्ञान न हो कि मैं इस शरीर का किस प्रकार अनुशासन करता हूँ, तब तक जो सम्पूर्ण संसार के सम्राट है उन प्रभु के शासन का भेद तुम कैसे समझ सकोगे? अतः इस बात को समझने के लिये तुम अपने ही एक कर्म पर विचार करो। मान लो, तुम्हारे हृदय में भगवान् का नाम लिखने की इच्छा हुई। यह संकल्प सबसे पहले तुम्हारे हृदय में स्फुरित होगा और फिर मस्तिष्क में जायेगा। जिसको हृदय स्थल कहते हैं वह प्राण की स्थिति का स्थल है, समस्त इन्द्रियों के व्यापार इसी के द्वारा सिद्ध होते हैं। शरीर-विज्ञान वाले तो इस पराणों के स्थान को ही चैतन्य कहते हैं, परन्तु मेरे मत में यह स्थूल, जड़ एवं नाशवान् हैं। मैं जिस हृदय को चैतन्यरूप कहता हूँ वह तो ज्ञान का स्थान है, वह इससे भिन्न अविनाशी है। अस्तु जब संकल्प हृदयस्थान से मस्तिष्क में पहुँचता है तो उस नाम की एक संकल्पमयी मूर्ति बन जाती है। पिर वह मूर्तिमान संकल्प नाड़ियों और माँस-पेशियों को संचालित करता है और उससे प्रेरित होकर अँगुलियाँ लेखनी को चलाती है, जिससे कागज पर अक्षर प्रकट होते हैं और उस नाम की मूर्ति प्रकट हो जाती है। इस प्रकार नाम की जैसी मूर्ति का संकल्प में स्फुरण हुआ था वैसी ही वह इन्द्रियों के द्वारा कागज पर प्रकट होती है। सो जैसे इसके प्राकट्य में तुम्हारी इच्छा ही मूल कारण है। उसी प्रकार इस जगत् की रचना का मूल कारण भी भगवान् की इच्छा ही है। जैसे वह इच्छा तुम्हारे हृदयदेश में स्फुरित हुई थी वैसे ही भगवदिच्छा का स्फुरण ईश्वर सत्ता में होता है। फिर जैसे तुम्हारी इच्छा मस्तिष्क में जाती है वैसे ही भगवदिच्छा ईश्वर से देवताओं को प्राप्त होती है। तुम्हारी इच्छा की जैसे संकल्प में मूर्ति बनती है उसी के अनुसार वह कागज पर अक्षरों के रूप में प्रकट होती है। उसी प्रकार भगवदिच्छा सबसे पहले महत्त्वरूप से मूर्तिमती होती है और फिर देवताओं की प्रेरणा से पंचभूतों के रूप में स्थूल रूप धारण करती है। वात पित्त, कफ भी भूतों के ही स्वभाव हैं। अतः जैसे कलम के द्वारा अक्षर प्रकट होते हैं वैसे ही इन तीनों के मेल से नाना प्रकार के शरीर उत्पन्न हो जाते हैं। कलम का काम तो यही था कि उसके द्वारा कागज पर तुम्हारे आदि संकल्प की मूर्ति प्रकट हो गयी, उसी प्रकार यहाँ पंचभूतों का कार्य भी इतना ही है कि उनके द्वारा देवताओं की प्रेरणा से अनेक प्रकार के शरीर और वनस्पति आदि उत्पन्न हो जाते हैं। पहले जैसे मस्तिष्क में ही भगवन्नाम की मूर्ति निश्चित हो जाती है और वही नाड़ियों एवं अँगुलियों के द्वारा कागज पर प्रकट होती है, उसी प्रकार यह सारी रचना पहले भगवान् के आदि-संकेत के अनुसार महत्तत्वरूप से हो लेती है और वही क्रमशः जगत् रूप में आविर्भूत होती है। जिस प्रकार तुम्हारी चेतना का स्थान हृदय है और उसी से सारी क्रियाएँ सिद्ध होती हैं, उसी प्रकार भगवदिच्छा का आदि स्थान ईश्वर है, उसी से सम्पूर्ण देवताओं को भी बल प्राप्त होता है और उसी की सत्ता से संसार का सारा व्यवहार सिद्ध होता है। इस प्रकार जीव और ईश्वर के साम्राज्यों में कोई भी अन्तर नहीं है, किन्तु इस रहस्य को वही समझ सकता है जिसके बुद्धिरूप नेत्र खुले हैं। किन्तु इस रहस्य को वही समझ सकता है जिसके बुद्धिरूप नेत्र खुले हैं। भगवान् ने भी कहा है कि मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया है। किन्तु यह बात तुम निश्चित जानो कि जिस प्रकार राजाओं के भेद को कोई राजा ही जानता है उसी प्रकार राजाओं के भेद कोई राजा ही जानता है उसी प्रकार भगवान् की लीला के रहस्य को भी महापुरुष ही समझ सकते है सामान्य पुरुषों की वहाँ तक पहुँच नहीं होती।
इस प्रकार भगवान् ने तुम्हें भी एक साम्राज्य दिया है, जिससे इस शरीर रूप देश के राज्य द्वारा तुम उनके साम्राज्य को पहचान सको। अतः तुम उनके इस महान् उपकार पर विचार करो, क्योंकि अपने इस राज्य के द्वारा ही तुम उनके साम्राज्य का भी परिचय प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारे इस राज्य में हृदयस्थान ही बैकुण्ठ है, मस्तिष्क देवलोक है, चित्त महत्त्व है, नेत्रादि इन्द्रियाँ देवता है और सिर आकाश है। तुम्हें तो प्रभु ने रूप-रंग से रहित ही बनाया है और यह जो रूप-रंग वाला शरीर है इसका तुम्हें आधिपत्य दिया है। तुम्हारे लिये उनका आदेश है कि तुम एक पल के लिये भी अपने राज्य से असावधान न रहो, यदि तुम इसकी ओर से अचेत रहोगे तो मुझे भी नहीं पहचान सकोगे। अतः पहले तुम अपने ही को पहचानो।
यहाँ जो कुछ वर्णन किया गया है वह जीव और भगवान् के राज्यों की सूचनामात्र है। यदि इनका सांगोपांग वर्णन किया जाय तब तो बड़ा विस्तार हो जायेगा। इसी प्रकार इस ब्रह्माण्ड और देवताओं के जो पारस्परिक सम्बन्ध एवं देवताओं के जो स्थान और पुरियाँ है उनकी विद्या भी अपार है। इन सबका तात्पर्य यही है कि बुद्धिमान् मनुष्य को इस रहस्य का अनुभव करना चाहिए कि भगवान् इस सम्पूर्ण सृष्टि के स्वामी है। किन्तु जिसका हृदय मलिन होता है वह यह कुछ नहीं समझ सकता। वह तो ऐसा प्रमादी होता है कि से श्री भगवान् के स्वरूप की सुन्दरता और उनकी अतुलित शक्तिमत्ता पर भी विश्वास नहीं होता। कहाँ तक कहें, जीवों की बुद्धि तो ऐसी मलिन हो रही है कि यहाँ जो कुछ वर्णन किया गया है उसे भी वे नहीं समझ पाते, फिर भगवान् के स्वरूप को वे कैसे पहचान सकोगे?
चौथी किरण
शरीरविज्ञानियों और ज्योतिषियों के मतों की समीक्षा तथा भगवान् के राज्य और उनकी व्यवस्था का वर्णन
संसार में जो शरीर-विज्ञान के पण्डित हैं वे तो वात, पित्त, कप को ही मूलतत्व मानते हैं और ज्योतिषी लोगों के मत में हमारी सारी प्रवृत्ति नक्षत्रों के अधीन है। किन्तु इससे इनकी बुद्धि की नन्दता ही सूचित होती है। यह ऐसी ही बात है जैसे कोई व्यक्ति कागज पर लिख रहा हो और उस पर कलम से अक्षरों की आकृतियाँ बनते देखकर कोई मकोड़ा यह समझने लगे कि इन आकृतियों को तो लेखनी ही बनाती है। इसे भले ही बड़ी भारी खोज समझ कर वह कृतकृत्यता का अनुभव करे, परन्तु है यह उसकी अदूरदर्शिता ही। ऐसी ही स्थिति इन शरीर-विज्ञान-वादियों की है। ये आपातदृष्टि से देखकर जड़ वात, पित्त और कफ को ही शरीर का उपादान और उन्हें सब कुछ करने-धरने वाला मानने लगे हैं। ज्योतिषी इनसे कुछ आगे बढ़े हैं। वे उस मकोड़े के समान है जो पहले की अपेक्षा कुछ विशेष बुद्धि रखता है और जिसने ऐसा निश्चय किया है कि ये अक्षर लेखनी की नहीं, अपितु इसे चलाने वाली अँगुलियों की कृति है। अतः ये वात-पित्तादि को नहीं, बल्कि उनके प्रेरक नक्षत्रों को ही सब कुछ करने-धरने वाला मानते हैं। किन्तु है ये भी मन्दगति ही, क्योंकि इनकी दृष्टि अभी नक्षत्रों से आगे उनके प्रेरक देवताओं और देवताओं के भी शासक ईश्वर या भगवान् तक नहीं गयी है।
इसके सिवा भिन्न-भिन्न मतवादियों में आत्मा और अनात्मा के विषय में भी बड़ा मतभेद हैं। उनमें कोई तो ऐसे हैं जो शरीर और प्राणों को ही चैतन्य मानते हैं। नकी दृष्टि तो बहुत ही स्थूल है, चैतन्यतत्व की उपलब्धि का मार्ग उनसे सर्वथा ओझल है। इसी से उनकी बुद्धि शरीर से भिन्न मानते हैं, वे अवश्य चैतन्य के प्रकाश की ओर उन्मुख है। किन्तु इस प्रकाश में भी उत्तरोत्तर अनेकों स्थल है। किन्ही की दृष्टि में वह प्रकाश तारा के समान है, किन्ही की दृष्टि में चन्द्रमा के समान और किन्हीं की दृष्टि में सूर्य के समान। किन्तु इन प्रकाशमय पदों का अनुभव भी उन्हीं को होता है जिनकी बुद्धि की गचि चिदाकाश में है। इस पर खलील नाम के एक संत ने कहा कि जिस प्रभु ने पृथ्वी और आकाश को उत्पन्न किया है। अभी तो उसकी ओर मैंने मुख किया है। और महापुरुष भी कहते हैं कि भगवान् और जीव के बीच में सत्तर-हजार पर्दे हैं, ये निवृत्त हों तो जीव प्रकाश रूप हो जाय। तात्पर्य यह है कि भगवान् के सत्तर हजार पर्दे अर्थात् कलाएँ है और ये सब प्रकाश रूप हैं। सो यदि वे इन सब पर्दों को हटा दे तो निश्चय ही उनका ऐसा प्रकाश हो कि जीव उनके तेज को सहन न कर सके, निश्चय ही उसका मुख भस्म हो जाय।
इन सब वाक्यों का तात्पर्य यही है कि यद्यपि चरम तत्व अत्यन्त दुर्लक्ष्य है तथापि आंशिक सत्य सभी मतों में हैं। शरीर विज्ञानियों ने जो कुछ कहा है वह भी ठीक ही है। उनकी बात तो तभी असत्य हो सकती थी जब वात, पित्त, कफ में भी भगवान् की सत्ता न होती। उनकी भूल तो केवल इतनी ही है कि उनकी इस अत्यन्त निम्नस्तर में ही अल-बुद्धि हो गयी है और उन्होंने इसी को वरम स्थान मान लिया है। अतः उन्हें मन्दमति ही कहा जा सकता है। उन्होंने मानो एक साधारण सेवक को ही राजा मान लिया है, यह नहीं समझा कि ये तो उस महाराज के अत्यन्त तुच्छ टहलुए हैं। इसी प्रकार ज्योतिषियों ने जो जगत् को नक्षत्रों के अधीन कहा है वह भी अशंतः ठीक ही है, क्योंकि यदि नक्षत्रोंम भगवान् की सत्ता न होती तो संसार में रात-दिन का भी भेद न होने पाता। सूर्य भी तो एक विशाल नक्षत्र ही है, उसी के द्वारा रात-दिन और शीत-उष्ण का भेद होता है। सूर्य जब सामने आता है तो दिन होता है और ओझल हो जाने पर रात होती है और जब दूर रहता है तो शीत ऋतु। भगवान् ने ही सूर्य को प्रकाश और उष्णता प्रदान किये हैं। अतः सूर्य उन्हीं को सत्ता से अपना कार्य कर रहा है। इसी प्रकार उन्होंने शुक्र को शीतलता दी है और उसे शोषण करने वाला बनाया है तता एक दूसरे नक्षत्र को उष्ण और सजल रचा है। अतः नक्षत्रों को संसार की प्रवृत्ति का कारण मानना भी धर्म के विरुद्ध नहीं है। ज्योतिषियों को तो इसीलिये भ्रान्त कहा है कि वे नक्षत्रों को ही संसार की प्रवृत्ति का मूल प्रेरक मानते हैं यह नहीं जानते कि ये भी पराधीन है और श्रीभगवान् की आज्ञा से प्रेरित होकर ही अपने-अपने काम में लगे हुए हैं। इनमें स्वयं कोई शक्ति नहीं है। जैसे हाथों को भी भुजा और कन्धों की नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क ही प्रेरित करता है उसी प्रकार ये तारामण्डल और नक्षत्र भी भगवान् की आज्ञा का अनुवर्तन करने वाले तुच्छ टहलुओं के समान ही है।
इस प्रकार यद्यपि आंशिक सत्य शरीर-विज्ञानियों और ज्योतिषियों के मतों में भी है, किन्तु वे वास्तविक रहस्य को नहीं जानते और अपने-अपने मतों का आग्रह करके अपने मत को ही चरम सिद्धान्त समझते हैं। उनके विषय में यह दृष्टान्त पूर्णतया चरितार्थ होता है- किसी स्थान पर कुछ अन्धे रहते थें। उन्होंने सुना कि यहाँ नगर में एक हाथी आया है ।उनकी इच्छा यह जानने की हुई कि हाथी कैसा होता है। अतः वे हाथी के पास जा उसे हाठ से टटोलने लगे। उनमें से किसी का हाथ हाथी की टाँग पर, किसी का दाँत पर, किसी का सूँड पर और किसी का कान पर पड़ा। बस, उन्होंने समझ लिया कि हाथी ऐसी ही है और वे लौटकर परस्पर पूछने लगे कि भाई! हाथी कैसा था? उनमें से जिसने हाथी की टाँग पकड़ी थी वह बोला ‘हाथी खम्भे के समान था,’ जिसने दाँत पकड़ा था वह बोला, ‘हाथी मूसल की तरह था,’ जिसने सूँड छुई थी वह कहने लगा कि हाथी अँगरखे की बाहों की तरह था, और जिसने कान पकड़ा था वह बोला, ‘हाथी पंखे की तरह था।’ इस प्रकार मतभेद होने से उनमें खूब वाद-विवाद होने लगा। अब विचार किया जाय तो अंशतः उन सभी का कथन ठीक है, परन्तु वही पूर्ण सत्य नहीं है। इसी प्रकार शरीर विज्ञानियों और ज्योतिषियों ने भी महाराज के तुच्छ टहलुओं को ही उनका अद्भुत सामर्थ्य देखकर महाराज मान लिया है। किन्तु जिन्हें भगवान् ने अपने पास पहुँचने का सीधा रास्ता दिखाया है वे उनकी तुच्छता औऱ पराधीनता को अच्छी तरह समझते हैं औऱ जानते हैं कि जो पराधीनता होता है वह राजा नहीं हो सकता, अतः इन सबके स्वामी तो भगवान् ही हैं।
इसलिये तुम ऐसा समझो कि यह ब्रह्माण्ड एक राजभवन के समान है। उसी का एक कक्ष बैकुण्ठपुरी है जो प्रधान-मंत्री के रहने का स्थान है। इस राज्य के प्रधान-मंत्री भगवान् विष्णु हैं, जो परब्रह्मरूपी महाराज के अत्यन्त समीपवर्ती हैं और सभी जिनके अधीन हैं। उनके निवासस्थान के चारों ओर एक बारहदरी है, ये ही बारह राशियाँ कही जाती है। इनमें से प्रत्येक द्वार पर उस प्रधानमंत्री का एक-एक कर्मचारी रहता है। ये ही बारह राशियों के बारह देवता है। इस बारहदरी के बाहर नवग्रह रूप नौ घुड़सवार घूमते रहते हैं। प्रधान मंत्री की ओर से कर्मचारियों को जो आज्ञा होती है उसे ये भी सुनते हैं। इनके नीचे पंचतत्वरूप पाँच पदाति है। इनकी दृष्टि सर्वदा घुड़सवारों की ओर ही रहती है और ये यही देखते रहते हैं कि उनके द्वारा हमारे लिये महाराज की क्या आज्ञा होती है। इन पदातियों के हाथ में जो पाँच पाश है वे ही बात-पित्तादि कहे गये हैं। उनके द्वारा वे भगवान् की आज्ञा से किन्ही मनुष्यों को तो ऊर्ध्वगति की ओर खींच लेते हैं और किन्हीं को नीचे गिरा देते हैं- किन्हीं को सुखरूप शिरोपाव देते हैं और किन्हीं को दुःखरूप दण्ड देते है। इस प्रकार यद्यपि सुख-दुःख भी भगवान् की प्रेरणा से ही प्राप्त होते हैं, किन्तु संसार में जब किसी मनुष्य को भोगों की ओर से विरस और शोकाकुल-सा देखा जाता है तो वैद्य लोग तो कहते हैं कि इसे वायु रोग है, इसका कारण शीत ऋतु की शुष्कता है, जब तक वसन्त न आवे इसका उपचार नहीं हो सकता और जब उसी को कोई ज्योतिषी देखता है तो वह कहता है कि इसे यह वायु रोग वृहस्पति के कोप से हुआ है, क्योंकि इस समय वृहस्पति और मंगल का विरोध है, अतः जब तक इनका विरोध दूर न हो इसका रोग दूर नहीं हो सकता। सो एक दृष्टि से यद्यपि उनका कथन भी ठीक है, किन्तु उसकी जो भोगों से अरुचि हुई है उसका वास्तविक कारण तो और ही है।
बात वास्तव में यह है कि श्रीभगवान् जिस जीव का उद्धार करना चाहते हैं, उसके पास तुरन्त ही वृहस्पति और मंगल इन दो अश्वारोही दूतों को भेजते हैं। उनकी आज्ञा से वायु-रूप पदाति उस जीव पर शुष्कता रूप पाश डालता है, जिससे उसका चित्त भोगों की ओर से विरक्त हो जाता है। फिर वह शोक-रूपी चाबुक लगाकर उसकी श्रद्धा-रूपी बागडोर खींचता है, जिससे उसका मुख भगवान् के दरबार की ओर हो जाता है। इस रहस्य को शरीर-शास्त्री और ज्योतिषी नहीं समझते, यह विद्या तो सन्तों के अनुभव-रूपी समुद्र में ही छिपी हुई है। सन्तों की विद्या सभी दिशा ओर सभी कार्यों में भरपूर है, अतः वे ग्रह और नक्षत्रों की गति को भी पहचानते हैं और यह भी जानते हैं कि वे भी भगवान् की आज्ञा पाकर ही किसी जीव को उटाते और किसी को गिराते हैं। तथापि वैद्य और ज्योतिषियों का कथन भी ठीक है, यद्यपि वे महाराज, प्रधान-मंत्री और सेनापति को नहीं जानते। वे नहीं समझते कि इस रोग और चिन्ता में भी प्रबु की अपार करुणा ही भरी हुई है, क्योंकि वे दुःख, रोग, आपत्ति और दण्ड देकर भी जीव को अपनी ही ओर खींचते हैं। प्रबु का कथन है कि जब सात्विकी पुरुषों को कोई रोग होता है तो मैं उन्हें पीड़ा नहीं देता बल्कि उस दुःख के द्वारा भी मैं अपने प्रियजनों को अपनी ही ओर खींचता हूँ। अतः यह दुःख भी जीवों को मेरी ओर खींच ले जाने वाली रस्सी ही है।
इस प्रकार पहले हमने जीव के स्वरूप की पहचान के विषय में वर्णन किया, और फिर भगवान् के स्वरूप का परिचय कराया। अब भगवान् के राज्य और उनकी व्यवस्था की पहचान करायी है। यह पहचान भी जीव को अपने राज्य और अपनी व्यवस्था की पहचान होने पर ही प्राप्त होती है, इसलिये पहले उल्लास में अपने-आपको पहचान का ही वर्णन किया गया है।
पाँचवीं किरण
भगवत्स्तुतिपरक चार वाक्यों का विवरण
यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान् की स्तुति चार वाक्यों से की गयी है। वे वाक्य हैः-
- भगवान् निर्लेप और शुद्ध है।
- वे सम्पूर्ण जगत् के ईश्वर है।
- भगवान् एक है, उनके समान कोई दूसरा नहीं है।
- वे सबसे बड़े है, और परे से भी परे हैं।
ये चार वाक्य यद्यपि बहुत संक्षिप्त है, तथापि भगवान् की पूर्णता को सूचित करने वाले हैं। तुमने जब अपनी निर्लेपता के द्वारा भगवान् की निर्लेपता को समझा, तब तुम्हें निर्लेपता के अर्थ की पहचान हुई। फिर जब अपने राज्य द्वारा तुम्हें भगवान् के साम्राज्य का परिचय हुआ, और तुमने समझा कि काल, कर्म और स्वभाव सहित जितने देवताओं का सम्बन्ध तुम्हारे साथ है, वे सब ईश्वर के ही अधीन है, तो ‘धन्यवाद के योग्य कौन है’ इस बात का तुम्हें पता लग गया। तुम यह बात जान गये कि ईश्वर के सिवा और कोई सुख देने वाला नहीं, क्योंकि स्वयं कोई भी समर्थ या स्वाधीन नहीं है। अतः जो भी सुख प्राप्त होते है, वे प्रभु का ही उपकार है, और उन्हीं का धन्यवाद करना चाहिये। इस प्रकार जब तुम यह समझ गये कि कोई भी समर्थ नहीं, जब भगवान् के ही अधीन है, तब उपर्युक्त तृतीय वाक्य का तात्पर्य भी तुम्हारी समझ में आ ही गया। अब रहा चौथा वाक्य, उसका तात्पर्य यह समझना चाहिये कि तुम जो ऐसा मानते हो कि मैंने भगवान् को पहचान लिया, सो वास्तव में तुमने उन्हें कुछ भी नहीं पहचाना है, क्योंकि उनकी महत्ता का अर्थ तो यही है कि सारे अनुमानों के द्वारा भी जीव उन्हें वास्तव में नहीं पहचान सकता। बड़े होने का यह अर्थ नहीं समझना चाहिये कि भगवान् अमुक पदार्थ से बड़ा है। क्योंकि वास्तव में उनके सामने तो कोई पदार्थ है ही नहीं। यह जितनी सृष्टि है, वह सब भगवान् के प्रकाश का ही प्रतिबिम्ब है, और उन्हीं की सत्ता से भास रहा है। ऐसी स्थिति में भला, उन्हें किससे बड़ा कहेंगे? जिस प्रकार धूप सूर्य से भिन्न है ही नहीं, तो सूर्य को धूप से बड़ा भी कैसे कहा जायेगा?
अतः भगवान को महत्ता या बड़ाई का अर्थ यही है कि मनुष्य अपनी बुद्धि या अनुमान के द्वारा उन्हें किसी प्रकार नहीं जान सकता। तथा उनकी जो निर्लेपता और शुद्धता है, उसे भी मनुष्य की निर्लेपता के समान समझना अत्यन्त अनुचित है। क्योंकि भगवान् का स्वरूप तो इस सम्पूर्ण भासमान प्रपंच से विलक्षण है, उसे किसी के भी समान नहीं कह सकते। फिर भला यह मनुष्य उसकी क्या समता कर सकता है? भगवान् ऐसी बुद्धि से रक्षा करे, जिसके द्वारा जीव उनके महान् ऐश्वर्य और साम्राज्य को मनुष्य के ऐश्वर्य और राज्य के समान ही जाने, अथवा उनकी विद्या और शक्ति की मनुष्य की विद्या और शक्ति से तुलना करे। यद्यपि पहले हमने भी इसी प्रकार वर्णन किया है, किन्तु वह तो प्रभु के स्वरूप को लक्षित कराने के लिये एक दृष्टान्तमात्र कहा है। उसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि इस प्रकार मनुष्य को भगवान् के विषय में कुछ समझ हो जाय। जैसे कोई बालक किसी बुद्धिमान पुरुष से पूछे कि राज्य कनरे में कैसा सुख मिलता है? और वह कह दे कि जैसा तुझे गेंद-बल्ला खेलने में। बालक इस खेल के सुख से अधिक सुख जानता ही नहीं, इसलिये उसे राज्यसुख को उसके द्वारा लक्षित कराया जाता है। इस दृष्टान्त के सिवा और किसी प्रकार वह उसे समझ भी तो नहीं सकता। किन्तु वास्तव में यह बात सब जानते ही हैं कि इन दोनों सुखों की परस्पर कोई तुलना नहीं हो सकती। हाँ, ‘सुख’ शब्द से दोनों ही एक परिचय दिया जाता है, अतः संज्ञा की एकता होने के कारण बालक को उसका कुछ बोध कराया जा सकता है। इसी प्रकार भगवान् की शुद्धता और निर्लेपता का वर्णन किया है, वह भी मन्दबुद्धि पुरुषों को समझाने के निमित्त से ही है। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भगवान् को पूर्णता को भगवान् के सिवा और कोई नहीं जान सकता।
वास्तव में भगवान् की पहचान का विषय इतना विस्तृत है कि उसका कोई अन्त नहीं है। यहाँ तो भगवान् के प्रति जीव की प्रीति और श्रद्धा बढ़े, इस निमित्त से थोड़ा-सा वर्णन कर दिया है। और इतना ही समझने का मनुष्य अधिकारी भी है। जीव की भलाई तो भगवान् की पहचान और उनकी सेवा-भजन आदि में ही है, जिससे कि मृत्य के समय उसका ध्यान भगवान् की ओर लगा रहे, क्योंकि वे ही जीव की स्थिति के स्थान है, और अन्त में निःसन्देह वहीं इसे पहुँचना है। अतः इसकी भलाई इसी में है कि पहले ही प्रभु में इसका प्रेम हो जाय। प्रभु में जिसकी जितनी अधिक प्रीति होती है, उतना ही उसे उनके दर्शनों में विशेष आनन्द आता है। और जब तक जीव को उनकी पहचान न हो, अथवा भजन की अधिकता न हो, तब तक उसके हृदय में भगवत्प्रेम को प्रगाढ़ता नहीं होती। यह बात तो प्रसिद्ध ही है कि जिस पुरुष के साथ किसी की विशेष प्रीति होती है, उसी का वह अधिक स्मरण करता है, और जिसका अधिक स्मरण किया जाता है, उसी के साथ प्रीति भी दृढ़ होती जाती है। कहते हैं, एक बार संत दाऊद को आकाशवाणी हुई थी कि ‘हे दाऊद! तेरे सब कामों को सिद्ध करने वालों मैं ही हूँ और तेरा प्रयोजन भी मेरे ही साथ है, अतः तू एक क्षण भी मेरे भजन से अचेत मत हो।’
परन्तु इस मनुष्य के हृदय में भजन तभी होता है, जब पहले यह सत्कर्मों में बीते और इसे सत्कर्मों का अवकाश तब मिलता है जब यह संपूर्ण भोग-वासनाओं को त्यागे। अतः पाप-कर्मों को त्यागना ही हृदय की मुक्ति का कारण है, और सत्कर्मों को ग्रहण करने से ही भजन में दृढ़ता होती है। ये दोनों साधन भगवान् के प्रति प्रेम उत्पन्न करने वाले हैं। और उत्तम भोगों का बीज भी भगवान् के प्रेम में ही है। यह जीव शरीर धारी है, अतः यह सभी प्रकार के भोगों से शून्य तो रह नहीं सकता, इसे शरीर निर्वाह के लिये भोजन और वस्त्रों की अपेक्षा तो रहेगी ही। इसलिये इसे विचार में स्थित होकर कर्तव्य कर्म और भोग वासना का विवेक करना चाहिये। विचार की मर्यादा भी दो प्रकार की होती है- एक तो यह कि मनुष्य अपनी बुद्धि और अनुभव के आधार पर ही अपनी मर्यादा का निश्चय करे, और दूसरी यह कि किन्हीं महापुरुष के आश्रित रहकर उनकी आज्ञानुसार आचरण करे। किन्तु अपनी बुद्धि और पुरुषार्थ के आश्रित रहकर मर्यादा में रहना बहुत कठिन है, क्योंकि जीव के हृदय में भोग वासना की इतनी प्रबलता है कि वह इसकी बुद्धि को अन्धा करके यथार्थ मार्ग को इसकी दृष्टि से ओझल कर देती है, और अपने अभीष्ट भोगों को ही पुण्य का रूप देकर सामने ले आती है। अतः इस मनुष्य को अपना आचरण स्वाधीन नहीं रखना चाहिये। किन्हीं महापुरुष को अपना शरीर समर्पित कर देना चाहिये। हाँ, सभी मनुष्य ऐसे नहीं होते, जिन्हें आत्म-समर्पण किया जाय। जो ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न सन्त हों, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार आचरण करे, कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। ऐसा होने पर सहज ही में कल्याण हो सकता है, और यही वास्तव में संतों का सच्चा सेवक होना भी है। इसके विपरीत जो पुरुष अपनी वासनाओं के कारण सन्त की मर्यादा का उल्लंघन करता है, उसकी बुद्धि तत्कला नष्ट हो जाती है। इसी पर प्रभु कहते हैं कि जिस मनुष्य ने मर्यादा का त्याग किया है उसने अपने पर ही अन्याय कर डाला है।
छठी किरण
संतमार्ग से विपरीत चलने वाले सात प्रकार के मूर्खों का वर्णन
जिन लोगों ने अपनी वासनाओं के कारण सन्तों की आज्ञा और मर्यादा को त्यागा है, उनकी स्थितियाँ सात प्रकार की होती हैं। उनका हम क्रमशः वर्णन करते हैं-
पहले- ये ऐसे मूर्ख होते हैं कि इनका भगवान् पर भी विश्वास नहीं होता। ये कहते हैं- ‘भगवान् कल्पनामात्र है। यदि वास्तव में कोई इस जगत् का ईश्वर होता तो उसका भी कुछ रूप-रंग होना चाहिये था। किन्तु ईश्वर का तो कोई रूप-रंग या स्थान-दिशा आदि पाया नहीं जाता, इसलिये वह केवल कल्पना ही है। इस जगत् के कार्य तो तत्त्वों के स्वभाव और नक्षत्रों की प्रेरणा से ही होते हैं।’ इन मूर्खों का मत है कि मनुष्य एवं अन्य जीव तथा नाना प्रकार की रचना जो दिखायी देती है वह ईश्वर के बिना स्वयं ही उत्पन्न हुई है और इसी प्रकार स्थित रहेगी। अथवा इसे तत्वों का स्वभाव ही समझना चाहिये। सो, उनका यह कथन व्यर्थ ही है। वे मूर्ख तो अपने विषय में ही कुछ नहीं जानते, तहब और किसी पदार्थ को क्या जानेंने? उनका कथन ऐसा ही है, जैसे कोई पुरुष लिखे हुए अक्षरों को देखकर कहे कि ये अक्षर तो किसी विद्वान् और समर्थ लेखक के बिना स्वयं ही लिख गये हैं, अथवा अनादिकाल से इनकी मूर्ति इसी प्रकार चली आयी है। सो जिनके बुद्धिरूप नेत्र मूँदे हुए हैं, उन भाग्यहीनों की ही ऐसी दृष्टि हो सकती है। इस विषय में शरीर विज्ञानियों और ज्योतिषियों की भूल का वर्णन तो पहले कर ही चुके हैं।
दूसरे- ये लोग ऐसे मूर्ख है कि परलोक को ही नहीं मानते, और कहते हैं कि मनुष्य भी घास और खेती की तरह ही है। जब यह जीव मरता है तो मूल ही से नष्ट हो जाता है, इसलिये पाप, पुण्य, सुख, दुःख और पताड़ना आदि सब व्यर्थ ही है। इनकी मूर्खता तो देखों कि अपने को भी घास अथवा गधे और बैलों की तरह समझते हैं तथा आत्मा जो चैतन्य और अविनाशी है, उसे नहीं पहचानते। मृत्यु तो केवल शरीर के नाश का ही नाम है, किन्तु ये इस बात को नहीं समझते।
तीसरे- ये लोग भगवान् और परलोक को मानते हैं, परन्तु इनका विश्वास ऐसा शिथिल होता है कि इन्हें सन्तजनों के वाक्यों में विश्वास नहीं होता। ये कहते हैं- ‘भला भगवान को हमारे भजन की क्या आवश्यकता है और हमारे पापाचरण से भी उन्हें क्यों दुःख होता है, क्योंकि भगवान् तो ऐसे समदर्शी है कि उनके लिये तो भजन और पाप में कोई अन्तर है नहीं। फिर भला, वे हमारे भोजन की भी क्या अपेक्षा रखते हैं?’ ये मूर्ख भगवान् के इस कथन पर कोई ध्यान नहीं देते कि जिज्ञासुजन जो पुरुषार्थ और शुभकर्म करते हैं, वह नके मन की पवित्रता के लिये ही होता है। ये भाग्यहीन पुरुष तो यही समझते हैं कि भजन और शुभकर्म भगवान् के लिये किये जाते हैं, अपने कल्याण के लिये नहीं। इनकी यह समझ ऐसी है जैसे कोई रोगी कुपथ्य का त्याग न करे और कहे कि इससे वैद्य की क्या हानि है? ठीक है, इससे वैद्य की तो कोई हानि नहीं है, किन्तु रोगी का तो नाश हो ही जाता है। रोगी का नाश वैद्य की अप्रसन्नता से नहीं, अपितु कुपथ्य ही से होता है। वैद्य तो उसे आरोग्यलाभ का मार्ग दिखाने वाला ही है। इसी प्रकार मलिन स्वभाव बुद्धि के नाश का कारण है और भगवान् के भजन तथा उनकी पहचान से बुद्धि नीरोग होती है।
चौथे- इन मूर्खो का कहना है कि सन्तों ने जो हृदय को भोग और क्रोधादि से शुद्ध करने को कहा है, यह असम्भव है, क्योंकि ये स्वभाव तो मनुष्य को सृष्टि के आरम्भ से ही मिले हुए हैं। उनकी निपृत्ति के लिये प्रयत्न करना तो ऐसा ही है जैसे कोई काले कम्बल को सफेद करना चाहे। ये लोग नहीं जानते कि सन्तों ने तो क्रोध और भोग को अपने अधीन करने को ही कहा है जिससे कि मनुष्य सन्तों की आज्ञा और मर्यादा का उल्लंघन न करे। इसके सिवा उन्होंने जो राजसी-तामसी कर्मों का त्याग करने को कहा है, यह बात तो हो ही सकती है। ऐसी स्थिति तो अनेकों पुरुषों ने प्राप्त की है। महापुरुष ने कहा है कि अन्य पुरुषों की तरह मैं भी क्रोध करता हूँ, परन्तु मेरा हृदय सन्तप्त नहीं होता। प्रबु ने भी ऐसे लोगों की प्रसंसा की है, जिन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त की हो और विजय प्राप्त करने का अर्थ तो यही है कि क्रोध तो हो, किन्तु वह हृदय को सन्तप्त न करे। यदि सर्वथा क्रोध न हो तो उसे क्रोध पर विजय प्राप्त करना भी कैसे कहेंगे?
पाँचवे- ये लोग कहते हैं कि भगवान् तो परम कृपालु और दयालु है। वे हमारे अवगुणों की ओर नहीं देखेंगे। पर यह नहीं जानते कि यद्यपि वे परम दयालु है, तथापि पापियों को दण्ड देने वाले भी है। इस संसार में जो नाना प्रकार के रोग, कष्ट और निर्धनता आदि दुःख है, उन पर इनकी दृष्टि ही नहीं जाती। भगवान् तो निश्चय ही अत्यन्त कृपालु और दयालु है। किन्तु जब तुम अपनी आजीविका के लिये प्रयत्न करते हो तब तुम्हारी यह दृष्टि कहाँ रहती है? यदि उनकी दयालुता में विश्वास हो तो व्यवहार और आजीविका के लिये उद्योग करने की क्या आवश्यकता है? क्योकि प्रभु तो विश्वम्भर हैं। वह तो उद्योग किये बिना ही सबका पालन करने वाले हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पृथ्वी और आकाश के भीतर रहने वाले सम्पूर्ण जीवों का पालन करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। ऐसा कहकर मानो प्रबु ने स्पष्ट ही जीव को व्यावहारिक प्रवृत्ति में पड़ने से रोका है। किन्तु उन्होंने कहीं भी भजन या पुरुषार्थ करने के लिये मना करके उसे परलोक सुधारने का प्रयत्न करने से नहीं रोका ये लोग भगवान् को परम कृपालु समझकर भी यदि माया की तृष्णा नहीं त्याग सकते, तो व्यर्थ ही अपने मुख से परलोक की बातें बनाते हैं, और कहते हैं कि भगवान् हमें क्षमा कर देंगे। वास्तव में ये अपने मन के सिखाये हुए हैं और वासनाओं के दास है। भगवान् की कृपा पर इन्हें कुछ भी विश्वास नहीं है।
छठे- ये लोग व्यर्थ अभिमानी होते हैं। ये कहते हैं कि हमें वह अवस्था प्राप्त हुई है कि पाप हमें स्पर्श नहीं कर सकते। हमारा धर्म तो ऐसा पक्का है कि उसे किसी प्रकार का मल कभी स्पर्श ही नहीं कर सकता।
अधिकतर तो इन लोगों की ऐसी स्थिति होती है कि यदि इनके एक वचन का भी खण्डन कर दिया जाय तो जन्मभर के लिये विरोधी बन जाते हैं, अथवा भोजन के लिये एक ग्रास माँगे और वह न मिले तो इनका हृदय क्रोधान्धकार से भर जाता है। वस्तुतः तो परमपुरुषार्थ में इनकी ऐसी दृढ़ता होती नहीं कि पाप इन के पास न फटक सके, फिर इनका इस प्रकार अभिमान करना कैसे संगत हो सकता है? यदि किसी ने दम्भ और क्रोध के द्वारा ऊपर से वैर-भाव और भोग विलास को दबा भी दिया, और इतने में ही समझने लगा कि मैंने परमपद प्राप्त कर लिया है, तो वह अभिमानी ही कहा जायेगा, क्योंकि सन्तों की अवस्था तो ऐसी हुई है कि जब कभी नसे कोई त्रुटि हो गयी है, तो वे भगवान् के भय से रोने लगे हैं और प्रभु से प्रार्थना करके उसके लिये क्षमा माँगते हैं। जो सच्चे सत्पुरुष हुए हैं, वे तो थोड़े से पाप से भी डरते थे, और मलिनता का सन्देह होने पर शुद्ध अन्न भी त्याग देते थें। फिर इन मूर्खों ने कैसे समझ लिया कि हम मान और भोगों के बन्धन से मुक्त हो गये हैं। इन बुद्धिहीनों की अवस्था उन सन्तों से तो बढ़कर हुई नहीं है। यदि कहो कि सन्तजन भी कर्मों से निर्लिप्त ही थे, उन्होंने जीवों के कल्याण के लिये ही अशुभ कर्म त्यागे थे, तो भी उनकी ही तरह ये लोग लोक-कल्याण के लिये अशुभ कर्मों का त्याग क्यों नहीं करते? इन्हें भी यह समझना चाहिये कि यदि कोई हमारे अशुभ कर्मों को देखेगा तो वह भी धर्म-मार्ग से भ्रष्ट हो जायेगा और उसकी बुद्धि नष्ट हो जायेगी। यदि कहो उनकी बुद्धि नष्ट होने से उन महापुरुषों की भी कोई हानि नहीं होती थी। महापुरुषों के लिये भी व्यवहार की शुद्धि परम आवश्यक है। कहते हैं, महापुरुष के पास सकाम भाव से एक छुहारा आया। उन्होंने उसे मुँह में डाल लिया, किन्तु जब मालूम हुआ तो उसे तुरन्त थूक दिया। भला, वे उसे खा ही लेते तो भी उन्हें क्या पाप लग सकता था, और क्या उससे दूसरे लोगों की हानि होती? किन्तु जब उन्होंने उस छुहारे को खाने में भी हानि देखी तो इन मूर्खों को क्या माँस-मदिरा के सेवन से भी हानि नहीं होगी। विचार करे तो उनकी अपेक्षा इन मूर्खों की स्थिति बढ़ी-चढ़ी तो नहीं है, और न छुहारा खाने के पाप से मांस-मदिरा सेवन का पाप ही कम है। यह कैसे जाना जाय कि उन्हें तो छुहारा खाने से भी पाप लगता था, और इन्हें मांस-मदिरा से भी कोई दोष नहीं होता। इससे निश्चय होता है कि इनकी ऐसी करतूते देखकर माया हँसती है। इन मूर्खों को उसने अपना हास्यास्पद और खिलौना ही बना रक्खा है। बुद्धिमान् लोग जब इनके दम्भों को देखते हैं तो चकित रह जाते हैं। धर्मात्मा पुरुष तो वे ही हैं, जो इस मन को छलरूप जानते हैं। जिस पुरुष ने मन और वासनाओं को अपने अधीन नहीं किया, वह तो महानीच है, कोरा पशु ही है। जिसे अपने मन की चालों का पता ही नहीं लगता, सका अभिमान करना तो व्यर्थ ही है। उसका यह कहना कि मैंने मन को अपने अधीन कर लिया है, कोरी मूर्खता ही है। समें मन को जीतने का कोई लक्षण ही नहीं पाया जाता। मन को जीतने का लक्षण तो यह है कि जीव का कर्म उसकी वासनाओं के द्वारा प्रेरित न हो, अपितु वह सन्तों की आज्ञाओं का अनुसरण करे और सर्वदा अपने को उन्हीं की आज्ञा के अधीन रखे, तभी वह सच्चा कहा जा सकता है। जो पुरुष अपने सयानेपन और चतुराई से निर्दोष बनना चाहता है वह तो मन का दास और झूठा अभिमान करने वाला है, अपने मन का निरीक्षण कभी नहीं छोड़ना चाहिये। जब मनुष्य मन की ओर से निःशक हो जाता है तो अवश्य छला जाता है, और फिर इसे अपने सर्वनाश का भी पता नहीं चलता। इसके सिवा सन्तों के आदेशानुसार आचरण करना तो जिज्ञासुओं का प्रथम कर्तव्य है। इसके बिना तो धर्म की ही दृढ़ता नहीं होती, फिर परमपद पाने की तो सम्भावना ही कहां है? वह तो परे से परे हैं, अतः उसका अबिमान करना ही व्यर्थ है।
सातवें- ये लोग अपनी वासनाओं की प्रबलता से ऊँचे हो जाते हैं। इन्हें अनजान नहीं कह सकते, क्योंकि ये अपने को निर्लेप नहीं समझते। जब मनमाना आचरण करने वाले लोग को कुमार्ग में चलते और तरह-तरह से भोग भोगते देखते हैं, तथा साथ ही यह भी देखते हैं कि वे बड़ी गम्भीर और सूक्ष्म बातें कह कर अपने को संतरूप से प्रकट करते हैं और वेश-भूषा भी संतों का सा ही रखते हैं, तो इनमें भी वैसे ही भोग लम्पटता आ जाती है। ये भोगों की दुःखरूपता को न जानकर कहते हैं, ‘भोग निन्दनीय नहीं है, और न इनमें दुःख ही है।’ इनकी दुःखरुपता तो केवल कथन मात्र ही है। ये लोग पाखण्डियों के संग और मन की वासनाओं के कारण अत्यन्त अचेत और अन्धे से हो जाते हैं, तथा माया का इन पर पूरा अधिकार रहता है। ये केवल बातों से या कहने-सुनने से सीधे नहीं होते, क्योंकि इनकी यह भूल अज्ञानवश नहीं है, ये तो जान-बूझकर बावले हुए हैं, अतः इन के सुधार का उपाय तो केवल राजदण्ड ही है।
इस प्रकार जो सात प्रकार के मूर्ख है, उनकी अवस्थाओं का इतना ही वर्णन पर्याप्त है। यहाँ इनका वर्णन इस उद्देश्य से किया है कि ऐसी अवस्थाएँ या तो अपने मन के कारण होती हैं या सन्तों ने जो भगवत्प्राप्ति का मार्ग बताया है, उससे अचते रहने से। किन्तु किसी भी प्रकार हो, जब हृदय में मूर्खता का स्वभाव दृढ़ हो जाता है तो उसे दूर करना बहुत कठिन होता है। कोई ऐसे मूर्ख भी होते हैं कि अज्ञान और संशय में पड़ कर मनमाने मार्ग से चलते रहते हैं और उसी में अपना गौरव भी समझते हैं, किन्तु जब उनसे कोई प्रश्न किया जाता है तो हक्के-बक्के से रह जाते हैं और कोई उत्तर नहीं दे सकते। साथ ही स्वयं किसी से कुछ पूछते भी नहीं, क्योंकि उनके हृदय में भगवन्मार्ग के प्रति न तो प्रीति ही होती है, और न किसी वचन में शंका ही। वास्तव में शंका भी उसी को होती है, जिसके हृदय में किसी प्रकार की खोज होती है। ऐसे मनुष्यों का उपचार करना बहुत कठिन होता है। ये तो ऐसे रोगी के समान है, जो वैद्य के पास जाकर बेधड़कर अपनी कुटेवों का वर्णन करता है। ऐसे रोगी की चिकित्सा होनी कठिन ही है। ऐसे मूर्खों को यही उपदेश करना चाहिये कि जिस विषय को तुम नहीं समझते उसकी और से अपने को अनजान ही प्रकट करो। बस, इतना विश्वास रक्खो कि तुम भी भगवान् के ही उत्पन्न किये हुए हो और वे सर्वसमर्थ है, जो चाहें वही कर सकते हैं- इस बात में भी कभी सन्देह नहीं करना चाहिये। इस प्रकार जब उनमें कुछ श्रद्धा दिखायी दे तब सन्तों के वचन और युक्तियों द्वारा समझाओं जैसा कि मैंने इस ग्रन्थ में किया है।
ज़ारी
Guest Authors
- Aatif Kazmi
- Absar Balkhi
- Afzal Muhammad Farooqui Safvi
- Ahmad Raza Ashrafi
- Ahmer Raza
- Akhlaque Ahan
- Arun Prakash Ray
- Balram Shukla
- Dr. Kabeeruddin Khan Warsi
- Faiz Ali Shah
- Farhat Ehsas
- Iltefat Amjadi
- Jabir Khan Warsi
- Junaid Ahmad Noor
- Kaleem Athar
- Khursheed Alam
- Mazhar Farid
- Meher Murshed
- Mustaquim Pervez
- Qurban Ali
- Raiyan Abulolai
- Rekha Pande
- Saabir Raza Rahbar Misbahi
- Shamim Tariq
- Sharid Ansari
- Shashi Tandon
- Sufinama Archive
- Syed Ali Nadeem Rezavi
- Syed Moin Alvi
- Syed Rizwanullah Wahidi
- Syed Shah Shamimuddin Ahmad Munemi
- Syed Shah Tariq Enayatullah Firdausi
- Umair Husami
- Yusuf Shahab
- Zafarullah Ansari
- Zunnoorain Alavi