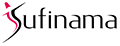हज़रत शाह तुराब अ’ली क़लन्दर और उनका काव्य
 Sufinama
July 10, 2024
Sufinama
July 10, 2024
सूफ़ी-संतों के योगदान को अगर एक वाक्य में लिखना हो तो हम कह सकते हैं कि सूफ़ी और भक्ति संतों ने हिंदुस्तान की गंगा-जमुनी तहज़ीब को नाम दिए हैं। ये नाम गंगा-जमुनी तहज़ीब को जोड़ कर रखने वाली कड़ियाँ हैं। सूफ़ी-संतों ने हिंदुस्तान में गंगा-जमुनी तहज़ीब की आधार-शिला रखी और धीरे-धीरे हिंदुस्तान में साझा संस्कृति की वह विशाल इमारत खड़ी हो गई जो आज दुनिया के लिए मिसाल है। अठारहवी सदी के सूफ़ियों और संतों ने एक और प्रयोग किया जिस ने इस संस्कृति की जड़ों को और मज़बूत बना दिया। इन सूफ़ी-संतों ने मिसालें नहीं गढ़ीं बल्कि अपने आचरण और काव्य से वे स्वयं ही मिसाल बन गए। अठारहवीं सदी आते-आते भक्ति संतों और सूफ़ियों ने अपने उपमान आपस में बदल लिए। भक्ति संतों के काव्य में जहाँ ख़ुदा, महबूब और इश्क़ जैसे शब्दों की भरमार आ गई वहीं सूफ़ी संतों ने कृष्ण, राम, प्रियतम, होली जैसे विशुद्ध हिन्दुस्तानी प्रतिमानों पर जम कर शायरी की। गंगा-जमुनी संस्कृति के पैरहन में सूफ़ी-संतों ने न सिर्फ़ सादगी का ख़याल रखा बल्कि इस में अपने काव्य के जड़ी-गोटे भी लगाए।
अवध का क्षेत्र भी इस आन्दोलन से अछूता नहीं रहा। मलिक मुहम्मद जायसी, हज़रत शाह ख़ादिम सफी, हज़रत शाह काज़िम क़लन्दर और शाह तुराब अली क़लन्दर जैसे सूफ़ियों के कलाम हमें द्वैत और अद्वैत से पार ऐसी दुनिया में पहुंचा देते हैं जहाँ दुई के सारे भेद समाप्त हो जाते हैं।
हज़रत शाह तुराब अली क़लन्दर का जन्म सन् 1767 ई. में लखनऊ के क़रीब काकोरी में हुआ। शाह तुराब अली क़लन्दर के वालिद हज़रत शाह काज़िम क़लन्दर एक महान सूफ़ी बुज़ुर्ग हुए हैं। भगवान श्रीकृष्ण पर उन्होंने कई ठुमरियाँ लिखी हैं जो शांत रस के नाम से प्रकशित हैं। शाह काज़िम क़लन्दर के मुर्शिद हज़रत शाह बासित अली क़लन्दर इलाहाबादी थे। शाह काज़िम कई वर्षों तक इलाहबाद में रहे। बाद में अपने मुर्शिद के आदेश पर काकोरी में ख़ानक़ाह तामीर की। काकोरी की इस ख़ानक़ाह का सिलसिला हज़रत क़ुतुबुद्दीन बीना दिल क़लन्दर, हज़रत नज्मुद्दीन क़लन्दर से होता हुआ हज़रत नूरुद्दीन मुबारक ग़ज़नवी तक पहुँचता है जो हज़रत शैख़ शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी के खलीफ़ा थे।
हज़रत शाह काज़िम क़लन्दर ने ब्रज भाषा में दोहे, ठुमरियाँ, छंद तथा भजन आदि लिखे हैं। उनके कलाम में वहदत-उल-वुजूद उस सादे धागे की तरह प्रतीत होता है जिस धागे से बांध कर शाह काज़िम रंग-बिरंगी ठुमरियों की पतंगें उड़ाते हैं।
शाह तुराब का जन्म ऐसे महान सूफ़ी के घर हुआ था जिनकी ख़ानक़ाह में प्रेम और भक्ति का झरना अनवरत बह रहा था। हज़रत काज़िम क़लन्दर ने शाह तुराब को फ़क़ीरी में मस्त रहना सिखाया। उनका यह शे’र इस की तस्दीक करता है –
तू सब से अपने आप को नाक़िस तुराब समझे जा
यही तो देखते हैं हम बड़ा कमाल तेरा
हज़रत तुराब अली क़लन्दर की प्रारंभिक शिक्षा मुल्ला क़ुदरतुल्लाह बिलग्रामी और मौलाना मुईनुद्दीन बंगाली की देख-रेख में हुई। उन्होंने मौलाना हमीदुद्दीन मुहद्दिस-ए-काकोरवी से हदीस का ज्ञान प्राप्त किया। मौलाना नज्मुद्दीन खाँ ने उन्हें अरूज की शिक्षा दी और मौलाना फ़ज़लुल्लाह ने उन्हें न्यायशास्त्र पढ़ाया।
हज़रत शाह काज़िम क़लन्दर क़स्बा से फ़ासले पर क़ब्रिस्तान में एक छोटे से हुजरे में रहते थे। बारह वर्ष की उम्र से ही शाह तुराब की तौहीद-ए-वुजूदी की शिक्षा प्रारंभ हो गई। शाह तुराब को अपने वालिद के मुरीदों की ख़िदमत करने का आदेश हुआ । दालान पर झाड़ू लगाने का काम भी शाह तुराब के जिम्मे था। पंद्रह साल की उम्र तक शाह तुराब अपने पिता से तर्बियत पाते रहे। सत्रह वर्ष की उम्र में शाह तुराब का ब्याह मुज़फ़्फ़रुद्दौला अबुल बरकात खां की नवासी और मुहम्मद उयूज़ चकलादार शाही की बेटी से हुआ।
हज़रत शाह तुराब, मिर्ज़ा मज़हर जान-ए-जाना, ख़्वाजा मीर दर्द और ख़्वाजा रुक्नुद्दीन इश्क़ के समकालीन थे। यह वो समय था जब मीर-तक़ी मीर और मुसहफ़ी जैसे शायर दिल्ली छोड़ कर लखनऊ आ चुके थे।
शाह तुराब को बचपन से शायरी का शौक़ था। उन्होंने पहले शहीद तख़ल्लुस किया और बाद में तुराब। उनके उर्दू कुल्लियात में शहीद तख़ल्लुस कहीं नहीं मिलता।
शाह तुराब की पहली मसनवी अस्ल-उल-मारिफ़ है। यह मसनवी निहायत आसान ज़बान में लिखी गई है। उनकी उर्दू शायरी को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले हिस्से में वो ग़ज़लें हैं जिन का विषय इश्क़-ए-मजाज़ी है, दूसरे हिस्से में वो ग़ज़लें हैं जिन में इश्क़-ए-मजाज़ी और इश्क़ ए हक़ीक़ी का समावेश है जबकि तीसरे हिस्से में वो ग़ज़लें हैं जिनका विषय तसव्वुफ़ है।
शाह तुराब की शुरूआती ग़ज़लों के कुछ शेर देखिए –
रहता है गम-ए-दिल से मुझे जान का खटका
है अश्क़-ए-रवाँ से मुझे तूफ़ान का खटका
ग़ैर के पास यार बैठ गया
दिल में मेरे गुबार बैठ गया
हज़रत शाह तुराब की शायरी में आगे चलकर तसव्वुफ़ मुख्य विषय बन गया –
निशाँ इस का किसी से कब बयाँ हो
वही पावे निशाँ जो बे-निशाँ हो
मुनज़्ज़ह वो तो हे कौन-ओ-मकाँ से
मकाँ उस को कहाँ जो ला-मकाँ हो
कोई जागह नहीं पर उस से ख़ाली
ज़मीं हो ’अर्श हो या आसमाँ हो
सिवा उस के नहीं कोई जहाँ में
तलाश उस की करो यारो जहाँ हो
‘तुराब’ उस्ताद से मालूम कर लो
तरीक़-ए-मा’रिफ़त गर क़द्र-दाँ हो
हज़रत शाह तुराब अली क़लन्दर फ़ारसी में भी सिद्धहस्त थे। उनका एक फ़ारसी दीवान भी मिलता है जिस की शा’इरी फ़ारसी काव्य-परंपरा की दृष्टि से उत्कृष्ट है-
ऐ बे-ख़बर चे पुर्सी अज़ मज़्हब-ए-क़लंदर
बर-हक़ बुवद अनल-हक़ दर मश्रब-ए-क़लंदर
(ऐ बे-ख़बर! तू क़लंदर के मज़्हब के बारे में क्या पूछ रहा है
क़लंदरों के मश्रब में अनल-हक़ (मैं ख़ुदा हूँ) ही सब कुछ होता है)
अह्ल-ए-हक़ीक़तस्त ऊ क़ाएल ब-वह्दतस्त ऊ
हर्फ़-ए-दुई न-शुनवद कस अज़ लब-ए-क़लंदर
(वो परम सत्य और एकत्व का क़ाइल है
क़लंदर की ज़बान से कोई द्वैत के शब्द नहीं सुन सकता)
हज़रत शाह तुराब अली क़लन्दर ने सन् 1858 ई. में 94 वर्ष की उम्र में जगती के इस पालने को अलविदा कहा और काकोरी में अपने बुज़ुर्गों की ख़ानक़ाह में सुपुर्द-ए-खाक़ हुए।
उनकी प्रमुख किताबें हैं –
1. रिसाला मजमा-उल-फ़वाइद
2. रिसाला फ़त्ह-उल-उनूज़
3. अस्नाद-उल-मशीख़त
4. मुजाहिदात-ए-औलिया
5. कश्फ़-उल-मुतवारी
6. मतालिब-ए-रशीदी
7. और अमृत रस
मुंशी नवल किशोर प्रेस ने उनका दीवान सन्1876 ई. में प्रकाशित किया।
शाह तुराब अली क़लन्दर के उर्दू दीवान से फ़ाल भी निकाला जाता है।उनके शेर का एक मिसरा निकाह फिल्म के प्रसिद्ध गीत में आता है। शे’र यूँ है –
शहर में अपने ये लैला ने मुनादी कर दी
कोई पत्थर से न मारे मिरे दीवाने को
हज़रत शाह तुराब अली क़लन्दर अपनी ठुमरियों के लिए विशेष तौर पर याद किए जाते हैं। इनकी ठुमरियों का संग्रह अमृत रस के नाम से प्रकाशित हो चुका है।
सूफ़ी दर्शन का सम्बन्ध जीवन के अनुभवों से प्राप्त मूलभूत सिद्धांतों से है। इंसान को अपने संकुचित परिवेश से बाहिर निकाल कर विराट प्रकृति के समक्ष उपस्थित करना, परम सौन्दर्य की ओर उन्मुख करना और अपने अस्तित्व के बाहर और भीतर उस अविनाशी प्रियतम की आनंदानुभूति करना ही सूफ़ी साधना का मूल है।
ज़र्रे-ज़र्रे में उस परम चेतना का निवास होने की वजह से सूफ़ी इसी प्रकृति के नाट्य में परम सत्ता के रूपों का दर्शन करते हैं। वह संसार की हर शै में इसी ईश्वरीय चेतन सत्ता का मनोहारी संगीत सुनते हैं।
सूफ़ी संतों के काव्य में कहीं बनावटीपन नहीं मिलता। सूफ़ियों का ज्ञान अनुभवजनित होता है। इस अनुभवजनित ज्ञान को स्वर देने के लिए ही सूफ़ी कविता का प्रयोग करते थे। इनकी कविता को अनुभव के उसी तल पर जाकर समझा जा सकता है। दादू दयाल जी ने लिखा है – “केते पारिख पचि मुए, कीमत कही न जाय”
सूफ़ियों ने अपने अनुभव को जन्म के अंधे का स्वप्न, या गूंगे के गुड़ खाने से व्यक्त किया है। गूंगा व्यक्ति जिस प्रकार स्वाद की अनुभूति में असमर्थ हो कर केवल संकेतों के माध्यम से अपनी बात कहता है, उसी प्रकार इस भक्ति रस का पान करने वाले सूफ़ी साधक भी भाषा के सामान्य प्रयोग से ऊपर उठ कर प्रतीकात्मक भाषा में अपनी बात कहते हैं। जब आशिक़ और माशूक़ में कोई अंतर शेष नहीं रहता तब एकात्म भाव की परिणति होती है।
भारतीय जीवनशैली, संस्कृति एवं साहित्य को भगवान श्री कृष्ण ने अनेक रूपों में प्रभावित किया है। कृष्ण को केंद्र में रखकर जितने साहित्य की रचना हुई है उतनी किसी अन्य व्यक्तित्व को लेकर नहीं हुई।कृष्ण का व्यक्तित्व निरंतर विकास शील रहा है।कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में आया है जहाँ उन्हें ऋषि कहा गया है। सूफ़ी कवियों में मालिक मुहम्मद जायसी ने कृष्ण पर केन्द्रित अपनी किताब कन्हावत लिखी है। सूफ़ी स्वाभाव के अनुकूल ही उन्होंने आचार,विश्वास आदि के नाम पर हिन्दू या मुसलमान किसी की खिल्ली नहीं उड़ाई और न ही दोनों धर्मों के खंडन कर उन्हें चिढ़ाया। जायसी का मार्ग प्रेम का मार्ग था। प्रेम की इस अमृत धारा में हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य का मैल धुल गया। जायसी ने सूफ़ियों की नीति का परिचय कन्हावत में बड़े सुन्दर ढंग से दिया है –
जोगी केर जोग भल, भोगी कर भल भोग
कन्हावत महाकाव्य की कथा का मूलाधार श्रीमदभागवत है। उस समय ब्रज में वल्लभाचार्य का बड़ा प्रभाव था और उनकी यात्राएं ब्रजमंडल में होती रहती थी। जायसी ने सूफ़ी दर्शन को इस महाकाव्य में बड़े खूबसूरत तरीक़े से व्यक्त किया है –
परगट भेस गोपाल गोविन्दू – कपट गियान न तुरुक न हिन्दू
साहित्य में परंपरा जो सूफ़ी को अपने पूर्व के सूफ़ियों से विरासत के रूप में मिलती है, उन साहित्यिक प्रयोगों को भविष्य में और विकसित रूप देना ही उस परंपरा का सही निर्वहन है। सूफ़ी कवि अपने पूर्व की परंपरा की उपेक्षा नहीं करता। यह परंपरा एक ऐसी वस्तु है जिसे एक हाथ से लिया जाता है और अपने अनुभवों की चाशनी में लपेट कर अगली पीढ़ी को दिया जाता है। परंपरा का उतना अंश ही महत्वपूर्ण होता है जो हमें ऐसा संस्कार दे जिस में विस्तार की सम्भावना और उदारता हो।
जायसी की यह परंपरा हमें हज़रत शाह काज़िम क़लन्दर के कलाम में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। हज़रत शाह काज़िम क़लन्दर कृष्ण की छवि से मोहित हैं और सूफ़ियों का सम्पूर्ण दर्शन उन्हें कृष्ण की छवि और उनकी लीलाओं में दिखाई पड़ता है। यह सूफ़ियों के श्रीकृष्ण से बढ़ते सम्बन्ध का दूसरा उदहारण है। शाह काज़िम क़लन्दर लिखते हैं –
गुप्त नहीं प्रकट है काज़िम घट–घाट वाही को देख जमाल
सूफ़ी साधना की चार अवस्थाएँ कही जाती हैं। पहली अवस्था हाल की अवस्था है। यह वो अवस्था है जब सूफ़ी साधक का मन विचलित होता है । उसे लगता है कि उसे कुछ चाहिए लेकिन क्या चाहिए यह मालूम नहीं है। सूफ़ी इसे ईश्वर का वरदान कहते हैं। दूसरी अवस्था मक़ाम की अवस्था है। इस अवस्था में मुर्शिद अपने मुरीद को ढूंढ लेता है। आत्मा रुपी युवती की शादी हो गई है पर गौना नहीं हुआ। पति के स्वरुप का वर्णन अपनी सखियों से तो ख़ूब सुना है लेकिन अब तक पति के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तीसरी अवस्था बक़ा की अवस्था है। जब मुर्शिद अपने मुरीद के साथ रहता है। युवती का गौना हो गया और अब वह पति के साथ रह रही है और उसे समझ रही है। चौथी अवस्था फ़ना की अवस्था है जब मुर्शिद और मुरीद का भेद ही समाप्त हो जाता है। मुर्शिद और मुरीद दोनों एक हो जाते हैं। कुछ सूफ़ियों ने एक और अवस्था बताई है -फ़ना होकर बक़ा रहने की अवस्था, जब मुर्शिद नहीं रहता, मुरीद बच जाता है लेकिन वह मुर्शिद का ही प्रतिरूप होता है।
जायसी के काव्य में जहाँ हाल और मक़ाम की अवस्था का वर्णन मिलता है वहीं हज़रत शाह काज़िम क़लन्दर के कलाम में बक़ा और फ़ना की अवस्थाओं का वर्णन साफ़ ज़ाहिर होता है। कहीं शाह काज़िम श्री कृष्ण से क्षण भर का वियोग सहन नहीं कर पाते –
मनमोहन हो कहाँ जाय बसे
कल करत रहे जो उन कुंजन बिछुड़े फिर न मिले दर्शन
धीरे–धीरे मन बिरहन को कब हुए बिछुड़े फिर न मिले दर्शन
वहीं श्री कृष्ण जब उनके सामने खड़े हो जाते हैं तो शाह काज़िम उन पर तन-मन-धन सब न्योछावर कर देते हैं –
काले–पीले श्वेत हरे मा, हम तो देखा हरे हरे
फिर देखा हरा न काला, को दीन्ह कहे लो पियरवा
सूफ़ियों का वहदत-उल-वजूद परमात्मा को ही एक-मात्र सत्ता मानता है और उसी का अस्तित्व हक़ीक़ी समझा जाता है। सूफ़ियों के अनुसार दुई संभव नहीं इसलिए या तो वह स्वयं रह सकता है या परमात्मा । परमात्मा ही बचे इस लिए स्वयं के अस्तित्व को मिटा देना ही सूफ़ी दर्शन का मूल है।। शाह काज़िम क़लन्दर भी कृष्ण के स्वरुप को कुछ इसी प्रकार चित्रित करते हैं –
घर–बाहर अब वही है काज़िम, हम ना हैं ना हैं ना हैं
बक़ा की अवस्था का वर्णन शाह काज़िम अपने काव्य में कुछ यूँ करते हैं –
छबि मोहनी का कठिन है देखब
देख पड़त नहीं कोऊ दिखाई
काज़िम देखे साहब अनमूरत
जिस की मूरत होवे कन्हैया
जब शाह काज़िम बक़ा की अवस्था से फ़ना की अवस्था में प्रवेश करते हैं तो उन के समक्ष द्वैत का भेद समाप्त हो जाता है और हर तरफ महबूब के ही दर्शन होते हैं –
अपने पीतम सों हम मिल के हो गए वा के रंग
हम वाके वह हमरे रंग मिल दोऊ भए एक अंग
श्री कृष्ण के घट-घट व्यापी रूप का वर्णन शाह काज़िम क़लन्दर यूँ करते हैं –
जाको बतावें जग से न्यारा, सो पाया डारे गर बाँहें
कौन कहत है अलख निरंजन, घट–घट बीच समयों ना हैं
हज़रत शाह तुराब अली क़लन्दर के काव्य में भी यही रंग मिलते हैं लेकिन इनकी रचनाओं में फ़ना और फ़ना हो कर बक़ा रहने की अवस्था का ज़िक्र भी मिलता है। यहाँ भक्त और भगवान का जो रिश्ता जायसी की कन्हावत से शुरु हुआ था वह और भी ज़्यादा परिपक्व और आत्मीय बन जाता है।
मोरी बिथा सुन कान्ह कहत हैं
मैं तोरी बात पर कान न देहौं
आन बान हमरी है याही
छक के दरस कबहूँ आन न देहौं
जान के मोसे वह जान कहत है
कैसे कहूँ फिर जान न देहौं
वारूँगी जान ‘तुराब‘ पिया पर
जान देहौं पर जान न देहौं
भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता अब इतना प्रगाढ़ हो चला है कि तुराब श्री कृष्ण को उलाहना दे रहे हैं-
बहुत सही तोरी अब न सहूँगी
एक कहोगे तो लाख कहूँगी
चैन करो तुम औरन के संग
मैं नहीं तुम्हरे संग रहूँगी
देखी पीत तुम्हारी झूठी
अब न काहू को जी सो चहूँगी
काहे तू मोसे आँख चुरावत
सन्मुख तोरे मैं आपै न हूँगी
जारो न फूँको जियरवा मोरा
रो रो मैं गंगा पार बहूँगी
जाओ विदेस संताप के हमका
अब तो कबहूँ पाती लिखूँगी
हौं कर जोड़े ‘तुराब’ के आगे
गुरु की दया बिन कब निबहूँगी
शाह तुराब और शाह काज़िम के प्रतीकों में समानता है इस लिए इन के प्रतीक और भी सुन्दर और मार्मिक हो गए हैं। शाह काज़िम के शांत रस में जहाँ विरह का रंग सर्वत्र छाया हुआ है वहीं शाह तुराब की ठुमरियों में मिलन और महबूब से रूठने-मनाने का भाव दिखता है । शाह काज़िम ने कृष्ण के साथ जो सम्बन्ध स्थापित किया था, शाह तुराब उसी राह पर कई क़दम आगे पहुंचे मालूम पड़ते हैं।
हाँ हाँ मो-का न छेड़ कन्हैया
हौं तो दिनन की थोड़ी
वृज मा का एक हम हीं बसत हैं
और बहुत हैं साँवरी गोरी
निकसी हूँ आज मंदिर सो अपने
सास ननद की चोरी
फेंक न लाल गुलाल बसन पर
ऊजर है अब चूनर मोरी
रंग सो बोरे जो मोरी चुनरिया
खेलूँ ‘तुराब’ वही संग होरी
हज़रत शाह तुराब अली क़लन्दर के बारे में एक कहानी काकोरी और लखनऊ में बड़ी प्रसिद्ध है। एक बार इस इलाक़े में कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। हज़रत तुराब अली क़लन्दर ने जब यह देखा तो एक मुनाजात लिखी और कहते हैं कि जब यह दुआ पढ़ी गई तो झमाझम पानी बरसने लगा। आज भी लखनऊ और काकोरी के लोग जब बारिश नहीं होती तो हज़रत शाह तुराब की ये दुआ ज़रूर पढ़ते हैं –
ख़ुदा से या रसूल-अल्लाह बंदों की सिफ़ारिश कर
कि बरसे सब कहें बारान-ए-रहमत ख़ूब सा झर-झर
गया सावन चला भादों न बरसा अब तलक पानी
हुई बरसात आख़िर किस तरह ‘आलम न हो मुज़्तर
मैं तेरा नाम लेता हूँ दु’आ में अव्वल-ओ-आख़िर
वसीला जिस का ऐसा हो दु’आ रद्द उस की हो क्यूँ कर
ख़ुदा-ना-ख़्वास्ता गर ख़ुश्क-साली यूँही रहती है
तो हो जाएगी दुनिया कोई दिन में ‘अर्सा-ए-महशर
जो बादल ख़ूब सा गरजे-ओ-पानी ज़ोर से बरसे
वबा बिजली से मारी जाए महँगी पर गिरें पत्थर
‘तुराब’ आज़ाद हो ग़म से मिटे ये रंज ‘आलम से
घमंड उस का बढ़े मौला तेरी बंदा-नवाज़ी पर
इधर हाल ही में इन पंक्तियों के लेखक का ख़ानक़ाह काज़मिया क़लन्दरिया में जाना हुआ। आज भी यह ख़ानक़ाह एक पुरसुकून दर्सग़ाह मालूम पड़ती है, जहाँ इंसान तो क्या पेड़-पौधे भी अदब से पेश आते हैं। हमें बताया गया कि ख़ानक़ाह में बहुत चुनिन्दा लोगों को ही मुरीद किया जाता है। भारत विभाजन के बाद काकोरी से सैकड़ों परिवारों का पलायन हो गया जिस की वजह से इस ख़ानक़ाह के कई मुरीद पाकिस्तान चले गए। ख़ानक़ाह का परिसर बहुत बड़ा है और मरम्मत की राह देख रहा है। इस ख़ानक़ाह के ज़्यादातर मुरीद नौकरी-पेशा रहे हैं। इस ख़ानक़ाह के शुरुआती भवनों की तामीर राजा टिकैत राय ने करवाई थी। उन के बाद धीरे-धीरे दूसरे निर्माण हुए। ख़ानक़ाह परिसर में आम, बरगद और नीम के सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ एक गहरी अध्यात्मिक शान्ति प्रदान करते हैं। ख़ानक़ाह में हज़ारों पांडुलिपियाँ भी सुरक्षित हैं।
सूफ़ी साहित्य ने भाषाओं के बीच पुल का काम किया है। सूफ़ियों और संतों ने भाषाओं के विकास में न सिर्फ़ अपना अमूल्य योगदान दिया है बल्कि इन के काव्य में भाषाओं के क्रमिक विकास से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूत्र भी छिपे हैं जिन्हें जाने बगै़र हिंदी अथवा उर्दू दोनों भाषाओं का अध्ययन अधूरा है।
–सुमन मिश्र
Guest Authors
- Aatif Kazmi
- Absar Balkhi
- Afzal Muhammad Farooqui Safvi
- Ahmad Raza Ashrafi
- Ahmer Raza
- Akhlaque Ahan
- Arun Prakash Ray
- Balram Shukla
- Dr. Kabeeruddin Khan Warsi
- Dr. Shamim Munemi
- Faiz Ali Shah
- Farhat Ehsas
- Iltefat Amjadi
- Jabir Khan Warsi
- Junaid Ahmad Noor
- Kaleem Athar
- Khursheed Alam
- Mazhar Farid
- Meher Murshed
- Mustaquim Pervez
- Qurban Ali
- Raiyan Abulolai
- Rekha Pande
- Saabir Raza Rahbar Misbahi
- Shamim Tariq
- Sharid Ansari
- Shashi Tandon
- Sufinama Archive
- Syed Ali Nadeem Rezavi
- Syed Moin Alvi
- Syed Rizwanullah Wahidi
- Syed Shah Tariq Enayatullah Firdausi
- Umair Husami
- Yusuf Shahab
- Zafarullah Ansari
- Zunnoorain Alavi