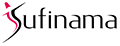लखनऊ का सफ़रनामा
लखनऊ के मुतअ’ल्लिक़ बृज नारायण चकबस्त ने बहुत पहले कहा था :
ज़बान-ए-हाल से ये लखनऊ की ख़ाक कहती है
मिटाया गर्दिश-ए-अफ़्लाक ने जाह-ओ-हशम मेरा
दिल्ली के बा’द हिन्दुस्तान का उजड़ने वाला ये दूसरा शहर है। ब-क़ौल मिर्ज़ा हादी रुसवा:
दिल्ली छुटी थी पहले अब लखनऊ भी छोड़ें
दो शहर थे ये अपने दोनों तबाह निकले
तबाही और बर्बादी के बावजूद भी ये हिन्दुस्तान का मक़बूल-तरीन शहर माना जाता है जहाँ आज भी उसकी ख़ूबसूरती मुसाफ़िरों को ठहरने पर मजबूर करती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि 8 नवंबर 2021 ’ईस्वी सोमवार को दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुआ और सुब्ह 6 बजे चारबाग़ रेलवे स्टेशन पर हमारी गाड़ी पहुँची।स्टेशन पर क़दम रखते ही ऐसा महसूस हुआ कि हम किसी नवाब साहब के क़िला’ या उसकी सैर-गाह में क़दम रख रहे हैं। हैरत-ओ-तहय्युर से इधर उधर तकता फिरता और अपने ज़ेहन पर ज़ोर डालता कि हिन्दुस्तान में इस तरह का स्टेशन तो नहीं पाया जाता फिर ऐसा क्यूँ? छाँट-परख के बा’द तारीख़ ने ये याद-दहानी कराई कि तुम जहाँ खड़े हो वो अवध के नवाब की ता’मीरात का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हुकूमत ने लखनऊ का रेलवे स्टेशन क़रार दिया है। हम ने स्टेशन को ख़ूब ग़ौर से देखा,ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ, उसकी लंबाई, चौड़ाई, बेहतरीन मेहराब, बड़े-बड़े पाए और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत नक़्श-ओ-निगार जो लोगों को देखने पर मजबूर कर रहे थे । लाल चूने से रंगा हुआ नवाब साहब का चार बाग़ अपनी पूरी शान-ओ-शौकत के साथ लखनऊ की ख़ूबसूरती और उसकी तरक़्क़ी का इफ़्तिख़ार बना हुआ है ।मुझ जैसा मुसाफ़िर तो गोया इसी फ़िक्र में डूब गया कि उन्नीसवीं सदी में नवाब साहब का ये बाग़ किस क़दर सर-सब्ज़-ओ-शादाब हुआ करता होगा? ख़ैर हम ब-वक़्त-ए-इशराक़ हज़रत मख़्दूम शाह मीना के आस्ताना पर पहुँचे ये बुज़ुर्ग अवध के सरख़ैल अस्फ़िया में से हैं।
कहते हैं कि आपका नाम शैख़ मोहम्मद और आपके वालिद शैख़ क़ुतुबुद्दीन थे। ये देहली से जौनपुर आए और फिर वहाँ से दिलमउ में क़ियाम-पज़ीर हुए। बचपन ही में आपके ’आदात-ओ-अतवार से आसार-ए-विलायत ज़ाहिर थे ।दस बरस की ’उम्र तक शैख़ क़िवामुद्दीन के ज़ेर-ए-तर्बियत रहे और फिर शैख़ की हस्ब-ए-वसियत उनके ख़लीफ़ा क़ाज़ी फ़रीदून और उनके बा’द शैख़-ए-आ’ज़म से बित्तर्तीब शर्ह-ए-क़ाफ़िया और किताब-ए-विक़ाया पढी । कहते हैं कि आप कभी बे-वुज़ू नहीं रहते। ऐ’न-उल-विलायत में मर्क़ूम है कि एक मर्तबा शैख़ सारंग ने आपको किसी शहर में भेजा। जब आप उस शहर से हो कर दुबारा शैख़ सारंग की ख़िदमत में पहुँचे तो शैख़ ने फ़रमाया कि इस शहर में एक और दरवेश हैं तुम उनसे मुलाक़ात क्यूँ नहीं करते? आपने ’अर्ज़ किया कि मुझको आप ही की मोहब्बत काफ़ी है। शैख़ ने ख़ुश हो कर उन्हें ख़िर्क़ा-ए-ख़िलाफ़त ’अता किया। आख़िर-ए-’उम्र में छ: माह ’अलील रहने बा’द 23 सफ़र 884 हिज्री को विसाल किया। आपके मज़ार-ए-अक़्दस से मुत्तसिल दाएँ तरफ़ आपके बिरादर-ए-ख़ुर्द हज़रत अहमद के ’अलावा पाईं में दो क़ब्रें मौजूद हैं जिस पर कत्बा नहीं है। आस्ताना से मुल्हक़ निहायत कुशादा मस्जिद है उसकी ता’मीर महाराजा मोहम्मद ए’जाज़ रसूल ख़ाँ (जहाँगीराबाद )ने 1343 हिज्री में कराई है और क़िता-ए’-तारीख़ ’अज़ीज़ सफ़ीपुरी ने लिखा है। आस्ताना की जदीद ता’मीर मौजूदा सज्जादा-नशीं शैख़ राशिद ’अली मीनाई इब्न-ए-शैख़ शाहिद ’अली मीनाई 12 नवंबर 2007 ’ईस्वी ता 20 फ़रवरी 2008 में करा चुके हैं। आस्ताना से दस क़दम के फ़सिले पर दाएँ तरफ़ हज़रत औलिया शहीद नामी बुज़ुर्ग का भी मज़ार और हुज्रा है जिस पर 1027 हिज्री दर्ज है । वाक़ि’ई यहाँ दिल बहुत लगा।
अब हम फ़ातिहा पढ़ कर फ़ारिग़ हुए तो सामने किंग जॉर्ज मेडीकल यूनीवर्सिटी नज़र आई।वाक़ि’ई इस यूनीवर्सिटी का बाग़ निहायत दिल-कश है। तक़रीबन दो घंटे तक यहाँ का लुत्फ़ उठाया और अब सुब्ह के नाशते से फ़ारिग़ हो कर बिरादर-ए-’अज़ीज़ शायान अबुल-’उलाई सल्लमहु के हमराह हुसैनाबाद की तरफ़ रवाना हुए। रिक्शे वाले के पहियों की तरह हमारा दिल भी बे-क़ाबू हो रहा था ।अल-अमान वल-हफ़ीज़ करते करते हम लोग हुसैनाबाद पहुँचे जहाँ दाएँ-बाएँ बुलंद से बुलंद ‘इमारतें एक दूसरों के मुक़ाबिल खड़ी थीं। हम ने आसिफ़ुद्दौला (पैदाइश 1748 ’ईस्वी विसाल 1797 ’ईस्वी) का तज़्किरा बुज़ुर्गों से ख़ूब सुना था। वो सारे क़िस्से और मनाज़िर नज़रों के ठीक सामने गर्दिश कर रहे हैं। बेहतरीन से बेहतरीन और ’उम्दा से ’उम्दा ’इमारतें लखनऊ की शान-ओ-शौकत की बेहतरीन मिसाल हैं । पूरा हुसैनाबाद नवाब साहब की कारीगरी से भरा पड़ा है ।अब इन तमाम ’इमारात की सैर दिन-भर में तो मुम्किन नहीं, लिहाज़ा रिक्शे वाले को तय किया और चल पड़े। उसने अपनी शहर की पहचान दिखाते हुए बड़ी ख़ूबसूरती से कहा कि तशरीफ़ रखिए। इस पर हम लोग एक दूसरे का मुँह तकते रहे और जी ही जी में उसका लुत्फ़ ले रहे थे कि भला एक रिक्शे वाला बैठने के लिए तशरीफ़ का लफ़्ज़ इस्ति’माल कर रहा है। दरयाफ़्त करने पर उसने बताया कि हम लखनऊ के आबाई हैं और अब चूँकि ज़िदा-तर अफ़राद लखनऊ में दूसरे शहरों से आकर बस रहे हैं इसलिए लखनवी ज़बान से दूर हो कर वो अपनी ज़बान बोल रहे हैं । मेरे ख़याल से उसकी बुनियादी वजह ये है कि ज़बान की इस्लाह और उसकी तरक़्क़ी वहाँ की तहज़ीब-ओ-तमद्दुन से होती है। जितना तमद्दुन तरक़्क़ी करता जाएगा ज़बान का मे’यार उतना ही बुलंद होता जाएगा और जिस जगह उसकी तरक़्क़ी में कमी आने लगेगी वहीं ज़बान भी ग़ैर मे’यारी होती जाएगी।
अल-ग़र्ज़ हम लोग इमाम-बाड़ा की तरफ़ रवाना हुए। ये इमाम-बाड़ा लखनऊ में दरिया-ए-गोमती के जुनूबी किनारे से मुल्हक़ हुसैनाबाद इंटर कॉलेज के मग़रिब में एक वसी’-ओ-’अरीज़ ’इलाक़ा का इहाता किए हुए है।
यूँही बातें करते करते रूमी दरवाज़ा पहुँचे।ये दरवाज़ा आसिफ़ुद्दौला की अहलिया ने 1784 ’ईस्वी में ता’मीर किराया था। इसकी ख़ूबसूरती और बनावट कुछ इस तरह है कि छोटा इमाम-बाड़ा की तरफ़ से आईए तो एक कुशादा दरवाज़ा है और लौटिए तो तीन छोटे छोटे दरवाज़े हैं। कहते हैं कि नवाब की अहलिया ने दरवाज़ा के ऊपरी हिस्सा में लौंग का नक़्शा बनवाया है, ये तक़रीबन 27 ’अदद थे जो अब झड़ कर सिर्फ़ 22 रह गए हैं ।इस दरवाज़ा की दूसरी ख़ास बात ये है कि इसको उलट कर देखिए तो अहलिया के गले का हार नज़र आएगा। लखनऊ के चिकन कुर्ते के काज के इर्द-गिर्द आज भी रूमी दरवाज़ा का ’अक्स बना होता है।
अब हम बड़ा इमाम-बाड़ा में दाख़िल होते हैं ।इसमें दाख़िल होने का टिकट 50 रुपये का है। इसे इमाम बाड़ा और आसिफ़ी इमाम बाड़ा भी कहते हैं ।इसे आसिफ़ुद्दौला ने ता’मीर कराया है जो दस अहम हिस्सों पर मुश्तमिल है जिन में रूमी दरवाज़ा, पहला मर्कज़ी दरवाज़ा, नौबत-ख़ाना, गोल सेहन-ओ-सब्ज़ा-ज़ार, मस्जिद-ए-आसिफ़ी, बावली और भूलभुलय्या शामिल हैं। मुहर्रम के महीने में आईए तो ये हुसैनाबाद ईरान से कम नहीं लगता।जिसने ईरान का लुत्फ़ उठाया है या उसकी तहज़ीब से आश्ना है वो इसे ब-ख़ूबी समझता है । इस इमाम-बाड़े की ता’मीर के बारे में मुख़्तलिफ़ क़िस्से बयान हुए हैं ।कहा जाता है कि 1784 ’ईस्वी के आस-पास अवध में शहर का हर अमीर-ओ-ग़रीब क़हत-साली का शिकार हो रहा था। आसिफ़ुद्दौला ने उस नाज़ुक मौक़ा’ पर लोगों को रोज़गार फ़राहम करने की निय्यत से इमाम-बाड़ा की बुनियाद रखी ।चूँकि अमीर लोग दिन में मज़दूरी करने से शरमाते थे इसलिए ता’मीर का काम दिन की तरह रात को भी जारी रखा गया ताकि फ़ाक़ा-कश अमीर लोग रात के अंधेरे में आकर मज़दूरों में शरीक हो सकें । इस तरह अवध के बिगड़ते हुए मआ’शी हालात भी दरुस्त हुए और इमाम-बाड़ा की ता’मीर भी मुकम्मल हो गई।
हम लोग मर्कज़ी दरवाज़ा से दाख़िल हुए और वसी’-ओ-’अरीज़ बाग़ की सैर करते हुए आसिफ़ी मस्जिद पहुँचे जिसे आसिफ़ुद्दौला ने इमाम-बाड़ा की ता’मीर से क़ब्ल बनवाया है ।इस मस्जिद में हज़ारों नमाज़ियों की गुंजाइश है। सेह गुंबद और दो लंबे मीनार के साथ सेहन-नुमा मस्जिद जिस पर सियाह रंग चढ़ा है ।बड़ी लंबी-लंबी सीढ़ियाँ और कुशादा कमरे के साथ हिन्दुस्तान की चंद ख़ूबसूरत मसाजिद में से एक है।इस मस्जिद के पहले इमाम मा’रूफ़ शी’आ ’आलिम मौलाना सय्यद दिलदार नक़्वी (पैदाइश 1753 ’ईस्वी विसाल 1820) ’ईस्वी हुए।
अब हम लोग वस्ती दालान की तरफ़ बढ़ रहे हैं ।ये दालान 303 फ़िट लंबा, 53 फिट चौड़ा और 63 फिट ऊँचा है और दुनिया के ’आला-तरीन दालानों में से एक है जिस में लोहे लकड़ी के ब-ग़ैर बे-मिसाल डाँट के साथ जोड़ी गई है । दूसरे लोगों की तरह हम लोग भी अपने अपने क़दम आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाते हुए दाख़िल हुए ।इसी दालान में नवाब आसिफ़ुद्दौला दफ़्न हैं।इस के पाँच मेहराबी दरवाज़े हैं। नवाब साहब की क़ब्र के इर्द-गिर्द ’उम्दा से ’उम्दा फ़ानूस रखे हुए हैं। लोग अदब के साथ उस जगह की ज़ियारत करते हैं और दिल ही दिल में मुस्कुराते हैं ।पर हम इस सोच-ओ-फ़िक्र में गुम हैं कि हमारी शान-ओ-शुकूह के वो सुनहरे दौर कहाँ चले गए? हमारी ’अज़मत-ए-रफ़्ता कैसे बहाल होगी? हमारा माज़ी इस क़दर ताबनाक मगर मुस्तक़बिल की कोई खबर नहीं। अस्लाफ़ के कार-नामों पर हम कब तक जीते रहेंगे? क्या हमारे बा’द आने वाली नस्लों का कोई सरमाया होगा? हैरानी-ओ-परेशानी है कि हम माज़ी की रट लगाते लगाते मुस्तक़बिल से ना-आशना हो गए। सर सय्यद ख़ाँ (पैदाइश 1817 ’ईस्वी विसाल 1898 ’ईस्वी) ने ’अज़ीमाबाद में ख़िताब करते हुए कहा था :
“अपने बाप दादा की ’इज़्ज़त-ओ-बुजु़र्गी-ओ-हश्मत-ओ-मंज़िलत पर नाज़ करना बड़ी ग़लती है। हमारे बाप दादा अगर बहुत ’आली-क़द्र थे और हम नहीं हैं तो हम को इस पर नाज़ नहीं करना चाहिए बल्कि रोना चाहिए कि हम अपने बड़ों का भी नाम डुबोने वाले पैदा हुए, अगर औलाद की और क़ौम की ता’लीम-ओ-तर्बियत इस सतह पर न हो कि जिस ज़माना में वो लोग अपनी ज़िंदगी बसर करेंग़े उस ज़माने की मुनासिब लियाक़तें उनमें पैदा न हों तो ज़रूर अगले ख़ानदानों का नाम बर्बाद हो जावेगा, नवाब ख़लीलुल्लाह ख़ाँ शाह-जहाँनी का आप लोगों ने नाम सुना होगा।उनके पड़ पोते को मैं ने अपनी आँख से देखा है कि लोगों के पाँव दाबने आता था और दो-चार, तुग़लक़ाबाद के गाँव में जिस क़दर मुसलमान घसियारे आबाद हैं जो सारे दिन घास खोदकर शाम को बेचते हैं, मैंने ख़ूब तहक़ीक़ किया है कि सुल्तान मोहम्मद ’आदिल तुग़लक़ की औलाद में हैं, पस अगले बुज़ुर्गों पर फ़ख़्र करना ऐसी हालत में कि हम कुछ नहीं हैं क्या फ़ाएदा है?’
दुनिया में गुज़रे हुए वाक़िआ’त से हम को ’इब्रत और नसीहत पकड़नी चाहिए । ज़माना के वाक़िआ’त हम से आइन्दा ज़माना के वाक़िआ’त की पेशीन-गोई कर सकते हैं, इसी तरह की नसीहत-आमेज़ जुमले हमें हज़रत शाह अकबर दानापुरी पैदाइश 1843 ’ईस्वी विसाल 1909 ’ईस्वी) की तस्नीफ़ात में भी जा-बजा मिलते हैं।
ख़ैर बात कहाँ चल रही थी और हम कहाँ चले गए। अल-ग़र्ज़ इस ’इमारत का बालाई हिस्सा भी नक़्श-ओ-निगार से मुज़य्यन है ।कहते हैं मसूर की दाल और गन्ने के रस की मदद लेकर इस के बालाई हिस्सा को मज़बूत बनाया गया है। बड़े से बड़े और ’उम्दा से ’उम्दा ता’ज़िए और दर्जनों ’अलम एहतिराम के साथ ऊँची ऊँची जगहों पर रखे हुए हैं ।अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल कर बाएँ तरफ़ सीढ़ियों से चढ़ कर भूलभुलय्या की तरफ़ जा रहे हैं ।ये ना-क़ाबिल-ए-यक़ीन और लखनऊ की मशहूर सैर-गाह है ।इस के चकले रास्ते 489 एक जैसे दरवाज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से रास्ता ढूँढ़ना बहुत दुशवार हो जाता है ।कहा जाता है कि बालकोनी तक पहुँचने के 1024 रास्ते हैं जबकि वापसी के सिर्फ़ दो ही रास्ते हैं। यहाँ की दीवारों के कान भी होते हैं। कान को दीवार से मिला कर कुछ काहिए तो दूसरी तरफ़ कान लगाए हुआ शख़्स आपकी बात ब-ख़ूबी समझ सकता है। ’इमारत के ऊपरी हिस्सा से लखनऊ शहर को ब-ख़ूबी देखा जा सकता है। तक़रीबन दो एक घंटे की सैर के बा’द थोड़े वक़्फ़ा के लिए आराम किया और फिर बावली की तरफ़ चल पड़े ।ये बावली सी-सी-टी-वी कैमरे की मानिंद अंदर साइड की नक़्ल-ओ-हरकत दूसरी तरफ़ दिखाने का काम देता है ।अंदर बैठा शख़्स बाहर आने वाले कै ब-ख़ूबी देख सकता है मगर बाहर से आने वाला उससे बे-ख़बर रहता है। कहते हैं कि बावली में आज भी एक खज़ाने का राज़ छुपा है जिसे फ़िरंगियों के काफ़ी तलाश-ओ-तहकीक के बा’द भी वो उनके हाथ लगा।
अब हम लोग यहाँ से फिरते-फिराते छोटा इमाम बाड़ा पहुँचे। इसे अवध के नवाब मोहम्मद ’अली शाह (पैदाइश 1777 ’ईस्वी विसाल 1842 ’ईस्वी) ने 1837 में ता’मीर करवाया था। यहाँ आज भी मजालिस बरपा होती हैं ।मुहर्रम में लाखों रुपए के नियाज़ यहाँ से तक़्सीम होते हैं। आसिफ़ी इमाम-बाड़ा की निस्बत छोटा होने की वजह से उसे छोटा इमाम बाड़ा कहा जाता है अगरचे ये बड़ा वसी’-ओ-’अरीज़ है।
ये आगरा के ताजमहल की तर्ज़ पर बनाया गया हिन्दी और ईरानी नक़्शा है ।इस में हौज़ और बाग़ के ’अलावा मुख़्तलिफ़ मक़्बरे और एक मस्जिद भी हैं । ता’ज़िए, चंदन, मोम, हाथी के दाँत और दीगर क़ीमती अश्या के ’अलावा मुख़्तलिफ़ नवाब और उनके ख़ानदान के मुत’अद्दिद लोगों को यहाँ पर दफ़्न किया गया है ।इसी वजह से उसे नवाबों की आख़िरी आराम-गाह भी कहते हैं और एक क़ौल के मुताबिक़ इसके बानी नवाब मोहम्मद ’अली शाह, उनकी माँ, बेटी और उनके दामाद का मक़्बरा भी यहीं पर बना है।
इसकी सजावट बेल्जियम के काँच के क़ीमती झाड़, फ़ानूस, क़िंदीलों, दीवार-गीर और शम्’-दान से की गई है जिसकी बाबत ये पैलेस ऑफ़ लाइट भी कहलाता है। फ़ारसी काँच भी इस्ति’माल हुई है।दीवारों पर क़ुरआनी आयात कंदा हैं और सदर दरवाज़ा पर मछली के मुजस्समे और तार बाँधे गए हैं ताकि बिजली के असरात इमाम-बाड़ा की ’इमारत पर न पड़े। हवा जिधर की होती है मछली का मुँह उधर होता है।इसी ख़ूबसूरती और कारी-गरी के पेश-ए-नज़र उसे क्रिमलन आफ़ इंडिया भी कहा जाता है।
इसकी सैर कराने वाले ने हमें एक एक जगह की तफ़्सील और तारीख़ी कुन्हियात बतलाई। नवाब का कमरा, दालान, हम्माम, बाग़, ’इबादत-गाह और क़ीमती और तारीख़ी ता’ज़िए और ’अलम वग़ैरा की ज़ियारत के बा’द हम लोग घंटा-घर की तरफ़ चल पड़े। इस पर एक बड़ी सी घड़ी चस्पाँ हैं जो दुरुस्त वक़्त बताती है इसी से मुत्तसिल शाही तालाब, चाँद देखने के लिए एक मख़्सूस जगह और पिक्चर गैलरी है जिसे नवाब मोहम्मद ’अली शाह ने 1838 ’ईस्वी में ता’मीर कराया था। यहाँ लखनऊ के नवाब की मुख़्तलिफ़ पेंसिल स्कैच तसावीर और क़ीमती अश्या मौजूद हैं।
इन तमाम जगहों की ज़ियारत से जब फ़ारिग़ हुए तो शाम के पाँच गए थे। अब हम लोग हुसैनाबाद की सड़क पर निकले तो यक़ीन जानिए कि यूँ महसूस हुआ कि ईरान की सड़कों पर घूम रहे हैं। ईरानी चाय, ईरानी ज़बान के बड़े-बड़े पोस्टर और वहाँ की कुछ नक़्लें देख कर दिल ने एक ठंडी साँस ली और कहने लगा कि जैसे जौनपूर कभी शीराज़-ए-हिन्द हुआ करता था ऐसे ही लखनऊ भी कभी ईरान हुआ करता होगा।
अब हम लोगों ने अपने क़दम बढ़ाने शुरू’ किए और लखनऊ की सड़कों का तमाशा देखते हुए अमीनाबाद पहुँचे।ये बाज़ार वाक़ि’ई लखनऊ की शान है ।छोटे-बड़े हर तरह के साज़-ओ-सामान यहाँ फ़रोख़्त होते हैं। बड़ी तलाश-ओ-तहक़ीक़ के बा’द हमें एक दो दुकानें दो-पलिया या दो-पलड़ी कुलाह के मिले। चंद टोपियाँ जो पसंद आईं वो ले लिए पर मज़ीद दिल को तशफ़्फ़ी देने वाली टोपी की तलाश बाक़ी रही। कुलाह फ़रोख़्त करने वाला बेचारा ये कहता रहा कि परसों आईए तो बड़ी ख़ूबसूरत और कारीगरी से पुर टोपियों का कलेक्शन आएगा उनमें पसंद कर लीजिएगा अब उस बेचारे को क्या पता एक मुसाफ़िर की परेशानी। ये टोपी लखनऊ की तहज़ीब-ओ-तमद्दुन का एक बड़ा हिस्सा है। लखनऊ और इसके आस-पास के शहरों में इसका बहुत रिवाज है। मिर्ज़ा अनीस और पण्डित दया शंकर नसीम हमेशा दो-पलिया टोपी का ही इस्ति’माल करते थे ।कहा जाता है कि हज़रत मौलाना शाह ज़फ़र सज्जादा अबुल-’उलाई (पैदाइश 1907 ’ईस्वी विसाल 1974 ’ईस्वी) अमीनाबाद में मस्जिद के नीचे से दोपल्ला टोपी ख़रीदी थी और एक बड़ा नोट निकाल कर दिया था जिस पर दुकानदार ने हैरत का इज़हार करते हुए कहा कि इतने बड़े नोट का खुदरा नहीं है।उसी वक़्त नमाज़ का वक़्त हुआ तो शाह साहब नमाज़ के लिए मस्जिद में दाख़िल हो गए। नमाज़ से फ़राग़त के बा’द ख़याल न रहा और वो दानापुर लौट आए। तक़रीबन 30 बरस बा’द आपको ख़याल आया तो अमीनाबाद जा कर उस दूकान-दार को टोपी का पैसा दिया जिस पर दुकान-दार की हैरानी देखने लाइक़ थी।
“लखनऊ हम पर फ़िदा और फ़िदा-ए-लखनऊ” की ता’बीर देखना है तो अमीनाबाद की गलियों का जाइज़ा लीजिए। तरह तरह की ख़ूबसूरत अश्या, बेहतरीन से बेहतरीन अन्वा’-ओ-अक़्साम, की ऐ’श-ओ-’इश्रत से भरी अवधी तहज़ीब का एक बड़ा हिस्सा यहाँ बसता है। ख़ैर हम लोग बाज़ार की सैर के बा’द अमीनाबाद के मशहूर टुंडे कबाब जिसे गुलावटी कबाब भी कहते हैं, की दुकान पर गए । टुंडे कबाब की दुकान पर लोगों की भीड़ थी ।कहा जाता है कि भोपाल के नवाब साहब को खानों का बड़ा शौक़ था पर आख़िर ’उम्र में उनके दाँत टूट गए थे। उनके खाने के लिए उनके ख़ानसामाँ हाजी मुराद ’अली ने ऐसा कबाब तैयार किया जिसे ब-ग़ैर दाँत के भी खाए जा सकते थे । भोपाल से आए उस ख़ानसामाँ ने 1905 ’ईस्वी में अकबरी गेट के क़रीब गली में अपनी एक छोटी सी दुकान शुरू’ कर दी। टुंडे का मतलब है कि जिसका हाथ न हो। हाजी मुराद ’अली को पतंग का शौक़ था। उसी शौक़ ने उनका एक हाथ ख़त्म कर दिया जो बा’द में काटने पड़े और फिर वो अपने वालिद के हम-राह दुकान पर बैठने लगे। टुंडा होने की वजह से लोग उनके कबाब को टुंडे कबाब कहने लगे ।कहते हैं कि इस कबाब को बनाने में तक़रीबन 100 मसालों को शामिल किया जाता है ।मसालों के अज्ज़ा-ए-तर्कीबी को मख़्फ़ी रखने के लिए उन्हें मुख़्तलिफ़ दुकानों से ख़रीदा जाता है। उनमें से कुछ मसालों को ईरान और दूसरे ममालिक से भी दर-आमद किया जाता है। उसके बा’द उन्हें घर के बंद कमरे में मर्द मिंबरों के ज़रिआ’ बनाया जाता है यहाँ तक कि बेटियाँ भी मसालों का राज़ नहीं जानती हैं। आज तक हाजी ख़ानदान ने कबाब के नुस्ख़े का ये राज़ किसी के सामने नहीं लाया। ये छोटे-छोटे टिकिए के मानिंद बड़े लज़ीज़ और ज़ाइक़े-दार होते हैं ।हम ने ख़ूब आसूदा हो कर खाना खाया और शुक्र-ओ-एहसान के बा’द प्रकाश की ठंडी ठंडी कुल्फ़ी भी चखी। यहाँ की गुलाबी चाय भी बड़ी मशहूर है। अब दिन-भर के सफ़र की थकान से बदन चूर-चूर था ।ख़ैर चैन की साँस ली और क़ियाम किया।
आज 9 नवंबर मंगल की सुब्ह है ।चाय पी कर हम लोग हज़रतगंज की तरफ़ रवाना हुए। ये बाज़ार लखनऊ का सब से क़ीमती बाज़ार है ।इसे नवाब नसीरुद्दीन हैदर शाह (पैदाइश 1803 ’ईस्वी विसाल 1837 ’ईस्वी) ने 1827 में चीन के बाज़ार की तरह गंज मार्केट बनवाया था । नवाब मोहम्मद ’अली शाह के साहबज़ादे नवाब अमजद ’अली शाह ’उर्फ़ हज़रत (पैदाइश 1801 ’ईस्वी विसाल 1847 ’ईस्वी) के ’उर्फ़ी नाम पर 1842 ’ईस्वी में इसका नाम हज़रतगंज पड़ गया। 1857 ’ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इस सड़क की मरम्मत कराई और क़दीम तर्ज़ को गिरा कर लंदन की सड़कों की तर्ज़ पर इसे ता’मीर कराया।
ये बाज़ार निहायत क़ीमती और कुशादा सड़कों पर है।इसके किनारे बड़ी ख़ूबसूरत रौशन-दान और मोटे-मोटे पाए निहायत मज़बूत और ख़ूबसूरत तरीक़े से बनाए गए हैं और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर बैठने के लिए कुर्सी-नुमा स्टेंड भी लगाए गए हैं। दिल्ली की सैर करने वाले इसको कनॉट प्लेस से भी तश्बीह देते हैं।
अब हम नवाब वाजिद ’अली शाह (पैदाइश 1822 ’ईस्वी विसाल 1887 ’ईस्वी) से मंसूब बाग़ की तरफ़ बढ़ रहे हैं । ये बाग़ सौ साल क़ब्ल 29 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ़ वेल्ज़ के इस्तिक़बाल के लिए बनाया गया था।बनारस से दरख़्त मंगवा कर यहाँ लगवाए थे । कुछ मुंतख़ब जानवर भी रखे गए। इस तरह तीन किलो मीटर के वसी’-ओ-’अरीज़ दाइरे में एक ग्रीन पार्क का वजूद ’अमल में आया। बा’ज़ अफ़राद इसे बनारसी बाग़ भी कहते हैं, ता-हम प्रिंस ऑफ़ वेल्ज़ की आमद के बा’द ये इब्तिदाअन पार्क बना और फिर उसे प्रिंस ऑफ़ वेल्ज़ ज़ूलॉजिकल पार्क कहा जाने लगा और अब उसे नवाब वाजिद ’अली शाह ज़ूलॉजिकल पार्क या’नी चिड़िया-घर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक़रीबन पाँच हज़ार दरख़्त हैं जो शहर के एक हिस्से को तर-ओ-ताज़ा रखने में अहम किर्दार अदा करते हैं और दरमियान में एक ख़ूबसूरत संग-ए-मरमर का बना हुआ वसी’ दालान है जिसके चारों जानिब दिल-फ़रेब झरने और बाग़ात हैं।
अगर आप लखनऊ की सैर के लिए ‘आज़िम-ए-सफ़र हैं तो वहाँ के रिक्शे वालों को पहले ही तंबीह कर दीजिए कि मंज़िल के ’अलावा दूसरे मक़ामात पर मत लेजाना। हमें हर एक रिक्शे वाला सब से पहले चिकन की फ़ैक्ट्री ले गया और पहली दूसरी मर्तबा तो आदमी कुछ ख़रीद भी ले पर बार बार तबी’अत पर गिराँ गुज़रने लगता है।बा’द में सख़्ती से मना’ कर दिया कि हमें चिकन की फ़ैक्ट्री नहीं जाना है। एक रिक्शे वाले से पूछने पर पता चला कि 12 ’अदद कस्टमर पर एक चिकन कुर्ता फ़ैक्टरी से ब-तौर-ए-’इनआ’म मिलता है। लखनऊ के चिकन कुर्ता पर ग़ौर कीजिए तो पता चलेगा कि काज का किनारा रूमी दरवाज़ा का ’अक्स है।
अब यहाँ से निकल कर हम लोग अंबेडकर मेमोरियल पार्क की तरफ़ बढ़े। ये जगह भी निहायत ख़ूबसूरत और वसी’-ओ-’अरीज़ है।आधा शहर उसके बालाई हिस्से से बिलकुल साफ़ नज़र आता है ।मुख़्तलिफ़ हाथी-नुमा स्टैचू और पत्थर की कारी-गरी से भरा हुआ ये पार्क मौजूदा अहद में ता’मीरात का एक बेहतरीन हिस्सा है। थोड़े वक़्फ़े के बा’द हम लोग नज़ीराबाद पहुँचे ।ये बाज़ार भी अमीनाबाद से कम नहीं है। मोटर्स के पार्ट्स से लेकर हर तरह के सामान यहाँ नज़र आ रहे हैं ।आदमियों का हुजूम और ख़रीदारों की भीड़ धीरे-धीरे बढ़ती ही जा रही है। कुछ कपड़े की ख़रीद-ओ-फ़रोख़्त के बा’द अमीनाबाद से होते हुए हज़रतगंज पहुँचे ।यहाँ का बास्केट चाट काफ़ी लज़ीज़ होता है। हम लोग हज़रतगंज की सैर करते हुए चार-बाग़ रेलवे स्टेशन पहुँच कर नवाब वाजिद ’अली शाह अख़्तर का ये शे’र गुनगुना रहे हैं कि:
दर-ओ-दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं
ख़ुश रहो अहल-ए-वतन हम तो सफ़र करते हैं
Guest Authors
- Aatif Kazmi
- Absar Balkhi
- Afzal Muhammad Farooqui Safvi
- Ahmad Raza Ashrafi
- Ahmer Raza
- Akhlaque Ahan
- Arun Prakash Ray
- Balram Shukla
- Dr. Kabeeruddin Khan Warsi
- Faiz Ali Shah
- Farhat Ehsas
- Iltefat Amjadi
- Jabir Khan Warsi
- Junaid Ahmad Noor
- Kaleem Athar
- Khursheed Alam
- Mazhar Farid
- Meher Murshed
- Mustaquim Pervez
- Qurban Ali
- Raiyan Abulolai
- Rekha Pande
- Saabir Raza Rahbar Misbahi
- Shamim Tariq
- Sharid Ansari
- Shashi Tandon
- Sufinama Archive
- Syed Ali Nadeem Rezavi
- Syed Moin Alvi
- Syed Rizwanullah Wahidi
- Syed Shah Shamimuddin Ahmad Munemi
- Syed Shah Tariq Enayatullah Firdausi
- Umair Husami
- Yusuf Shahab
- Zafarullah Ansari
- Zunnoorain Alavi