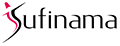ग्रामोफ़ोन क़व्वाली
 Sufinama
August 23, 2024
Sufinama
August 23, 2024
क़व्वाली अरबी के क़ौल शब्द से बना है जिस का शाब्दिक अर्थ बयान करना है। इसमें किसी रुबाई या ग़ज़ल के शेर को बार-बार दुहराने की प्रथा थी लेकिन तब इसे क़व्वाली नहीं समाअ कहा जाता था। महफ़िल-ए-समाअ का प्रचलन हिंदुस्तान के सूफ़ी ख़ानक़ाहों में बहुत पहले से रहा है।
समाअ या क़व्वाली जब हिंदुस्तान में आई तो उसमे फ़ारसी का समावेश हो चुका था। हज़रत अमीर ख़ुसरौ ने समाअ और क़व्वाली को नए आयाम दिये। जहाँ उन्होंने फ़ारसी और हिंदवी का इसमें सम्मिश्रण किया वहीं नए रागों और साज़ों का आविष्कार कर क़व्वाली को सूफ़ी ख़ानकाहों के साथ-साथ आम जनता के बीच भी मक़बूल कर दिया। क़व्वाली में नए स्थानीय आयामों जैसे चादर, बसंत, सेहरा, गागर आदि डालकर इसे विशुद्ध हिंदुस्तानी बनाने का श्रेय अमीर ख़ुसरौ को ही जाता है। अमीर ख़ुसरौ के हिंदवी कलाम बदक़िस्मती से कालचक्र में कहीं खो गए लेकिन क़व्वालों ने सीना-ब-सीना इन्हें याद रखा और इन्हें जनमानस तक पहुँचाया।
प्रसिद्ध किताब ‘सियर-उल-औलिया’ में कई पेशेवर क़व्वालों का ज़िक्र आया है। इससे पता चलता है कि क़व्वाल सूफ़ी ख़ानक़ाहों के अलावा बाहर की महफ़िलों में भी गाया करते थे। इन क़व्वालों में अमीर ख़ुर्द ने दो क़व्वालों का उल्लेख ज़्यादा किया है। ये क़व्वाल थे – हसन पेहदी और सामित क़व्वाल। ये दोनों हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ख़िदमत में हाज़िर रहते थे। बक़ौल अमीर ख़ुर्द, हसन पेहदी महफ़िल के श्रोताओं को अपनी गायकी से मंत्रमुग्ध कर देते थे और लोगों में हाल की कैफ़ियत तारी हो जाती थी। सामित क़व्वाल में भी येी खूबियाँ थी। हसन पेहदी जहाँ बाहर की मजलिसों में भी हिस्सा लेते थे, वहीं सामित क़व्वाल पूरी तरह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ख़ानक़ाह के लिए समर्पित थे और जब भी हज़रत क़व्वाली सुनने की इच्छा ज़ाहिर करते थे, ये हमेशा हाज़िर रहते थे। हज़रत बारहा अपनी ख़ानक़ाह से बाहर बाग़ में अथवा चबूतरा-ए-यारा (ये जगह हज़रत की मौजूदा दरगाह के पास ही स्थित हैं जहाँ हज़रत के महबूब भांजे शेख़ तक़ीउद्दीन नूह की क़ब्र है) चहल-कदमी करने जाते थे तब उनके साथ ख़्वाजा इक़बाल (ख़ानक़ाह की देख-रेख का ज़िम्मा इनका था) और सामित क़व्वाल भी होते थे जो बहुत धीमी आवाज़ में मुख़्तलिफ़ शायरों की ग़ज़लें पढ़ते रहते थे। जिस शायर की ग़ज़ल हज़रत पर अपना प्रभाव छोड़ती थी वो ग़ज़ल समाअ महफ़िलों में प्रसिद्ध हो जाती थी।
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने क़व्वालों को गाने के एवज़ कभी भी पैसे नहीं दिये, हालांकि ख़्वाजा इक़बाल जिनके ज़िम्मे ख़ानक़ाह की पूरी व्यवस्था थी वो क़व्वालों को पैसे दिया करते थे या नहीं ये राज़ कभी नहीं खुला। सियर-उल-औलिया से मालूम पड़ता है कि शायद क़व्वालों की आमदनी के दूसरे ज़रिए भी थे। क़व्वाल ऐसी महफ़िलों में भी क़व्वाली पढ़ा करते थे जिनका सूफ़िया से कोई तअल्लुक़ नहीं होता था। सियर-उल-औलिया के अनुसार–ख़्वाजा अज़ीज़उद्दीन जो अमीर ख़ुर्द के रिश्तेदार और क़व्वाल भी थे, दिल्ली से कुछ दिनों तक बाहर रहे और वापसी के बाद सबसे पहले हज़रत की ख़ानक़ाह पर हाज़िरी दी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उनसे उनके सफ़र के बारे में पूछा और साथ ही साथ ये भी पूछा कि शादी में जो महफ़िल-ए-समाअ हुई वो कैसी थी ?
ख़ैर-उल-मजालिस में भी क़व्वालों के ख़ानक़ाह के बाहर प्रदर्शन का ज़िक्र आता है। ख़्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ दिल्ली, सय्यद अलाउद्दीन नामक क़व्वाल से पूछते हैं कि महफ़िल-ए-समाअ’ कैसी थी और कहानी में आगे अल-कुशैरी के निशापुर की एक महफ़िल में शिरकत करने का ज़िक्र भी आता है।
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीदों की शायरी क़व्वाली क़व्वाल ख़ूब पढ़ते थे। उस समय छपाई के साधन पर्याप्त न होने की वजह से क़व्वाल अपनी शायरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पँहुचाने का एक सशक्त माध्यम थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ख़ानक़ाह से जुड़ाव निश्चय ही क़व्वालों और शायरों के लिए फ़ायदेमंद था क्योंकि उन की प्रसिद्धि आवाम में फैल रही थी। इस तरह न सिर्फ़ उस वक़्त बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए गंगा-जमुनी तहज़ीब का एक ख़मीर पैदा हुआ जिस का प्रभाव ये हुआ कि दो महान संस्कृतियों को आपस में घुलने-मिलने का एक साझा मंच मिल गया।
क़व्वाली का सबसे रोचक पक्ष ये है कि हिंदुस्तान में गंगा-जमुनी तहज़ीब की जब नीव डाली जा रही थी, क़व्वाली ने उस काल को भी अपने रस से सींचा है। क़व्वाली ने हिन्दुस्तानी साझी संस्कृति को न सिर्फ़ बनते देखा है बल्कि इस अनोखी संस्कृति के पैराहन में ख़ूबसूरत बेल बूटे भी लगाए हैं और अपने कालजयी संगीत से इस संस्कृति की नीव भी मज़बूत की है। क़व्वालों को ये संस्कृति विरासत में मिली है। क़व्वालों का ये योगदान आज के दौर में इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्यूंकि इन्हों ने हमारी इस गंगा-जमुनी तहज़ीब को अपना स्वर दिया है।
सियर-उल-औलिया के नौवे अध्याय के पहला पारा आदाब-ए-समाअ को मन्सूब है जिसमे महफ़िल-ए-समाअ के आदाब बताए गए हैं। इसमें समाअ के दौरान हँसना, खाँसना और जम्हाई लेने की मनाही की गयी है। सुनने वाले का ध्यान क़व्वाल की तरफ़ न होकर ख़ुदा की तरफ़ हो और नज़रें झुकी हुई हों।
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने समाअ’ की तीन शर्तें भी बताई हैं –
इख़वान – ये शब्द अरबी ज़बान का है और अख़ का बहुवचन है। अख़ का अर्थ भाई होता है अर्थात क़व्वाली ऐसे लोगों के बीच होनी चाहिए, जो हम-ख़याल हों।
(अगर लोग हम-ख़याल न हों तो क़व्वाली से पहले उन्हें कुछ क़िस्से या आध्यात्मिक बातें सुनाकर उनका ध्यान क़व्वाली की तरफ़ लाना चाहिए। निज़ामी बंसरी में एक वाक़िआ आता है जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत ख़्वाजा तूसी (मटका पीर) की ख़ानक़ाह पर महफ़िल-ए-समाअ के लिए तशरीफ़ लाते हैं। वहाँ जब क़व्वाली शुरू होती है तो लोगों में वो ज़ौक़ पैदा नहीं होता जो हज़रत की ख़ानक़ाह पर होता था। हज़रत क़व्वालों को रुकने का इशारा करते हैं और लोगों को सूफ़ी बुज़ुर्गों की बातें सुनाना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में जब लोगों के दिल एक तरफ़ माइल हो गए तब हज़रत ने क़व्वालों को हुक्म दिया कि वो अब क़व्वाली शुरू करें। क़व्वाली शुरू हुई और सब लोगों की कैफ़ियत देखने लाइक़ थी।)
मकान – क़व्वाली जहाँ हो वो जगह साफ़-सुथरी हो और किसी को कोई तकलीफ़ न पहुँचे।
ज़मान – मुनासिब वक़्त हो। लोग अपनी इबादत से फ़ारिग़ हो चुके हों।
क़व्वाली के बीच में मज़ाहिया जुमलों का इस्तेमाल भी वर्जित था।
क़व्वाली के दौरान वज्द की हालत को चिश्ती मलफूज़ात में यूँ व्यक्त किया गया है कि रोज़-ए-अलस्त को जब ख़ुदा ने रूहों से पूछा – क्या मैं तुम्हारा ख़ुदा नहीं हूँ ? इस पर रूहों ने जवाब दिया था – हाँ ! आप ही हमारे ख़ुदा हैं ! सियर-उल-औलिया के अनुसार ये जवाब शाब्दिक भी हो सकता है, मानसिक भी और हार्दिक भी। जब क़व्वाल की ख़ूबसूरत आवाज़ भीतर जाती हैं तो रूह को अपने उसी सनातन प्रेमी की याद आती है और वो रोज़-ए-अलस्त की तरह ही जवाब देती हैं। ये जवाब कंधे हिलाकर, सर हिलाकर या वज्द की कैफ़ियत की सूरत में होता है।
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने समाअ की कैफ़ियत को बड़े ख़ूबसूरत शब्दों में बयान किया है –
समाअ’ के दौरान एक कैफ़ियत ऐसी होती है कि अगर कोई सिर में कील ठोक दे तो भी पता न चले, पर इससे भी बढ़कर एक कैफ़ियत होती है जिसमें अगर पैरों के नीचे गुलाब की एक पंखुड़ी भी पड़ जाए तो इंसान को पता चल जाए। ये कैफ़ियत सबसे आला दर्जे की होती है।
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ क़व्वाली में वाध्य यंत्रों का इस्तेमाल लोगों के हृदय तक शायरी का ज़्यादा प्रभाव डालने के लिए मान्य था। हज़रत के मुरीदों में कुछ जैसे – हज़रत अमीर ख़ुसरौ, ख़्वाजा बुर्हानुद्दीन गरीब और ख़्वाजा हसन अला सिजज़ी ने अपनी मजलिसों में वाध्य यंत्रों के प्रयोग की अनुमति दे रखी थी जबकि दूसरे मुरीद जैसे–ख़्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ दिल्ली ने साज़ों के प्रयोग पर रोक लगा रखी थी।
क़व्वाली को सीना-ब-सीना याद रखने की ज़िम्मेदारी ने ही क़व्वाल घरानों को जन्म दिया। क़व्वाली सुनने की एक मात्र जगह पहले ख़ानक़ाह या दरगाह होती थी जहाँ हर शाम क़व्वाल सूफ़ी बुज़ुर्गों के कलाम पढ़ते थे और लोग उन्हें अपने दिलों में भर कर घर लौट आते थे। सूफ़ी कलाम शब्द प्रधान होते हैं इसलिए वहाँ बैठे सामईन के दिल से हर शेर या रुबाई पर आह ! निकलती थी। सालाना उर्स के अवसर पर कई क़व्वालों को सुनने का अवसर लोगों को मिलता था और इस अवसर पर हज़ारों लोग दूर-दूर से सूफ़ी संगीत सुनने आते थे। सैकड़ों सालों में क़व्वाली की मक़बूलियत कभी कम नहीं हुई बल्कि इस में दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा होता रहा।
सब कुछ यूँ ही चल रहा था कि एक अविष्कार ने क़व्वाली की इस विशुद्ध हिन्दुस्तानी विधा को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। किसी ने ये नहीं सोंचा था कि एक आवाज़ को दोबारा भी सुना जा सकता है। क़व्वाल अपने उस्तादों से एक बंदिश सीखने के लिए पूरी ज़िन्दगी उन की सेवा में बिता देते थे। किस ने सोचा था कि वोी बंदिशें अब कभी भी और कहीं भी सुनी जा सकेंगी। ये थामस एडिसन द्वारा ग्रामोफ़ोन का आविष्कार था जिसे पहले फ़ोनोग्राफ़ कहा जाता था। बाद में बर्लिनर ने इस ग्रामोफ़ोन में कुछ ज़रूरी सुधार किए और ग्रामोफ़ोन कंपनी की शुरुआत हुई। जल्दी ही आवाज़ के इस जादुई बक्से ने पूरे पश्चिम को अपना दीवाना बना लिया।
हिंदुस्तान में इस की शुरुआत उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में हुई जब इंडियन ग्रामोफ़ोन एँड टाइपराइटर कंपनी की शुरुआत हुई। उस के बाद बीसवी सदी में कोलंबिया, ट्विन और His Masters Voice इसी का नाम है।
रिकॉर्डिंग उद्योग की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, ग्रामोफ़ोन कंपनी ने 1901 में कलकत्ता में अपना कार्यालय स्थापित किया। भारत से कंपनी को बड़ी उम्मीदें थीं। एक साल के भीतर, इसके प्रमुख तकनीकी विशेषज्ञ एफ.डब्ल्यू. गैसबर्ग अपनी रिकॉर्डिंग टीम के साथ कलकत्ता पहुँचे। उस समय, उन्हें वहाँ जाना पड़ता था जहाँ प्रदर्शन करने वाले कलाकार होते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्राऐं की और 600 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए। भारत की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में 500 से अधिक कलाकारों को रिकॉर्ड किया गया। उनमें से अधिकांश को एक मिनट से लेकर तीन मिनट तक के गाने रिकॉर्ड करने का प्रशिक्षण देना पड़ता था।
शुरुआती वर्षों में रिकॉर्डिंग पीतल के हॉर्न की सहायता से की जाती थीं और कलाकारों को ऊँची आवाज़ में गाना पड़ता था। बाद में 1925 में, इलेक्ट्रिक कार्बन माइक्रोफ़ोन के प्रयोग ने लोक और हास्य गीतों, क़व्वाली, भजन और येाँ तक कि संवादों के साथ पूरे नाटक को रिकॉर्ड करने की एक नई प्रथा को जन्म दिया। कुछ वर्षों के भीतर, कई रिकॉर्डिंग कंपनियाँ सामने आईं, लेकिन ‘हिज मास्टर्स वॉयस’ लेबल के साथ ग्रामोफ़ोन सुनते हुए एक कुत्ते की छवि के ट्रेडमार्क के साथ ग्रामोफ़ोन कंपनी का 1970 के दशक तक भारत में लगभग एकाधिकार रहा। वर्ष 2000 में कंपनी का नाम बदलकर ‘सारेगामा इंडिया लिमिटेड’ कर दिया गया।
हिंदुस्तान में कंपनी का ध्यान दो विधाओं पर सब से पहले गया, पहला शास्त्रीय संगीत और दूसरी क़व्वाली। पहली विधा भारत में हज़ारों वर्षों से चली आ रही थी और क़व्वाली को भी छः सौ साल हो गए थे। इस कार्य में भी कई चुनौतियाँ थीं। क़व्वालों से कलाम रिकॉर्ड करवाना आसान नहीं था। उस समय के दूसरे संगीतकारों की तरह क़व्वाल भी इस मशीनी काम को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। कुछ लोगों को ये डर था कि ये माइक्रोफ़ोन हमेशा के लिए उन की आवाज़ छीन लेगा तो कुछ लोगों को ये लगता था कि हमारे संगीत को ये हम से छीन कर हमारी मर्ज़ी के बग़ैर दूसरे लोगों तक पहुँचा देगा जिस से हमारी रोज़ी-रोटी छिन जाएगी। कुछ लोगों का ऐतराज़ इस बात पर था कि उन की आवाज़ को होटलों, दुकानों और आम बाज़ारों में सुना जाएगा। क़व्वाली को सुनने के लिए जहाँ ख़ास लोग और ख़ास समय तक निर्धारित था वहाँ इसे सब तक पहुँचा देने की बात लोगों को समझ नहीं आ रही थी।
1902 ई. में सब से पहले तीन क़व्वालों का कलाम रिकॉर्ड किया गया जिन में प्यारू क़व्वाल, कालू क़व्वाल और फ़ख़्र-ए-आलम क़व्वाल थे। ये क़व्वाल देखते ही देखते हिन्दुस्तान भर में प्रसिद्ध हो गए। धीरे-धीरे बाकी क़व्वाल भी रिकॉर्डिंग कंपनी से जुड़ते गए और क़व्वालों का नाम और उनका काम शहरों और कस्बों से निकल कर हिंदुस्तान ही नहीं विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया।
शुरुआत में ज़्यादातर क़व्वाली ना’तिया (हज़रत पैग़म्बर मोहम्मद (PBUH) की शान में) होती थी लेकिन धीरे-धीरे क़व्वालों को ये एहसास हुआ कि उनके सुनने वालों का दायरा अब बढ़ रहा है। पहले क़व्वाली शहरों में बसे इलीट मुस्लिम वर्ग और ख़ानक़ाही लोगों को ध्यान में रख कर पढ़ी जाती थी लेकिन बाद में क़व्वालों को ये एहसास हुआ कि दरगाह में आने वाले लोगों में हिन्दुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। इस के बाद क़व्वालों ने भजन, ठुमरियाँ, देशभक्ति के गीत और हिन्दू-मुस्लिम एकता पर भी कलाम पढ़े।
इंडियन ग्रामोफ़ोन एँड टाइपराइटर कंपनी ने सर्वप्रथम दिल्ली में काम शुरु किया और हिज मास्टर्स वाइस ने भी दिल्ली में अर्से तक क़व्वाली रिकॉर्ड की। इस समय कालू क़व्वाल (कलकत्ता) का कलाम सब से ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। अन्य लोकप्रिय क़व्वालों में प्यारेलाल (दिल्ली), कल्लन क़व्वाल (मेरठ), मुमताज़ हुसैन (दिल्ली) अब्दुल रज़्ज़ाक़ (अलीगढ) हबीब पेंटर और कुछ आगरे के क़व्वाल थे।
सन 1925 ई. में कोलम्बो ग्रामोफ़ोन कंपनी ने बम्बई में क़व्वाली को रिकॉर्ड करना शुरु किया। इस कंपनी ने एम. बशीर क़व्वाल (हैदराबाद), अब्दुल रहमान काँचवाला, सालेह मोहम्मद, इस्माइल आज़ाद और शहाबुद्दीन हैदराबादी के रिकॉर्ड बनाए। बाद में दूसरे क़व्वालों को भी येाँ रिकॉर्ड किया गया। आगे चलकर ये कंपनी हिज मास्टर्स वाइस कंपनी में मिल गई।
आगे चलकर जो दौर आया वो नई तरक़्क़ी पसंद शाइरी,फ़िल्म और जासूसी नॉवेल का दौर था। इन का असर क़व्वाली पर भी पड़ा। क़व्वालों ने बड़ी आसानी से फ़िल्मी संगीत में अपना स्थान बना लिया वहीं जासूसी उपन्यासों की तरह एक नई तज़मीन का आग़ाज़ किया। इस तज़मीन में पंद्रह-बीस या कई बार इस से भी ज़्यादा मिसरों की नज़्म पढ़ी जाती थी जिस का मक़सद एक इन्तिज़ार की कैफ़ियत पैदा करना था। फिर इसी इन्तिज़ार को एक ऊँचाई तक पहुँचा कर आख़िरी शेर में क्लाइमेक्स पैदा कर दिया जाता था। आज़ाद शायरी का सिक्का चल रहा था इस लिए बड़ी आसानी से क़व्वाल शायर भी बन गए। नई नज़्म ने क़व्वालों को हर पाबन्दी से आज़ाद कर दिया। इस से धीरे-धीरे ख़ानक़ाही क़व्वाली कम होने लगी। आगे चलकर तो क़व्वालों की दो चौकियाँ भी आमने सामने बिठाई जाने लगीं और बैतबाज़ी को क़व्वाली के नाम पर पढ़ा जाने लगा लेकिन ये जो भी था क़व्वाली नहीं थी।
हिज मास्टर्स वाइस ने बम्बई में भी आपनी एक शाखा शुरु की जो सिर्फ़ गुजराती और मराठी गीतों को रिकॉर्ड करती थी। उस के गुजराती संभाग में तबला-नवाज़ उस्ताद क़ासिम अब्दुल्ला काम करते थे जो आगे चल कर इस के इंचार्ज बन गए। उन्होंने हिंदुस्तान भर के क़व्वालों को ढूँढ निकाला और दिल्ली ऑफिस को बम्बई में क़व्वाली रिकॉर्ड करने पर मजबूर किया। इस से पहले बम्बई में उर्दू और हिंदी की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। इस बात का कुछ विरोध भी हुआ लेकिन इस विरोध के वावजूद हिज मास्टर्स वाइस की मुंबई शाखा ने सन 1938 ई. में पहली क़व्वाली रिकॉर्ड की जिस के फ़नकार बशीर क़व्वाल (पुणे) थे और कलाम कौसर मेरठी का था जिस के बोल थे – प्यारे अहमद-ए-मुख़तार। इस रिकॉर्ड की दूसरी ओर बशीर क़व्वाल द्वारा पढ़ा गया दूसरा कलाम था – तुम बिन कौन संभाले, मोरी नैय्या डगमग डोले। इस के बाद अब्दुल रहमान काँचवाला, मोहम्मद सालेह, शैख़ अहमद (पुणे), सैयद जाफ़र क़व्वाल, शैख़ लाल (नागपुर) अजीम प्रेम रागी और इस्माईल आज़ाद की क़व्वालियों का दौर शुरु हुआ जो आगे भी ज़ारी रहा।
इनके बाद तो क़व्वाली के फ़नकारों की जैसे झड़ी लग गई। इन में कुछ को बड़ी लोकप्रियता हासिल हुई। कुछ नाम हैं – पद्म श्री अज़ीज़ अहमद ख़ान वारसी, अब्दुल रब काविश, शंकर शम्भू, युसूफ आज़ाद, जानी बाबू,बन्दे हसन, क़लन्दर आज़ाद, शफ़ी नियाज़ी, अज़ीज़ नाज़ाँ, छोटे यूसुफ़ आज़ाद, शकीला बानो (भोपाल), कामिनी देवी, शकीला बानो (पुणे), रज़िया बानो, शमीम बानो और राशिदा ख़ातून आदि।
ख़ानक़ाहों और दरगाहों पर आम तौर पर महिला क़व्वालों को कलाम की इजाज़त नहीं थी। ग्रामोफ़ोन ने महिला क़व्वालों को ये अवसर दिया और देखते ही देखते कई महिला क़व्वाल प्रसिद्ध हो गई।
इन क़व्वालियों को रिकॉर्ड करने और क़व्वालों की प्रसिद्धि का एक स्याह पक्ष भी था। ये कंपनियाँ विशुद्ध व्यावसायिक कंपनियाँ थी जिन्हें कलाम के मेयार और उन की शुद्धता से कोई मतलब नहीं था। उनके लिए आवाम की पसंद सर्वोपरि थी। जिस प्रकार क़व्वाल को बरसों के रियाज़ के बाद स्वरों पर नियंत्रण प्राप्त होता है उसी प्रकार श्रोताओं को भी कानों के रियाज़ की ज़रुरत होती है। फिर क़व्वाली तो हमेशा से हम ख़्याल सामेईन के बीच ही पढ़ी जाती रही है। एक समय ऐसा भी आया कि क़व्वाली लोकप्रिय तो बहुत हुई लेकिन कलाम का मेयार बिल्कुल नीचे गिर गया। क़व्वाली के लिए ये अपनी राह से भटक जाने या अपनी एक नई राह बनाने का समय था। क़व्वालों ने इस नई राह को भी ढूंढ लिया और देशभक्ति की क़व्वालियाँ पढ़ी जाने लगीं।
आज़ादी के बाद भारत की कई ख़ानक़ाहों से क़व्वालों की हिज्रत हुई और क़व्वाली के कई घराने पाकिस्तान जा कर बस गए। ग्रामोफ़ोन के बाद रेडियो की बारी थी जो हिंदुस्तान के घर-घर में पहुँच गया था। पाकिस्तान रेडियो ने जहाँ क़व्वाली के प्रचार-प्रसार पर धयन दिया वोीँ आल इंडिया रेडियो ने संगीत की अन्य विधाओं को ज़्यादा प्रमुखता दी। मज़हबी क़व्वाली धीरे-धीरे धर्मनिरपेक्ष हो चली थी। येी इसका वास्तविक रूप भी था।
कुछ क़व्वाल ऐसे भी थे जिन्होंने लोकप्रियता में बड़े-बड़े उस्ताद गायकों को भी पीछे छोड़ दिया। 1975 में जब सोने का भाव 540 रूपये प्रति तोला हुआ करता था उस दौर में एक क़व्वाल ऐसे भी थे जिन्होंने कलकत्ता के कला मंदिर में अपने एक प्रोग्राम के लिए 1,80,000 रूपये की राशि ली थी। इनकी प्रसिद्धि का आ’लम ये था कि उन की राँची यात्रा के दौरान लोगों ने ट्रेन रोक दी थी ताकि इनसे एक बार हाथ मिलाने का मौक़ा’ मिल सके। 1977 में दोबारा झांसी में ट्रेन रोकनी पड़ी और लोगों ने इनका इस्तिक़बाल किया। ये क़व्वाल थे अ’ज़ीज़ नाज़ाँ जिन्हें ‘बाग़ी क़व्वाल’ भी कहा जाता है।
अ’ज़ीज़ नाज़ाँ (7 मई 1938- 8 अक्टूबर सन् 1992 ई.) मुंबई के एक प्रतिष्ठित मालाबारी मुस्लिम परिवार में पैदा हुए। घर में संगीत सुनने और गाने की सख़्त मनाही थी। इस माहौल में भी उन्होंने चोरी-छिपे संगीत की शिक्षा जारी रखी। हर बार जब वो गाते-बजाते पकड़े जाते तो उन की जम कर पिटाई होती पर कलाकार वो क्या जो समाज के विरोध से कला को छोड़ दे! उनके पिता का जब देहान्त हुआ तब अ’ज़ीज़ 9 साल के थे। उस के बा’द ही वो ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो गए। कुछ ही समय बा’द वो प्रसिद्ध क़व्वाल इस्माईल आज़ाद के सानिध्य में आ गए जो अपनी क़व्वाली ‘हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने’ से फ़िल्म जगत में अपनी धाक जमा चुके थे। धीरे धीरे अ’ज़ीज़ नाज़ाँ की ख्याति बढ़ने लगी और उन्हें स्वतंत्र क़व्वाल के रूप में जाना जाने लगा। 1962 में उन्होंने ग्रामोफ़ोन कंपनी के साथ क़रार पर हस्ताक्षर किए।
1962 अ’ज़ीज़ के लिए बड़ा भाग्यशाली वर्ष रहा। उन्होंने ‘जिया नहीं माना’ रिकॉर्ड किया जो लोगों के बीच बड़ा प्रसिद्ध हुआ। सन्1968 ई. में उन्होंने ‘निग़ाह-ए-करम’ रिकॉर्ड किया जिसे क़व्वाली पसंद करने वालों ने ख़ूब सराहा। उन्हें अस्ल मायनों में सफलता 1970 में मिली जब कोलंबिया म्यूज़िक कंपनी द्वारा ‘झूम बराबर झूम’ रिलीज़ किया गया और इस गाने नें सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सन्1973 ई. में फ़िल्म ‘मेरे ग़रीब नवाज़’ को इसी गाने की ब-दौलत अपार सफलता मिली। उस समय प्रचलित रेडियो प्रोग्राम बिनाका गीत माला में ‘झूम बराबर झूम’ कई हफ़्तों तक पहले नंबर पर रहा था।
झूम बराबर झूम ने अ’ज़ीज़ नाज़ाँ की गायकी को जन मानस के दिलों में सदा के लिए स्थापित कर दिया था। इस गाने के बा’द अ’ज़ीज़ नाज़ाँ ने कई फ़िल्मों में ब-तौर प्ले बैक सिंगर भी कार्य किया जिनमें रफ़ू चक्कर (1975), लैला मज्नूँ (1976), फ़क़ीरा (1976) और तृष्णा (1978) आदि उल्लेखनीय हैं।
जीवन के शुरूआ’ती दिनों में अ’ज़ीज़ नाज़ाँ उस्ताद बड़े ग़ुलाम अ’ली ख़ान साहिब के घर पर चले जाया करते थे जो उनके घर के पास ही भिन्डी बाज़ार में स्थित था। बड़े ग़ुलाम अ’ली ख़ान साहिब के येाँ संगीत के विद्वानों का ताँता लगा रहता था। अ’ज़ीज़ उन्हें बैठ कर धंटों सुना करते थे। उन्होंने येाँ बैठ कर शास्त्रीय संगीत की बारीकियाँ सीखीं। बा’द में वो मोहम्मद इब्राहीम ख़ान साहिब के शागिर्द बन गए जो म्यूज़िक डायरेक्टर ग़ुलाम मोहम्मद साहिब के छोटे भाई और नौशाद साहिब के असिस्टेंट थे। कुछ समय बा’द उन्हें प्रसिद्ध म्यूज़िक डायरेक्टर रफ़ीक़ ग़ज़नवी साहिब से संगीत सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो मदन मोहन, ग़ुलाम मोहम्मद और उनके पूर्व उस्ताद मोहम्मद इब्राहीम ख़ान साहिब के गुरु रह चुके थे।
नाज़ाँ मालाबारी थे और उन की मातृभाषा मलयालम थी। उन्होंने औपचारिक शिक्षा गुजराती माध्यम से पूरी की थी। क़व्वाली पढ़ने के लिए उन्होने उर्दू शाए’र सादिक़ निज़ामी से उर्दू शाए’री की बारीकियाँ सीखीं। अ’ज़ीज़ नाज़ाँ को शाए’री का बड़ा शौक़ था। उन की निजी लाइब्रेरी में हज़ारों किताबें थीं और वो हर महीने पाकिस्तान और भारत के प्रकाशकों से 50- 60 नयी किताबें मंगवाते थे। कई प्रसिद्ध शाए’र यथा बशीर बद्र, मख़मूर सई’दी, मे’राज फ़ैज़ाबादी, कृष्ण बिहारी नूर, वसीम बरेलवी, मुज़फ़्फ़र वारसी, मुनव्वर राणा आदि उनके ख़ास दोस्तों में से थे। हालाँकि उन्होंने ज़्यादातर कलाम क़ैसर रत्नागिरवी,हसरत रूमानी और नाज़ाँ शोलापुरी के पढ़े हैं परन्तु मंच पर उन्हें याद हज़ारों शे’र लोगों को रोमांचित कर देते थे।
अ’ज़ीज़ नाज़ाँ बड़े प्रयोगधर्मी क़व्वाल थे। उन्होंने क़व्वाली में कई ऐसे प्रयोग किये जो पहले कभी नहीं हुए थे, यही कारण है कि इन्हें बाग़ी क़व्वाल भी कहा जाता है। 1983 में उन्होंने मुंबई के सारे क़व्वालों को एक साथ मिला कर ‘The Bombay Qawwal Association’ की स्थापना की लेकिन उन की बीमारी और तदुपरान्त मृत्यु के पश्चात ये संगठन टूट गया।
1978 में अ’ज़ीज़ नाज़ाँ साहिब की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। 1982 में HMV रिकार्ड्स के बैनर तले उनका एक और प्रसिद्ध गाना –‘चढ़ता सूरज’ रिलीज़ हुआ जिसने सफ़लता से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ ही समय बा’द HMV से कुछ विवादों के फलस्वरूप उन्होंने अपना क़रार तोड़ लिया और वीनस कैसेट्स के साथ क़रार-नामे पर हस्ताक्षर किये। उन्होंने अपना पहला एल्बम इस कम्पनी के साथ ‘हंगामा’ के नाम से रिकॉर्ड किया। 1992 में रिकॉर्ड हुआ गाना ‘मैं नशे में हूँ’ उन की आख़िरी रिकॉर्डिंग थी।
1992 में उन की तबीअ’त ख़राब हुई और इसी साल 8 अक्टूबर को अ’ज़ीज़ नाज़ाँ इस जहान-ए-फ़ानी से कूच कर गए।
अ’ज़ीज़ नाज़ाँ की क़व्वाली शुरुआ’त में इस्माईल आज़ाद की शैली का अनुकरण करती मा’लूम पड़ती है लेकिन बा’द में उस्ताद बड़े ग़ुलाम अ’ली और उस्ताद सलामत अ’ली साहिब के सानिध्य में आने के बा’द उन की गायकी में शास्त्रीय संगीत का गहरा प्रभाव दिखता है।अ’ज़ीज़ नाज़ाँ की को हज़ारों शे’र ज़बानी याद थे और उनका प्रयोग क़व्वाली पढ़ने के दौरान वो बड़ी ख़ूब-सूरती से किया करते थे। उन का संगीत संयोजन उस समय के हिसाब से काफ़ी आधुनिक था। 1969 में उन्होंने झूम बराबर झूम की रिकॉर्डिंग की। जहाँ उस समय तक क़व्वाल अपनी क़व्वाली में सिर्फ़ हारमोनियम और तबले का ही प्रयोग किया करते थे, अ’ज़ीज़ नाज़ाँ ने पहली बार क़व्वाली में मेंडोलिन, गिटार, कोंगो, आदि आधुनिक वाध्यों का प्रयोग किया था। 1971 में उन्होंने अपने गीत ‘मस्ती में आ पिए जा’ में पहली बार इलेक्ट्रिक गिटार और इलेक्ट्रॉनिक साउंड इफ़ेक्ट्स का प्रयोग किया था, फ़िल्म इंडस्ट्री में 70 और 80 के उत्तरार्ध में कल्याण जी, आर.डी. बर्मन साहिब और बप्पी लाहिरी ने इलेक्ट्रॉनिक धुनों का प्रयोग शुरू किया जबकि अ’ज़ीज़ नाज़ाँ ये काम 70 के दशक की शुरुआ’त में ही कर चुके थे।
अ’ज़ीज़ नाज़ाँ ने कई महान संगीतकारों के साथ काम किया और नए नए प्रयोग किए। उन्होंने पहली बार सितार और मेंडोलिन का फ़्यूज़न अपने गीत ‘तेरी नज़र का ओ दिलदारा’ में किया और इस गाने को अमर कर दिया। उन के अंतिम एल्बम ‘मैं नशे में हूँ’ में कुछ गानों में पाश्चात्य प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया गया था जो आगे चलकर कई संगीतकारों के लिए प्रेरणास्रोत बना। अ’ज़ीज़ नाज़ाँ को भारत में क़व्वाली के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है।
भारत-चीन युद्ध के समय जब पूरा देश एकता के सूत्र में बंध गया था,उस नाज़ुक दौर में अवाम को जगाने और सैनिकों का हौसला बढ़ाने का बीड़ा क़व्वाल हबीब पेंटर ने उठाया। उन की क़व्वालियों से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हबीब पेंटर को बुलबुल-ए-हिन्द की उपाधि से सम्मानित किया। हबीब अपने शुरूआती दिनों में घरों को पेंट करने का काम करते थे। येी कारण था कि उनका नाम हबीब पेंटर पड़ गया। हबीब खुद को हज़रत अमीर ख़ुसरौ का मुरीद कहते थे। इन की क़व्वालियाँ बड़ी प्रसिद्ध थीं। बहुत कठिन है डगर पनघट की और नहीं मालूम जैसी क़व्वालियों की उन दिनों धूम थी। हबीब ने कभी फ़िल्मों के लिए नहीं गाया। इन की मृत्यु 22 फरबरी 1987 ई. को हुई। उनके नाम पर अलीगढ़ में सिविल लाइन्स के पास एक पार्क का नामकरण किया गया है। उनके बा’द उनके बेटे अनीस पेंटर और नाती ग़ुलाम हबीब उन की इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।
शंकर-शम्भू दो सगे भाई थे जिनकी युगल क़व्वाली ने दुनिया भर को दीवाना बनाया।उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव चंदौसी में हुआ था। बड़े भाई शंकर और शम्भू ने सात वर्ष की आयु में अपने पिता उस्ताद चुन्नीलाल से संगीत की विधिवत शिक्षा शुरु की थी।उनके पिता प्रख्यात शास्त्रीय गायक थे और अपना नौटंकी ग्रुप चलाते थे। पूरे उत्तर प्रदेश से उस ग्रुप में पचास सदस्य थे। बाद में दोनों भाइयों ने जयपुर घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद मोहनलाल से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। उन्होंने उर्दू-फ़ारसी और अरबी भी सीखी।
एक बार शंकर और शम्भू ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर हाज़िरी देने पहुँचे। उन्हें वहाँ गाने का मौक़ा नहीं दिया गया क्यूंकि एक तो वो नए थे और दूसरे क़व्वालों की एक लंबी फ़ेहरिस्त कतार में खड़ी थी। ये देखकर बड़े भाई शंकर ने दरगाह की सीढ़ियों पर ही उपवास शुरू कर दिया। वो तीन दिनों तक भूखे-प्यासे ख़्वाजा साहिब की चौखट पर बैठे रहे। उन्होंने अपनी अंतिम साँस तक उपवास नहीं तोड़ने का प्रण लिया। आख़िरकार दरगाह कमिटी के लोगों ने दोनों भाइयों को उर्स के अंतिम दिन महफ़िल ख़ाना में गाने की इजाज़त दे दी। जब दोनों भाइयों ने ‘महबूब-ए-किब्रिया से मेरा सलाम’ गाना शुरू किया तो सारी जनता मंत्रमुग्ध थी। कई लोग वहाँ रोने लगे और इन क़व्वालों ने सबका दिल जीत लिया। उसी दिन उन्हें क़व्वाल की पद्वी मिली और उस दिन से दोनों भाई शंकर शम्भू क़व्वाल के नाम से प्रसिद्ध हुए।
उसी महफ़िल में कलाम सुनकर रोते हुए लोगों में से एक थे मदर इंडिया फ़िल्म के निर्माता महबूब ख़ान साहिब। उन्होंने इन दोनों भाइयों को मुंबई आमंत्रित किया और महबूब स्टूडियो के उद्घाटन समारोह में गाने का आग्रह किया। शंकर शम्भू ने आलम आरा, तीसरी कसम, बरसात की रात, शान ए ख़ुदा, लैला-मज्नूँ, मंदिर मस्जिद जैसी कई प्रसिद्ध फ़िल्मों को अपनी सुरीली आवाज़ से सजाया है। शंकर की मृत्यु सड़क दुर्घटना में सन् 1984 में हो गयी जबकि शम्भू क़व्वाल ने 1989 में इस संसार को अलविदा कहा।
ख़्वाजा हसन निज़ामी साहिब ने दिल्ली के एक वाइज़ क़व्वाल का ज़िक्र किया है। वाइज़ के कलाम हमें बहुत दिनों तक नहीं मिले। आख़िरकार हमारे अज़ीज़ हज़रत हसन नवाज़ शाह साहिब ने उनके कलाम का मजमुआ हमें पाकिस्तान से स्कैन करवा कर भेजा।इस किताब में वाइज़ क़व्वाल के कलाम तो हैं ही साथ-साथ हसन निज़ामी ने उनके बारे में भी लिखा है। हम पाठकों के लिए ख़्वाजा हसन निज़ामी द्वारा लिखित वो परिचय इस किताब में शामिल कर रहे हैं-
“मुझे ठीक मालूम नहीं है कि वाइज़ क़व्वाल की पैदाइश कहाँ की है लेकिन अब वो अरसा दराज़ से हैदराबाद दकन में रहते हैं। आज से 15–16 बरस पहले मैं ने उनको हज़रत मौलाना शैख़ निज़ाम-उद्दीन साहिब चिश्ती अहमदाबादी के साथ देखा था और गाना सुना था। इस के बाद हैदराबाद में उनका गाना सुना और मेरे दिल पर एक ख़ास असर उनके गाने का हुआ। मैं ने उनको वाइज़ क़व्वाल का ख़िताब दिया। इस के बाद उनको हर साल हज़रत महबूब-ए-इलाही साहिब के उर्स में बुलाया जाने लगा और हाज़िरीन-ए-मजलिस को उन की क़व्वाली में इस क़दर लुत्फ़ आया कि एक बड़े मुनकिर क़व्वाली अहल-ए-हदीस साहिब भी पोशीदा तौर से उन की क़व्वाली सुनने आए और मजलिस से बाहर जाकर उन्होंने कहा कि भई उस शख़्स ने ख़िलाफ़-ए-शरीअत बातें बहुत गायीं मगर इन्साफ़ की बात ये है कि मज़ा बहुत आया। अगर फिर कोई तख़्लिया की मजलिस मुम्किन हो तो मैं एक सौ रुपये तक इस गाने के लिए ख़र्च करूँगा।
देहली के हिन्दू हज़रात में मुस्लमानों से ज़्यादा वाइज़ क़व्वाल की मक़्बूलियत हुई और जनाब राय बहादुर लाला पारस दास साहिब मजिस्ट्रेट ने उनको अरसा तक अपने मकान पर ठहराए रखा।
मालूम हुआ है कि आला हज़रत हुज़ूर निज़ाम भी वाइज़ क़व्वाल के गाने को पसंद फ़रमाते हैं और हिज़ हाइनेस महाराजा साहिब अलवर तो बार-बार उन को अपनी रियासत में बुला कर सुनते हैं और हिन्दुस्तान की अक्सर मशहूर ख़ानक़ाहों में उन की शोहरत है और वो बुलाए जाते हैं। उनको अपने मुर्शिद के फ़ैज़ान-ए-सोहबत-ओ-तर्बियत से ये कमाल हासिल हुआ है और उनके मुर्शिद ने उनको ख़िलाफ़त भी दी है और वो बैअत भी करते हैं । मुझे याद है कि पंद्रह साल पहले जब मैं ने उनको देखा तब भी वो नमाज़ पंज गाना और तहज्जुद के पाबंद थे और अज़कार अश्ग़ाल करते थे।
मैं अच्छे क़व्वालों को तसव्वुफ़ का लेक्चरार और मुअल्लिम मानता हूँ और चूँकि वाइज़ क़व्वाल हक़ीक़ी माअनों में क़व्वाल हैं इस वास्ते मैं ने उनको वाइज़ क़व्वाल का ख़िताब दिया है कि वो अपनी क़व्वाली में तसव्वुफ़ का वाज़ कहते हैं”
भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी लोगों के दिलों में क़व्वाली के प्रति वोी दीवानापन था। पहले भारत के क़व्वालों के रिकार्ड्स पाकिस्तान में भी ख़ूब सुने जाते थे लेकिन सत्तर के दशक के बाद पाकिस्तानी क़व्वालों ने क़व्वाली की प्रसिद्धि के नए आयाम स्थापित कर दिए। इन क़व्वालों में ग़ुलाम फ़रीद साबरी, मक़बूल अहमद साबरी, अज़ीज़ मियाँ क़व्वाल आदि प्रसिद्ध हैं।
ग़ुलाम फ़रीद साबरी का जन्म 5 अप्रैल 1930 ई. में हरियाणा के रोहतक ज़िले के एक गाँव कल्याण में हुआ था। आप का विसाल सन् 1994 ई. में कराची में हुआ। 70 से 90 के दशकों में साबरी बंधुओं का बोलबाला रहा। इन्हें शहंशाह-ए-क़व्वाली की उपाधि मिली थी। उनका परिवार चिश्ती सूफ़ी सिलसिले के साबरी संप्रदाय से सम्बंधित है इसलिए इनका उपनाम साबरी है। ग़ुलाम फ़रीद साबरी की परवरिश और शिक्षा-दीक्षा ग्वालियर में हुई। छः साल की उम्र में इन्होने अपनी औपचारिक संगीत शिक्षा अपने पिता इनायत हुसैन साबरी से शुरू की। विधिवत शिक्षा शुरू करने से पहले पिता-पुत्र ने ग्वालियर के प्रसिद्ध सूफ़ी हज़रत गौस ग्वालियरी की दरगाह पर हाज़िरी दी थी।
1947 ई. में विभाजन की त्रासदी से ये परिवार भी गुज़रा। उन का परिवार अपना मूल निवास छोड़ कर कराची आ गया। उन्हें कराची के शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। वहाँ परिस्थितियाँ भयावह थीं। भोजन का कोई इन्तिज़ाम न था। ग़ुलाम फ़रीद साबरी को सड़क बनाने के लिए चट्टानों को तोड़ने की नौकरी मिली। आख़िरकार वो बीमार हो गए। उन्हें चिकित्सकों ने बताया कि फेफड़ों की स्थिति बहुत नाज़ुक हो चली है जिस की वजह से वो कभी क़व्वाली नहीं पढ़ पाएँगे। उन्होंने लेकिन हार नहीं मानी और लगातार अभ्यास से उन की आवाज़ बिल्कुल सही हो गई। उन्होंने अपने भाइयों मक़बूल अहमद साबरी, कमाल अहमद साबरी और महमूद ग़ज़नवी साबरी के साथ साबरी ब्रदर्स ग्रुप की स्थापना की और देश भर में प्रदर्शन करते रहे। उनका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन सन 1946 ई. में कल्याण में सूफ़ी मुबारक शाह साहिब के सालाना उर्स के अवसर पर हुआ। पाकिस्तान जाने से पहले वो भारत में उस्ताद कल्लन ख़ाँ की क़व्वाल पार्टी में भी शामिल हुए थे। बाद में 1956 में जब वो अपने भाई मक़बूल अहमद साबरी की पार्टी में शामिल हुए तब इन्हें साबरी ब्रदर्स के नाम से जाना जाने लगा। सन 1958 ई. में EMI पाकिस्तान द्वारा रिलीज़ किया गया उनका पहला एल्बम -मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन की सब से ज़्यादा सुनी जाने वाली क़व्वालियों में -भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, ताजदार-ए-हरम आदि बहुत लोकप्रिय हैं।
उनका निधन 5 अप्रैल 1994 को कराची में दिल के दौरे की वजह से हुआ। उन की अंतिम यात्रा में 40,000 लोग शामिल हुए। उन्हें नाज़िमाबाद में पापोश क़ब्रिस्तान में दफ़नाया गया जहाँ उन की क़ब्र अपने पिता के बगल में स्थित है।
अज़ीज़ मियाँ का अंदाज़ सबसे अनोखा था। किसी क़व्वाल घराने से न होने पर भी उन्होंने क़व्वाली को एक ऐसे मुकाम पर पहुँचाया जिस की हदें आसमान की बुलंदियों को छूती नज़र आती हैं। इन्हें शहंशाह-ए-क़व्वाली भी कहा जाता है। इंश्क़ ए हक़ीक़ी को उन्होंने रूहानी शराब में डुबाकर आशिक़ों के लिए एक कभी न उतरने वाला नशा तैयार कर दिया जिसमे सुनने वाले का ख़ुमार कभी नहीं टूटता।
अज़ीज़ मियाँ का जन्म 17 अप्रैल 1942 को मेरठ में हुआ था। वो पाकिस्तान के प्रमुख क़व्वालों में एक थे। सब से लम्बी क़व्वाली पढ़ने का रिकॉर्ड (हश्र के रोज़ नाचूँगा (लगभग 150 मिनट)) भी अज़ीज़ मियाँ के नाम है। सन् 1947 ई. में उनका परिवार मेरठ से पाकिस्तान चला गया। दस साल की उम्र में उन्होंने लाहौर के दाता गंज बख़्श स्कूल में हारमोनियम सीखना शुरुअ किया। उन्होंने इस स्कूल में सोलह वर्षों तक प्रशिक्षण लिया। बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से उर्दू, अरबी और फ़ारसी सीखी। उन्होंने एम.ए. अंग्रेज़ी में किया था। अज़ीज़ मियाँ अपने गीत ख़ुद भी लिखा करते थे। 1966 में उन्होंने ईरान के शाह पहलवी के समक्ष प्रदर्शन किया। उन के प्रदर्शन से ख़ुश होकर शाह ने उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। ये से अज़ीज़ मियाँ को लोकप्रियता मिलनी शुरु हुई। अज़ीज़ मियाँ की क़व्वालियों में आह और वाह दोनों आकर समाहित हो जाते हैं। कहीं इन के कलाम दिल को झकझोर देते हैं तो कहीं इनकी शैली आप को मुग्ध कर देती है। मुल्तान में एक पुल का नाम अज़ीज़ मियाँ के नाम पर रखा गया है। वास्तव में क़व्वाली एक पुल का ही तो कार्य करती है। वो मनुष्य की चेतना को महाचेतन से मिला देती है जिस के बाद चेतना का स्वरुप भी महाचेतन का ही स्वरुप हो जाता है।
अज़ीज़ मियाँ का विसाल 6 दिसम्बर 2000 ई. को तेहरान में हुआ। वो ईरान सरकार के निमंत्रण पर वहाँ गए थे। उन की क़ब्र मुल्तान में है जहाँ हर साल मई के पहले गुरुवार को उर्स मनाया जाता है।
ग्रामोफ़ोन ने हिन्दुस्तानी क़व्वाली को उन बुलंदियों तक पहुँचाया जिस की वो हक़दार थी। क़व्वाली को पढ़ा-सुना तो बहुत गया लेकिन किताब की शक्ल में इसे सुरक्षित करने के प्रयास न के बराबर हैं। अगर इधर-उधर बिखरी और हज़ारों छोटे गुलदस्तों के रूप में दूसरे गीतों के साथ छपी क़व्वालियों को जमा किया जाए तो हज़ारों कलाम मिल सकते हैं।
–सुमन मिश्र
Guest Authors
- Aatif Kazmi
- Absar Balkhi
- Afzal Muhammad Farooqui Safvi
- Ahmad Raza Ashrafi
- Ahmer Raza
- Akhlaque Ahan
- Arun Prakash Ray
- Balram Shukla
- Dr. Kabeeruddin Khan Warsi
- Dr. Shamim Munemi
- Faiz Ali Shah
- Farhat Ehsas
- Iltefat Amjadi
- Jabir Khan Warsi
- Junaid Ahmad Noor
- Kaleem Athar
- Khursheed Alam
- Mazhar Farid
- Meher Murshed
- Mustaquim Pervez
- Qurban Ali
- Raiyan Abulolai
- Rekha Pande
- Saabir Raza Rahbar Misbahi
- Shamim Tariq
- Sharid Ansari
- Shashi Tandon
- Sufinama Archive
- Syed Ali Nadeem Rezavi
- Syed Moin Alvi
- Syed Rizwanullah Wahidi
- Syed Shah Tariq Enayatullah Firdausi
- Umair Husami
- Yusuf Shahab
- Zafarullah Ansari
- Zunnoorain Alavi