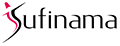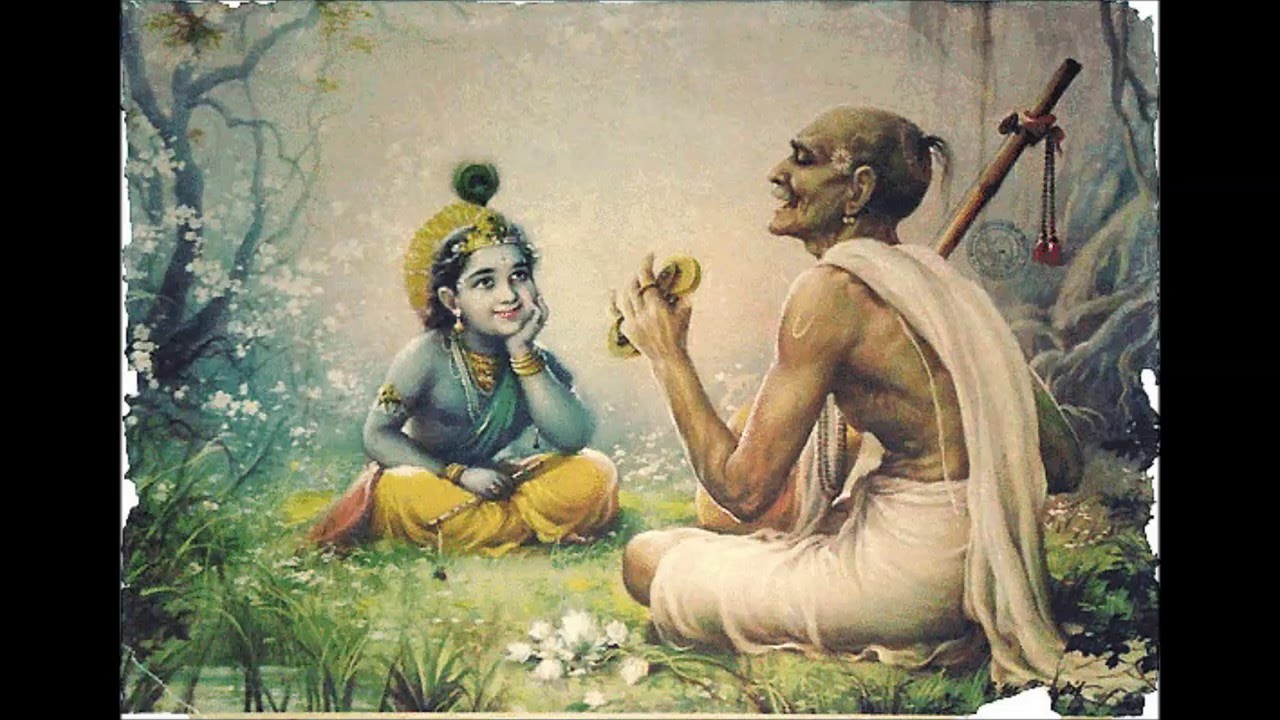
When Acharya Ramchandra Shukla met Surdas ji (भक्त सूरदास जी से आचार्य शुक्ल की भेंट)
 Sufinama Archive
March 22, 2019
Sufinama Archive
March 22, 2019
यह नक्षत्रों से भरा आकाश वियोगी जनों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। उस दिन भी तो आकाश नक्षरों से भरा हुआ था और मैं उस सुनील नभ के प्रत्येक तारे में अपनी प्रिया के रूप-वैभव की गरिमा देखने में तल्लीन होकर, महादेवी जी की यह पंक्ति- सो रहा है विश्व पर प्रिय तारकों में जागता है- मन ही मन गुन-गुना रहा था। तभी आकाश में बादल घिर आए। उन्होंने समस्त गगन को आच्छादितकर लिया और कुछ ही देर में वर्षा की झड़ी भी प्रारम्भ हो गई। मुझे करमे के भीतर आश्रय लेना पड़ा, उसी कमरे के भीतर, जिसका हवा में अबाध प्रवेश और आकाश के निरन्तर दर्शन के लिए सीकचों का खुला दरवाजा मेरे लिए कटघरे जैसा वातावरण उपस्थित कर देता था। उस दिन पता नहीं क्यों कालिदास के यक्ष की भाँति बादलों को दूत बना कर अपनी प्रिया के पास संदेश भेजने की बात मन में नहीं आई। हाँ, वर्षा की उन बूँदों को देख कर मन सूरदास की पंक्तियाँ—-
निशि दिन बरसत नयन हमारे।
सदा रहस पावस ऋतु हम पै जब ते श्याम सिधारे।।
अवश्य गुनगुना उठा। उसके बाद, एक नयी विचार परंपरा प्रवाहित हो उठी, सूरदास जी के विरह वर्णन को आचार्य शुक्ल ने बैठे-ठाले का काम और फालतू उमंग की अभिव्यक्ति कहा है… आचार्य शुक्ल तो गोस्वामी तुलसीदास के प्रति विशेष अनुरक्त थे…सूरदास जी पर तो उन्होंने कई स्थानों पर और गहरी चोटें की है… आज के किसी साहित्यकार जो जब उसका कोई कटु आलोचक मिल जाता है…अच्छी चोंचे लड़ती हैं…भक्त कवि सूरदास से यदि आचार्य शुक्ल की भेंट हो जाती है…तो…तो…सूरदास जी बहुत सौम्य व्यक्तित्व के थे…और शुक्ल जी अपने समस्त बुद्धि वैभव को लेकर भी श्रद्धालु प्रकृति के..चोंचे..चोंचें तो दोनों के ही नहीं थी…फिर भी दोनों का सम्मिलन…एक दूसरे के प्रति, गिला-शिकायत को लेकर…मनोरम तो होता ही…यही सब सोचते हुए नींद आ गई, और उस रात स्वप्न में अपनी प्रिया को न देख कर भक्त कवि सूरदास से आचार्य शुक्ल की भेंट का यह अपूर्व दृश्य देख बैठा। उसी की कुछ झलक सब के मनोरंजन के लिए यहाँ उपस्थित है।
भगवान् विष्णु के वैकुंठ-लोक के भक्ति नगर का एक सुन्दर-सा बँगलाः द्वार पर लिखा है, वृन्दावन। आकाश से परम मनोहर ज्योत्स्ना उतर रही है। लगता है जैसे सुधा की वर्षा हो रही है। शरद् पूर्णिमा के उस मधुर मादक वातावरण को तरंगित करता हुआ एक संगीत स्वर आ रहा हैः
ब्रज भयो महर कैं पूत जब यह बात सुनी।
सुनि आनन्दे सब लोग, गोकुल-गनक गुनी।।
सुनि धाई सब ब्रज नारि, सहज सिंगार किए।
तन पहिरे नूतन चीर, काजर नैन दिए।।
ते अपनैं-अपनैं मेल, निकसी भाँति भली।
मनु लाल मुनैयनि पाँति, पिंजरा तोरि चली।।
इस संगीत लहरी में डूबते उतराते हुए जिधर भी दृष्टि जाती है, कृष्ण की बाल लीला अथवा यौवन सुलभ चपलताओं का कोई-न-कोई प्रसंग सामने आ जाता है। कहीं कोई शिशु मणिमय आँगन में घुटनों के बल चलने का प्रयास कर रहा है। फिर दूसरे स्थल पर हम देखते हैं, वही बालक, कुछ और बड़ा होकर अपनी माता से चन्द खिलौना के लिए आग्रह पर अड़ा है। तभी पास से आता हुआ कुछ बच्चों का शरारत भरा स्वर सुनाई दिया। देखा तो एक छोटा-सा बालक, अपने से कुछ ही बड़े एक बालक के कंध पर खड़ा हुआ सामने के एक छोटे से भवन में सिकहर में टँगे दही के माठ को उतारने के प्रयत्न में लगा हैं। एक अन्य ओर दृष्टि जाती है तो दिखाई देता है- एक पन्द्रह सोलह वर्ष का नवयुवक झूले पर बैठी हुई नव-बाला को झोकें देकर ढुला रहा है, और उसके चारों ओर एकत्र उस नव-बाला की सखियाँ गीत गा रही हैं। सहसा कृष्ण राधा को, उनका हाथ बड़े स्नेह के साथ अपने हाथों में लेकर, उतार लेते हैं। सभी सखियाँ उन दोनों के चारों ओर एकत्र हो जाती हैं और तब रास-नृत्य प्रारम्भ हो जाता है।…
वृन्दावन के उस दिव्य वातावरण में न जाने कितनी देर तक मैं इस मनोहर दृश्यावली को देखता रहा। न जाने कितनी संगीत लहरियाँ भी कानों में आईं और गई। जब ध्यान टूटा तो संगीत के स्वर स्पष्ट हुएः
आजु निसि सोभित सरद सुहाई।
सीतल मंद सुगंध पवन बहे, रोम रोम सुखदाई।।
जमुना-पुलिन पुनीत, परम रुचि, रचि मंडली बनाई।
राधा वाम अंग पर कर धरि, मध्यहिं कुँवर कन्हाई।।
कुंडल संग……………
जिधऱ से यह स्वर लहरी आ रही थी, मैं उसी ओर बढ़ चला। उस वृन्दावन के बीच में स्थित एक छोटे से सामान्य से भवन के बरामदे में शीतल पाटी पर बैठा हुआ प्रौढ़ावस्था का एक व्यक्ति सितार बजा रहा था और गा रहा थाः—–
मानौ आई घन-घन-अन्तर दामिनि।
घन दामिनि दामिनि घन अन्तर, सोभित हरि ब्रज भामिनि।…
इस संगीत की मधुर धारा के बीच ऊपर उठते हुए उस गीति साधक के महा-महिम व्यक्तित्व के आगे मेरा मन अपने आप श्रद्धान्वत हो गया। कृष काया, सौम्य मुख-मंडल, संगीत के आरोह-अवरोह के साथ प्रतिपल नये वर्णों को धारण करने वाली भावन मुद्रा, खल्वाट सिर और उस पर क्रीड़ा करती हुई चोटी, सितार के तारों के साथ यन्त्रवत खेलती हुई पतली किन्तु लम्बी-सी उंगलियाँ, उन उंगलियों से जाग्रत होती हुई विभिन्न राग-रागिनियों में मुखरित होती हुई कृष्ण लीला के विभिन्न रूपों की झलकियाः इस मोहक व्यक्तित्व को देखते ही मुझे प्रतीत हो गया कि यही सूरदास जी हैं। मैं उनकी चरण-धूलि लेकर और चुपचाप बैठ गया और उस मधुर संगती धारा का आनन्द लेने लगा।
सूरदास जी के उस स्वर्गीय संगीत का आनंद लेने के लिए मेरे बाद और भी कई सज्जन आए। उनमें से मैं कई को पहचान भी सका, जो सज्जन पुराने लाला लोगों जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व को लेकर चूड़ीदार पाजामा, लम्बी अचकन और गोल टोपी पहन कर आये थे, वे रत्नाकर जी थे। भारतेन्दु जी भी अपने मनभावन रसिकों जैसे व्यक्तित्व को लेकर छैल-छबीली वेश-भूषा में वहाँ उपस्थित थे। अन्य महानुभाव जिन्हे मैं देखते ही जान गया, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ तथा प्रसाद जी थे। ये सभी, तथा जो और लोग वहाँ आये, सूरदास जी की अपनी मन की भावना के अनुरूप, प्रणाम कर के अथवा चरण-धूलि लेकर बैठते गये। सूरदास जी भावमग्न होकर अपनी संगीत साधना में तत्पर रहे। कभी अपने इष्टदेव श्रीकृष्ण की बाल लीला, कभी यौवन क्रीड़ा से सम्बन्धित पदों के गायन में तल्लीन रहे। सहसा उन्होंने गाना बन्द कर दिया और अपनी बन्द आँखों से पथ की ओर देखने लगे। कुछ ही क्षणों में हमने देखा कि पाश्चात्य वेश-भूषा धारण किये हुए एक प्रौढ़ावस्था के सज्जन, जिनके गोलाकार चेहरे पर आँखों में चश्मा चढ़ा हुआ था और नासिका के नीचे तितली के आकार की छोटी-छोटी मूँछे थी, आये। जब वे बरामदे के नीचे ही थे, सूरदास जी ने हलके से हँसी के भाव को लेकर उनसे कहा- सुकुल जी, आप तो शायद रास्ता भूल कर यहाँ आ गये हैं। आपके बाबाजी, मेरा मतलब है, भाई तुलसी तो, इस वृन्दावन के ठीक सामने, वह जो पंचवटी है न, उसमें रहते हैं।
सूरदास जी के इस कथन को सुनकर हमें लगा जैसे यह नये सज्जन आचार्य रामचन्द्र शुक्ल हैं, और सूरदास जी अपने इस कटु आलोचक को अपने यहाँ देख कर उनकी चुटकी ले रहे हैं। शुक्ल जी सूरदास जी के इन परिहास भरे शब्दों को सुनकर, पहले तो कुछ गंभीर हुए, उनकी मुद्रा में भी कुछ कठोरता- सी आई, किन्तु फिर उन्होंने अपने को संयत कर के हँसते हुए कहा, नहीं महाराज, आज तो मैं आपके श्री चरणों में अपने हृदय की श्रद्धा अर्पित करने आया हूँ।
सूरदास– बात बनाना तो तुम्हें खूब आता है। मेरे प्रति और तुम्हारे मन में श्रद्धा की भावना। कुमुदनी तो चन्द्रमा के प्रकाश को ही लेकर उल्लसित हो सकती है, सूर्य के प्रकाश को धारण करके आनन्द मग्न होने के लिए तो कमल-सा विशाल हृदय चाहिए।
शुक्ल– आपने भी किस दृष्टि दरिद्र नाम-हीन आलोचक की बात उठा दी, जो यमक की झोंक में आपको सूर और तुलसीदास जी को शशि बना गया, भला आपके सौम्य, सुशील और कोमल-कान्त व्यक्तित्व में सूर्य-सा प्रखर ताप कहाँ है, और तुलसीदास जी ने भी तो सब कहीं चन्द्रमा की शीतल चाँदनी नहीं छिटकाई हैं।
सूरदास– किन्तु, फिर भी तो आपने उन्हें पूर्ण भावुक कहा है, और साथ में यह भी जोड़ दिया है कि हिन्दी के कवियों में सर्वांगपूर्ण भावुकता तो हमारे गोस्वामी जी में ही हैं।
शुक्ल– हाँ, मैं अपने इस कथन को स्वीकार करता हूँ। इसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए मुझे विस्तार में जाना होगा। (अन्य लोगों की ओर देखते हुए) आप लोग यदि अनुमति दें तो मैं अपनी बात कुछ विस्तृत रूप में, आदरणीय सूरदास जी, तथा आप सभी महानुभावों के आगे रखने का प्रयत्न करूँ।
रत्नाकर– हम लोग तो सूरदास जी के सरस काव्य-प्रवाह का सुरस लेने आये थे, किन्तु सूरदास जी ने स्वयं ही जब यह वाक्-द्वन्द छेड़ दिया है, तो कुछ समय तक बौद्धिक विलास ही सही। हम सभी इस वाक्-विलास का आनन्द ले रहे हैं, आप अपनी बात स्पष्ट कीजिए।
शुक्ल– मेरी धारणा है कि कवि की पूर्ण भावुकता इसमें है कि वह प्रत्येक मानव स्थिति में अपने को डालकर उसके अनुरूप भाव का अनुभव करे। गोस्वामी जी ने राम चरित्र को लेकर, उसमें मानव जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों का समावेश कर दिया है। यदि कहीं सौन्दर्य है तो प्रफुल्लता, शक्ति है तो प्रणति, शील है तो हर्ष-पुलक, गुण है तो आदर, पाप है तो घृणा, अत्याचार है तो क्रोध, अलौकिकता है तो विस्मय, पाखण्ड है तो घृणा, तुलसीदास जी के हृदय में बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव से वर्तमान है। इतनी सर्वांगपूर्ण भावुकता हमें हिन्दी के अन्य किसी कवि में दिखाई नहीं देती, इसीलिए मैंने कहा है कि मानव प्रकृति के जितने अधिक रूपों के साथ गोस्वामी जी के हृदय का रागात्मक सामंजस्य हम देखते हैं, उतना अधिक हिंदी भाषा के और किसी कवि के हृदय में नहीं।
सूरदास– भाई तुलसी की रचनाओं का सम्यक् अध्ययन करके तुमने यह तो देख लिया है कि उन्होंने रामचरित्र में सभी प्रकार की परिस्थितियों का समावेश कर दिया है। किन्तु मेरा विचार है कि यदि तुम हिन्दी भाषा के अन्य कवियों की रचनाओं का भली प्रकार अध्ययन करो तो, उनमें से कुछ में तो तुम्हें पूर्ण भावुकता देखने को मिल जायेगी।
शुक्ल– अच्छा चलिए, आपके इस दिशा-निर्देश को स्वीकार करके सब के पहले मैं हिन्दी के कृष्ण भक्त कवियों को लेता हूँ। हमारे यहाँ का भक्ति मार्ग भगवान् की अनन्त शक्ति, शील और सौन्दर्य के अधिष्ठान रूप में इसी जगत् के व्यवहार के बीच रखकर चला है। रामोपासक भक्त तो उक्त तीनों विभूतियों-शक्ति, शील और सौन्दर्य से समन्वित राम में अपने हृदय को लीन करते आये हैं। पर कृष्ण भक्त कवियों ने तो श्रीकृष्ण को केवल वात्सल्य और श्रृंगार के आलम्बन रूप में लिया है। यदि हम कृष्ण चरित्र को उसकी सम्पूर्णता के साथ लें तो हम कृष्ण को भी राम की भाँति लोक-कलंक, अत्याचारियों का पराभव कर, धर्म की शक्ति और सौन्दर्य का प्रकाश फैलाते हुए देखते हैं। महाभारत में जो दिव्य-शक्ति भारत के सब से प्रचंड और अत्याचारी सम्राट जरासंध को लोकमार्ग से हटाती है, अधर्म में रत कौरवों के पराजय द्वारा धर्म की विजय-घोषणा करती है, कृष्ण भक्त कवियों ने उस दिव्य-शक्ति के रूप में कृष्ण को अपने हृदय में प्रतिष्ठित नहीं किया है। श्रीमद्भागवत का आश्रय लेकर उन्होंने कुछ तो कृष्ण की बाल-लीला पर अधिकतर गोपियों के साथ उनकी प्रेम-लीला का ही वर्णन किया है। भगवान् के जो तीन रक्षक, पालक और रंजक रूप माने गये हैं, उनमें उन्होंने केवल रंजक रूप अपने लिये छाँट लिया है। आपने भी तो केवल, श्रीकृष्ण की बाल-लीला और यौवन-लीला का ही मनोयोग के साथ वर्णन किया है।
सूरदास– हाँ यह तो मैं स्वीकार करता हूँ कि श्रीकृष्ण की बाल-लीला और यौवन-क्रीडा का मैंने पूर्ण मनोयोग के साथ वर्णन किया है, किन्तु ऐसा नहीं है कि मैंने उनके लोक-रक्षक रूप को बिलकुल लिया ही न हो। इसलिए तुम्हारा यह आक्षेप कि मैंने लोक-पक्ष को छोड़ दिया है, उचित प्रतीत नहीं होता।
शुक्ल– क्षमा कीजियेगा, महाकवि, मुझे लगता है जैसे किसी ने मेरे विरुद्ध आपके कान बहुत अधिक भर दिये हैं। लोक-पक्ष की उपेक्षा की बात तो मैंने आपके सम्बन्ध में नहीं, सामान्यतः कृष्ण भक्त कवियों के लिए कही है। आपके सम्बन्ध में तो मेरा स्पष्ट कथन है कि बाल-लीला के वर्णन में कृष्ण चरित्र के लोक-पक्ष को आपने स्थान दिया है, कंस के भेजे हुए असुरों के उत्पात से गोपों को बचाना, काली नाग को नाथ कर लोगों का भय छुड़ाना, इन्द्र के कोप से डूबते हुए गोकुल की रक्षा करना आदि, इसी प्रकार के प्रसंग है। किंतु यह तो आप भी स्वीकार करेंगे कि इन प्रसंगों के वर्णन में आपकी वृत्ति लीन नहीं हुई है। जिस उत्साह से तुलसीदास जी ने मारीच, ताड़का, खर-दूषण आदि के निपात का वर्णन किया है, उस ओज और उत्साह से आपने श्रीकृष्ण द्वारा बकासुर, अघासुर, कंस आदि का वध नहीं दिखाया है। मेरी तो यह भी धारणा है कि कंस और उसके साथी असुरों को आपने लोक शत्रु या लोकपीड़क के रूप में नहीं, श्रीकृष्ण के अपने शत्रु के रूप में चित्रित किया है।
सूरदास– बस यहीं मुझे आपत्ति है। मैं यह तो स्वीकार करता हूँ कि श्रीकृष्ण के इस लोक-संग्रही रूप में मेरा मन विशेष रूप से नहीं रमा है, और न मैं भाई तुलसीदास की भाँति इन लोक-रक्षा के कार्यों का पूर्ण ओज और उत्साह के साथ वर्णन ही कर पाया हूँ। किन्तु कंस और उसके साथी असुर काली नाग, इन्द्र आदि, हैं लोक शत्रु ही। मैंने उन्हें श्रीकृष्ण का अपना शत्रु उसी रूप में बना दिया है जिस प्रकार आपके परम प्रिय कवि तुलसीदास जी ने सीता-हरण करा कर लोक-पीड़क रावण को राम का निजी शत्रु भी बना दिया है।
आचार्य शुक्ल इसका कुछ उत्तर देते कि रत्नाकर जी बीच में बोल पड़े- सूरदास की यह आपत्ति तो आपको स्वीकार ही करनी पड़ेगी। उनके कंस, अधासुर आदि वास्तव में रावण की भाँति लोक-पीड़क हैं, हाँ, यह मैं मान सकता हूँ कि वे रावण जैसे प्रचंड नहीं है।
शुक्ल– अच्छा चलो मैं यह मान लेता हूँ कि कंस और उसके साथी असुर लोक-पीड़क हैं, फिर भी मेरा यह कहना है कि सूरदास जी ने लोक-पक्ष को समुचित रूप से ग्रहण नहीं किया है। उन्होंने भक्ति को लोक-मर्यादा से अधिक प्रतिष्ठा दी है। तभी तो कृष्ण के प्रति अनुरक्त होकर गोपियाँ लोक-लाज, कुलकानि, वैदिक अनुशासन सब को भंग कर के, कृष्ण के आवाहन पर तुंरत घरों से निकल पड़ती है। उसके बाद गीत, नृत्य और उन्मुक्त विलास-क्रीड़ा प्रारम्भ हो जाती है। मैं यह मानता हूँ कि कृष्ण और गोपियों की इस आनन्द-क्रीड़ा में एक महद् आध्यात्मिक रहस्य निहित है। किन्तु सामान्य जनता तो इस रंग-रहस्य में मर्यादा के अतिक्रमण, शील और सदाचार के उल्लंघन, उन्मुक्त विलास-क्रीड़ा के प्रोत्साहन के भाव को ही ग्रहण करेगी।
सूरदास– तुम्हारी यह आपत्ति मुझे भली प्रकार समझ में आ गई। किन्तु सामान्य जनता को दृष्टि में रख कर तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं था। मैंने तो श्रीनाथ जी के मन्दिर में भजन-कीर्तन में भाग लेने वाले एक विशेष मानसिक स्तर के भक्तों के लिए अपने पदों की रचना की थी। कृष्ण और गोपियों की आनन्द-क्रीड़ा में जो आध्यात्मिक रहस्य अन्तर्निहित है, उसे तो महाप्रभु, जो सौभाग्य से आज यहाँ उपस्थित हैं अधिक स्पष्ट कर सकेंगे।
शुक्ल जी तत्काल बोल पड़े- इस सम्बन्ध में महाप्रभु बल्लाभाचार्य जी को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। मैं स्वयं इस रहस्य से भली प्रकार परिचित हूँ। कृष्ण भक्ति सम्प्रदायों में कृष्ण और गोपियों के इस सम्मिलन को मुक्त आत्माओं के साथ परमात्मा की आनन्द-क्रीड़ा समझा जाता है। एक ओर पौराणिक व्याख्या है, श्रुतियों की प्रार्थना पर श्रीकृष्ण ने नित्य-वृन्दावन का निर्माण करके गोपियों के रूप में उनके साथ आनन्द-क्रीड़ा समझा जाता है। एक ओर पौराणिक व्याख्या है, श्रुतियों की प्रार्थना पर श्रीकृष्ण ने नित्य-वृन्दावन का निर्माण करके गोपियों के रूप में उनके साथ आनन्द-क्रीड़ा द्वारा उन्हें अपने समागम का दिव्य-आनन्द प्रदान किया था। कृष्ण भक्त-सम्प्रदायों में गोपियों को आदर्श समझा जाता है, और विविध मानसिक प्रयासों द्वारा अपने मन में उन्हीं जैसी भावना जगा कर नित्य-वृन्दावन में उस परब्रह्म सच्चिदानन्द के साथ सम्मिलन सुख की कामना की जाती है। किन्तु श्रीकृष्ण की प्रणय-क्रीड़ा के इस आध्यात्मिक रहस्य को बौद्धिक विकास के एक विशेष स्तर पर पहुँचे हुए लोग ही समझ सकते हैं। सामान्य जनता तो कृष्ण प्रेम-क्रीड़ा में लौकिक श्रृंगार का रंग-रहस्य ही ग्रहण कर पाती है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि आपने लोकपक्ष का समुचित निर्वाह नहीं किया है।
सूरदास– तुम्हारी इस तर्क-परम्परा के उत्तर में मुझे फिर वही दुहराना पड़ेगा जो मैं अभी कह आया हूँ। मैंने जनता को दृष्टि में रख कर लिखा ही नहीं है। जनता के कवि तो तुम्हारे बाबा जी है, मैं तो भक्तो का कवि हूँ। महाप्रभु जी, आप मेरे इस कथन को कुछ स्पष्ट कीजिए न।
बल्लभाचार्य– हाँ मैं स्वयं भी तुम्हारी बात कुछ और स्पष्ट करने को सोच रहा था। आचार्य शुक्ल, हमारे साहित्य में मानवीय चेतना के पाँच-स्तर माने गए हैं। अन्न, प्राण, मन, बुद्धि और अन्तरात्मा। भक्त या साधक जब अपनी प्रवृत्तियों को अर्न्तमुखी कर के अन्तरात्मा के स्तर पर पहुँचाता है, तभी उसे सच्चिदानन्द स्वरूप की अनुभूति होती है। आपके प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास तो अन्न के स्तर से प्रारम्भ कर के बुद्धि के स्तर तक ही पहुँच पाये। इसीलिए लोक-मर्यादा पर उनकी दृष्टि-बँध सी गयी। भक्त होकर भी भक्ति के उल्लास और परमानन्द को वे अनुभव नहीं कर पाये। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखा जाय तो नित्य-वृन्दावन के दिव्य-जीवन के आनन्द और उल्लास का वर्णन करने वाला सूर-सागर तुलसी के लोक-जीवन की मर्यादाओं में पूर्णतः आबद्ध काव्य-ग्रंथ राम-चरितमानस से कहीं अधिक श्रेष्ठ है।
शुक्ल– आचार्य महोदय, आप अपनी आध्यात्मिक जीवन-दृष्टि तो लेकर यह कह सकते हैं, किन्तु मुझे तो आध्यात्मिक को इतना अधिक महत्व देना कि लोक-जीवन पूर्णतः उपेक्षित रह जाय, समीचीन नहीं प्रतीत होता। मुझे तो यह धरती प्यारी है। इसमें खिलने वाले फूलों से प्यार है। इन पर मँडराती हुई तितलियाँ और मधु-संचय में तत्पर भौंरे मुझे भले प्रतीत होते हैं। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों से मुझे स्नेह हैं। यह नील गगन मुझे प्यारा लगता है। इनमें से सबसे अधिक आकर्षण मेरे मन में, मानव के प्रति हैं। मैं समझता हूँ उसी के सुख सन्तोष के लिए सृष्टि का यह अनन्त विधान है। मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है-
बड़े भाग मानुस तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मनुष्य की इसी क्षेष्ठता को दृष्टि में रखकर इस जगत् की प्रत्येक गति को मैं मानव सापेक्ष्य मानता हूँ।
सूरदास जी को शुक्ल जी के इस भावुकता पूर्ण कथन को सुन कर हँसी आ गयी और उन्होंने हल्के से परिहास की भावना को लेकर कहा-
किन्तु हे मानवोपासक! इस समय तुम धरती पर नहीं स्वर्ग में हो, वृन्दावन में हो, और मानवों के बीच नहीं दिव्य विभूतियों के बीच समुपस्थित हो।
शुक्ल– दिव्य सौन्दर्य और अलौकिक-उल्लास के गायक महाकवि, यह मैं भली प्रकार जानता हूँ, किन्तु इस स्वर्ग का मुझे वही प्यारा है जो कुछ धऱती से मिलता जुलता है। यहाँ जब मैं देखता हूँ कि किसी को कष्ट में देखकर कोई भी करुणा से गद्गद् नहीं होता, किसी को वर्षों बाद अपने बीच पाकर स्नेह विह्वल होकर उसे अपनी बाँहों में भर लेने को नहीं उठता, किसी को अत्यधिक प्रसन्नता को देखकर भी आनन्दमग्न होकर नृत्य नहीं कर उठता, तो मुझे अपना धऱती का जीवन ज़ोर से अपनी ओर खींचने लगता है। इस स्वर्ग का एकरस, एक-भाव जीवन, मुझे किसी प्रकार भी रुचिकर नहीं। यह तो कर्मों का विपाक है जो मुझे यहाँ आना पड़ा और रुकना पड़ रहा है। कभी-कभी मनुष्य की भलमनसाहत उसके लिए दण्ड स्वरूप हो जाती है।
शुक्ल जी का यह कथन समाप्त होते होते गुरुदेव रवीन्द्रनाथ बोल पड़े- आलोचक प्रवर, देवताओं की इस पुण्य भूमि में धरती के मानव की श्रेष्ठता के उद्घोषण के रूप में, मैं तुम्हारा अभिनन्दन करता हूँ। अपनी स्वर्ग से विदा शीर्षक रचना में, मैंने भी इसी प्रकार के भाव को व्यक्त किया है। मनुष्य को श्रेष्ठता का तो मैं भी प्रतिपादन करता हूँ। हमारे सोने के बंगाल के एक कृष्ण भक्ति कवि, चंडीदास ने भी इसी प्रकार के भाव को व्यक्त किया है—–
सवार ऊपर मानव सत्त, तहार ऊपर नाई।
मेरे समस्त साहित्य में मनुष्य की इसी श्रेष्ठता की घोषणा है।
प्रसाद– मानव की श्रेष्ठता का समर्थन तो मैं भी करूँगा, और मेरे पास बैठे हुए ये कालिदास, भारतेन्दु आदि भी इसी मत के हैं।
शुक्ल– मुझे प्रसन्नता हैं कि यहाँ उपस्थित कुछ दिव्य-विभूतियों ने भी मनुष्य की श्रेष्ठता के मेरे मत का समर्थन किया है। अभी प्रसाद जी मेरे समर्थन में बोले थे इन्हीं की धारा के एक कवि सुमित्रानन्दन पंत ने मानवीय श्रेष्ठता की घोषणा बड़ी भावात्मक शब्दावली में की है संयोग से वे भी यहाँ हैं। उनसे आग्रह है…….
पन्त- मेरी वे पंक्तियाँ हैं—–
सुन्दर हैं विहग सुमन सुन्दर,
मानव तुम सबसे सुन्दरतम्।
रंजित जग की तिल सुषमा से,
इस निखिल विश्व में चिर निरुपम।।
शुक्ल– इसी जीवन-दृष्टि को लेकर काव्य का मनव-सापेक्ष्य होना मैं उसकी सब से बड़ी कसौटी मानता हूँ।
सूरदास– लेकिन भाई यह सब तो विषयान्तर हैं। मैं तो उन आपत्तियों की चर्चा कर रहा था, जो तुमने मेरे सम्बन्ध में उठाई हैं। तुमने लिखा है- कि लोक-संघर्ष से उत्पन्न विविध व्यापारों की योजना मेरी रचनाओं में नहीं है, और जीवन की गम्भीर समस्याओं से इसी तटस्थता के कारण, उनमें वह वस्तु गाम्भीर्य नहीं है जो तुलसीदास जी की रचनाओं में है।
शुक्ल– हाँ, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मुझे आपकी रचनाओं में जीवन की गम्भीर समस्याओं से अलग रखने की वृत्ति देखने को मिलती है, और मैं यह जानना चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है।
सूरदास– सब से पहले तो मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि लोक-संघर्ष में उठने वाली समस्याओं का चित्रण मेरी रचनाओं का उद्देश्य नहीं है। मैंने इन क्षणिक समस्याओं को न लेकर उसके आगे खड़ी चिरन्तन समस्या को जीवन के सच्चे सुख, वास्तविक आनन्द की उपलब्धि किस प्रकार सम्भव है- उठाया है। इस सम्बन्ध में मैंने केवल यही नहीं बताया है कि उसका साधन क्या है, वरन् उस दिव्य जीवन की मनोहर दृश्यावली भी उपस्थित की है।
शुक्ल– आपके इस उत्तर से तो मेरी आपके विषय में धारणा और पुष्ट हो गयी। आप लोक-जीवन के दुख-द्वन्द्व, झगड़े-टन्टे, युद्ध-विप्लव से घबरा कर यहाँ स्वर्ग में नित्य-वृन्दावन में आ गये हैं। आपके इस पथ का अवलम्बन कर लेने से तो केवल आपके बौद्धिक और मानसिक स्तर तक पहुँचे हुए लोगों को ही लाभ हो सकता है, और फिर स्वर्ग में स्थान भी तो थोड़ा ही है। मैं तो मनुष्य में ही देवत्व सदभावना, सद् विचार और सदाचार- की प्रतिष्ठा करके अपनी धरती को ही स्वर्ग बनाने की कामना करता हूँ।
सूरदास जी हँसते हुए इस विश्वास के साथ जैसे यह कभी नहीं होने का, कहते हैं—- अच्छा भाई, जब तुम धरती को स्वर्ग बना लोगे तो हम लोग वहीं आ कर रहने लगेंगे। किन्तु अभी मेरी तुमसे जो शिकायतें हैं उनका उत्तर दिये जाओ।
शुक्ल– आपके मन में न जाने कैसे यह धारणा बद्धमूल हो गई है कि मैंने आपके विषय में केवल आपत्तियाँ ही उठाई हैं। मैंने तो स्पष्ट लिखा है कि सूर-सागर वास्तव में एक महासागर है- जिसमें हर प्रकार का जल आकर मिला है। जिस प्रकार उसमें मधुर अमृत है- उसी प्रकार कुछ खारा, फीका और साधारण जल भी है। मेरा प्रयास खारे, फीके और साधारण जल में हंस जैसी वृत्ति को लेकर, अमृत को अलग करने का रहा है। इसी दृष्टि को लेकर जहाँ मैंने आपके सागर के मूँगे, सीपी और घोंघों की ओर संकेत किया है, वहाँ उसके मोतियों की अपार राशि भी, उनकी दिव्य कीर्ति को और निखार कर, जनसाधारण की दृष्टि के आगे उपस्थित कर दी है।
सूरदास– इस समय तो मैं अपने सागर के कुछ मूँगे, सीपी और घोंघें और देखना चाहूँगा।
शुक्ल– आपके विरह-वर्णन के सम्बन्ध में भी मुझे आपत्ति रही हैं। परिस्थिति की गम्भीरता के अभाव में गोपियों के वियोग में वह गम्भीरता नहीं दिखाई पड़ती जो सीता के वियोग में है। सीता का अपहरण हुआ था और अपने प्रिय से इस प्रकार बल-पूर्वक अलग किये जाने पर, उन्हें कई सौ कोस दूर, दूसरे द्वीप के राक्षसों के बीच रहना पड़ा था। गोपियों के गोपाल केवल दो चार कोस दूर एक नगर में राज-सुख भोग रहे थे। गोपियाँ यदि चाहती तो वहाँ पहुँच भी सकती थी। इसीलिए आपका वियोग-वर्णन परिस्थिति के अनुरोध से नहीं, वरन् वियोग वर्णन के लिए ही लिखित प्रतीत होता है। गोपियों का वियोग तो बैठे-ठाले का काम है- और इसीलिए वह मुझे असंगत भी लगा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता के जिस वियोग का वर्णन किया है, वह राम को निर्जन वनों और पहाड़ों में घुमाने वाला, सेना एकत्र कारने वाला, पृथ्वी का भार उतरवाने वाला वियोग है। इस वियोग की गम्भीरता के सामने आपका वियोग-दर्शन अतिशयोक्ति पूर्ण होने पर भी बाल-क्रीड़ा सा प्रतीत होता है।
सूरदास– हाँ, मैने तुम्हारी इस आलोचना के सम्बन्ध में भी सुना है। किन्तु मुझे आश्चर्य यह देख कर होता है कि तुम्हारा जैसा सुखी आलोचक, लौकिक विरह और आध्यात्मिक-वियोग के अन्तर को नहीं समझ सका। भाई तुलसी ने लोक-संघर्ष का प्रसंग लिया है, इसीलिए उनके राम, सीता के वियोग में थोड़ा बहुत रो-धोकर उनके उद्धार के लिए तत्पर हो जाते हैं। रावण के यहाँ से सीता का उद्धार आवश्यक है, इसीलिए राम उस दिशा में अग्रसर होते हैं। गोपियाँ नारी सुलभ स्वाभिमान को लेकर श्रीकृष्ण को लौटाने नहीं जातीं। फिर कृष्ण तो मथुरा में बन्दी नहीं थे, जो गोपियाँ उनकी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील होती। भाई तुलसी ने तो सीता की वियोग व्यथा का वर्णन नहीं किया है, यदि किया होता तो वह बहुत कुछ वैसा ही होता जैसे जायसी भाई की नागमती तथा मेरी गोपियों का है। यदि नारी मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो मेरे वियोग-वर्णन में पूरी तरह से वास्तविकता देखने को मिलेगी। किन्तु इस यथार्थता के होते हुए भी मेरे वियोग-वर्णन का वास्तविक उद्देश्य तो उस परब्रह्म से वियुक्त विरहिणी आत्माओं की मनोव्यथा का उद्घाटन है।
शुक्ल– किन्तु महाकवि, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं आध्यात्मिकता को लौकिकता से अधिक महत्व नहीं देता। इसीलिए मैंने लोकदृष्टि से ही आपके वियोग वर्णन को परखना चाहा है। मुझे आशा है, आप भी यह स्वीकार करेंगे कि प्रिय से विमुक्त होकर गोपियों की भाँति निरन्तर रोने-धोने और निश्चेष्ट होकर बैठ रहने से, राम की भाँति थोड़ा-बहुत रो-धोकर अपने कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो जाना, कहीं अधिक श्रेयस्कर है।
सूरदास– लेकिन भाई वियोग-व्यथा में चेष्ठा तो राम में ही है, और पुरुष होने के कारण उनके लिए यही उचित भी है। भाई तुवलसी ने सीता की वियोग व्यथा के वर्णन को विशेष महत्व नहीं दिया है। यदि दिया होता तो मेरा निश्चित विश्वास है कि वह बहुत कुछ वैसा ही होता, जैसा मेरी गोपियों का है। खैर, छोड़े इस प्रसंग को। मुझे सब से अधिक दुख तो यह सुन कर हुआ है कि तुमने मुझे साम्प्रदायिकता की भावना में आविष्ट कहा है।
रत्नाकर– हाँ इस सम्बन्ध में तो मुझे भी शिकायत है। साम्प्रदायिकता का आरोप तो सूरदास जी से अधिक तुम्हारे तुलसीदास जी पर लगाया जा सकता है। उनके मन में तो केवल राम के प्रति ही श्रद्धा का भाव था। तभी तो उन्होंने कहा है—–
जाके प्रिय न राम वैदेही।
तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही।।
इतना ही नहीं, उन्होंने तो केवल उस माता को ही पुत्रवती माना है-जिसका पुत्र राम भक्त हो।
पुत्रवती युवती जग सोई, राम भगत जाकर सुत होई।
इसके अतिरिक्त हम उनकी रचनाओं में ब्राह्मणों के प्रति विशेष पक्षपात भी देखते है-
कवच अभेद विप्रपद पूजा। यहि सम विजय उपाय न दूजा।।
एक स्थल पर तो उन्होंने यह भी कह दिया है—-
पूजिय विप्र शील गुन हीना। शूद्र न गुन गन ज्ञान प्रवीना।। सूरदास जी की रचनाओं में इतनी संकुचित जीवन-दृष्टि कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी।
सूरदास– प्रिय रत्नाकर, भाई तुलसी ने यद्यपि यह सब कहा है, फिर भी इन्होंने उनकी मुक्त-कंठ से प्रशंसा की है। उनके प्रति अत्यधिक प्रेम होने के कारण उनके दोषों को, बड़ी-बड़ी भूलों को भी ये छिपा गये हैं, और उनसे तुलना करते हुए मेरी भूलों की इन्होंने तिल का ताड़ बना दिया है। इसीलिए इनसे मैं अत्यधिक क्षुब्ध हूँ। (इतना कहते-कहते उनका कंठ भर आता है, किन्तु वे कहते रहते हैं) मैं यह मानता हूँ कि मैंने भगवान् को केवल कृष्ण रूप में ही देखा है, किन्तु यह इसलिए हैं क्योंकि मेरा व्यक्तित्व महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण करने के अनन्तर, श्रीनाथ जी के मन्दिर में ही समाविष्ट हो गया था। श्रीनाथ जी के भजन-कीर्तन में ही मेरा शेष जीवन व्यतीत हुआ। फिर भी मैने भगवान् के अन्य रूपों के उपासकों को कभी बुरा-भला नहीं कहा है। न जाने क्यों ये तब भी मुझे साम्प्रदायिकता की भावना से ग्रस्त कहते हैं। (इन शब्दों के साथ उनका कंठ और भी भर आता है)।
शुक्ल– (परम विनम्रता के साथ) मुझे वास्तव में बहुत दुःख है कि मेरी आलोचना से आपको इतना अधिक क्षोभ हुआ है। मैं इसके लिए सम्पूर्ण मन से क्षमा-याचना करता हूँ।
सूरदाज जी (गद्गद् होकर)- नहीं, इतना अधिक विन्रम होने और क्षमा माँगने की आवश्यकता नहीं। आलोचक के उत्तरदायित्व की गहनता को मैं समझता हूँ, और मुझे यह भी ज्ञात है कि जहाँ तुमने मेरे दोषों की ओर संकेत किया है- वहाँ मुझमें जो थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ हैं, उनकी मुक्त-हृदय से सराहना भी की है। कुछ स्थल ऐसे भी हैं, जहाँ तुमने मुझे अपने प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास से श्रेष्ठ कहा है। मेरी धारणा है कि मेरी त्रुटियों की ओर तुम्हारी दृष्टि से अलग करके देखा है। मेरी भाषा आदि में जो त्रुटियाँ देखने को मिलती हैं, उनके सम्बन्ध में तुमने स्वयं स्वीकार किया है कि अन्धे होने के कारण काटने, छाटने और हरताल लगाने का कार्य मेरे लिए सम्भव नहीं हो सका।
शुक्ल– आपके इन शब्दों के साथ हमारा यह वाद-प्रतिवाद एक प्रकार से समाप्त हो जाता है। मैं आपसे तथा सभी उपस्थित सज्जनों से क्षमाप्रार्थी हूँ, जो मेरे कारण आज के कार्यक्रम में व्याघात पड़ गया है। मैं भी आज शरदपूनों के दिन, आपसे तर्क-वितर्क के लिए के नहीं, वरन् इस नित्य-वृन्दावन में कृष्ण-लीला के विभिन्न रूपों की झाँकी देखने, आपके संगीत का आनन्द लेने एवं सम्पूर्ण मन से आपके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने आया था। बाल-जीवन की दिव्य शोभा और यौवन के अनन्त उल्लास के गायक महाकवि! तुम्हारी काव्य प्रतिभा अप्रतिम है। तुम वास्तव में दिव्य-दृष्टि सम्पन्न थे, तभी तो वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन तुमने अपनी बन्द आँखों से किया उतना और किसी कवि ने नहीं। तुम्हारे बाल-लीला के चित्रण को देखकर लगता है, जैसे बालकों जैसी सरल प्रकृति तुम्हें स्वयं मिली थी। तभी तो तुम बाल-जीवन के बाहरी रूपों और चेष्टाओं का ही नहीं, बालकों की अन्तःप्रकृति का भी सूक्ष्म और विस्तृत वर्णन कर सके। यौवन के मनोविज्ञान का भी तुमसे अधिक ज्ञान रखने वाला अब तक तो दूसरा हुआ नहीं। तुम्हारा श्रृंगार वर्णन, प्रेम संगीतमय जीवन की एक गहरी चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करने वालों को माधुर्य के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। प्रेम के रंग-रहस्य को लेकर नारी हृदय की अपार-भाव राशि का जितना अधिक उद्घाटन तुमने किया है, उतना अन्य किसी ने नहीं। श्रृंगार रस का रसराजत्व यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया है तो तुम्हीं ने। काव्य के हृदय पक्ष की इस श्रेष्ठता के साथ, कलापक्ष का सम्पूर्ण सौष्ठव भी तुम्हारी रचनाओं में दर्शनीय है। तभी तो हमारी धारणा है कि तुममें जितनी सहृदयता और भावुकता है, उतनी ही चतुरता और वाग्विदग्धता भी। किसी बात को कहने के न जाने कितने टेढ़े सीधे ढंग…….सूरदास जी गद्गद् होकर बड़ी विन्रमता के साथ-बस इतना ही । एक सामान्य ठीकरे को हिमालय की गरिमा प्रदान करने का प्रयास न करो और फिर मैंने सुना है आज के किसी विचारक का कहना है कि सौन्दर्य किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में नहीं, देखने वाले की आँखों में उसकी दृष्टि में होता है। लो तुम्हारे प्रिय कवि……….
सूरदास जी के इस कथन के समाप्त होते-होते उन्हीं की अवस्था के एक सज्जन, शरीर से स्वस्थ, कान्तिमय मुखमंडल, रामनामी दुपट्टा ओढ़े हँसते हुए आये और इससे पहले कि कोई उनसे कुछ कहे वे स्वयं ही बोल पड़े-भाई सूर, क्षमा करना, मुझे आने में कुछ देर हो गयी। कुछ सज्जन आ गये थे, उन्होंने बड़ी विचित्र बातें सुनायी। हमारे देश में सात समुद्र पार से जो प्रचारक आये हैं, उनमें से कुछ यह प्रचार कर रहे हैं कि श्री राम के समय में ही उनके धर्ममठ, गिरजाघर, हमारे यहाँ बन गये थे, और इसके प्रमाणस्वरूप मेरे मानस की यह पंक्ति उद्धृत करते हैं—–
सर समीप गिरिजा-घर सोहा, वरनि न जाय देखि मन मोहा। इसी प्रकार एक अन्य सज्जन का कहना है कि मैं कुछ दिनों मस्जिद में भी रहा था, शायद मुसलमान भी हो गया होऊँ- तभी तो मैने लिखा है—
मांगि के खैबो, मसीत को सोइबो,
लेबे को एक न देबे को दोऊ।
तुलसीदास जी के इन शब्दों को सुन कर सभी लोग हँस पड़े और वातावरण की गम्भीरता पूर्णतः छट गयी। भारतेन्दु जी ने तब सूरदास जी से अपना कोई ललित पद सुनाने की प्रार्थना की। सूरदास जी ने सितार सँभालते हुए कहा- अब तो नन्द लला के जगावन की बेला भई- और फिर तार सँभाल कर गाने लगे—-
जागिए गुपाल लाल ग्वाल द्वार ठारे।
रैनि अंधकार गयो, चन्द्रमा मलीन भयो।
तारागन देखियत नहिं, तरनि किरनि बाढ़े।।
मुझे लगने लगा जैसे कोई मुझे ही जगा रहा हो। आँखें खोली तो देखा विद्या और जितेन्द्र सींकचों के बाहर खड़े हैं। मैंने उठ कर दरवाजा खोला। जितेन्द्र ने पूछा- आप कोई मधुर स्वप्न देख रहे थे, क्या? आपके मुख की मुद्रा बड़ी भावन थी। मैं शीघ्र ही तैयार होकर उनके साथ घूमने चल दिया और रास्ते में मैंने उन्हें………..।
-डॉ. विश्वनाथ मिश्र
Note – यह लेख ‘सम्मेलन पत्रिका’ में सन् 1970 में छपा था . अपने सुधी पाठकों के लिए हम यह लेख ज्यों का ज्यों प्रस्तुत कर रहे हैं.
Guest Authors
- Aatif Kazmi
- Absar Balkhi
- Afzal Muhammad Farooqui Safvi
- Ahmad Raza Ashrafi
- Ahmer Raza
- Akhlaque Ahan
- Arun Prakash Ray
- Balram Shukla
- Dr. Kabeeruddin Khan Warsi
- Dr. Shamim Munemi
- Faiz Ali Shah
- Farhat Ehsas
- Iltefat Amjadi
- Jabir Khan Warsi
- Junaid Ahmad Noor
- Kaleem Athar
- Khursheed Alam
- Mazhar Farid
- Meher Murshed
- Mustaquim Pervez
- Qurban Ali
- Raiyan Abulolai
- Rekha Pande
- Saabir Raza Rahbar Misbahi
- Shamim Tariq
- Sharid Ansari
- Shashi Tandon
- Sufinama Archive
- Syed Ali Nadeem Rezavi
- Syed Moin Alvi
- Syed Rizwanullah Wahidi
- Syed Shah Tariq Enayatullah Firdausi
- Umair Husami
- Yusuf Shahab
- Zafarullah Ansari
- Zunnoorain Alavi