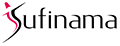Sufiyon ka Bhakti Raag ( सूफ़ियों का भक्ति राग )
तसव्वुफ मुसलमानों के नज़दीक मज़हब के आंतरिक पक्ष का नाम है। इससे तात्पर्य वह तपस्या और संयम है जो दिल के पर्दे हटाये और सत्य का रहस्योद्घाटन करे।
तसव्वुफ के उद्भव एवं विकास के दो युग बताये जाते है। पहला युग इस्लाम के आरम्भ से नवीं सदी ईस्वी के शुरु तक और दूसरा नवी सदी के बाहरवीं सदी तक। पहले दौर में तसव्वुफ कोई अलग मार्ग नहीं था बल्कि अपनी आस्था के प्रति दृढ़ मुसलमानों में से वह लोग जो तपस्या औऱ इबादत औऱ परहेज़गारी व सदाचार में शरीयत की पाबंदी का दृढ़ता से पालन करते थे, सूफी कहलाते थे। धीरे-धीरे कुछ नये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभावों के कारण और कुछ बाह्य प्रभावों से मुसलमानों में एक ऐसा गिरोह पैदा हुआ जो कुरआन के गुप्त अर्थों पर ज़ोर देते हुए उसकी व्याख्या नये ढंग से करने लगा। ये लोग एक तरफ शरई पाबन्दियों के और दूसरी ओर बौद्धिक तर्कों के खिलाफ थे और मज़हब का सरचश्मा कल्ब व रुह (हृदय व आत्मा) को बताते थे। उनके प्रभाव से पहले दौर का सीधा साधा कुफ्र व फाक़ा का नज़रिया कम समय में पूर्ण रूप से वहदते वजूदी (ऐकश्वरवादी) सम्प्रदाय बन गये। और अन्तःकरण के ये रुझान खुद की माकिराइयत तसव्वुर से मिलकर बहुत जल्द सारे आलमे इस्लाम में फैल गयी। इस्लाम की इस बुनियादी खुसूसियत को तसव्वुफ कहा जाता है।
वेदांत में जो स्थान शंकाराचार्य को प्राप्त है इस्लामी फलसफे में वही स्थान इमाम ग़जाली को प्राप्त है। ग़ज़ाली का कारनामा तसव्वुफ के सिद्धांत को नये सिरे से परिभाषित करना है। धीरे-धीरे सूफियाना दृष्टिकोण विद्वानों के चिंतन से गुज़र कर शायरों के विचारों पर छा गये। उनके कलाम में रच गये और शेर के जादू से जनसाधारण की ज़बान पर चढ़ गये। अरबी ज़बान के ऐसे शायरों में उमर बिन अलफरीद (मृ. 1235) और फ़ारसी के शायरों में अबू सईद इब्न अबिलख़ैर (मृ. 1048), हकीम सनाई (मृ. 1150), फरीदुद्दीन अत्तार (मृ. 1229/30), जलालुद्दीन रूमी (मृ. 1273), सादी (मृ. 1291), हाफिज़ (मृ. 1389), निज़ामी (मृ. 1199), जामी (मृ. 1492), ओहदी (मृ. 1337) और इराकी (मृ. 1289) विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हिन्दुस्तान में तो तसव्वुफ जैसे शायरी का पर्याय बन गया। हिन्दुस्तान के शायरों में अमीर खुसरो (मृ. 1325), उरफी शीराजी (मृ. 1591), फैज़ी (मृ. 1595), नज़ीरी (मृ. 1612), तालिब (मृ. 1626), कलीम (मृ. 1650), दारा शिकोह (मृ., 1659), सरमद शहीद (मृ. 1659), चन्द्रभान ब्रह्मण (मृ. 1662), बेदिल (1721), आनन्द राम मुख़लिस (1750) सब के सब तसव्वुफ़ में रचे बसे थे। बाद में उर्दू के शायरों ने भी इस परम्परा को जारी रखा।
तसव्वुफ के इतिहासकारों ने तसव्वुफ़ के बाह्य तत्वों को स्वीकार करते हुए कहा है कि यह हिन्दु धार्मिक दर्शन, वेदांत, बौद्ध विचारों या उनसे मिलते जुलते विचारों का निचोड़ है। तसव्वुफ और वेदांत की समानता के बारे में सबसे पहला संकेत विलियम जाँस ने दारा शिकोह के कथनों के आलोक में किया। जाँस का विचार था कि वेदांत के सिद्धांत इस्लाम में पूर्व के युगों में यूनान स्कन्दरिया पहुंच कर मध्ययुगीन ईसाइयत में विलीन हो चुके थे। तसव्वुफ के बाह्य तत्वों के इस सिद्धांत को पॉमर, जॉन पी ब्राउन, दोज़ी, फॉन क्रीमर, गोल्ड ज़हर, रिचर्ड हार्टमन और मैक्सने भी की है।
फॉन क्रीमर के शोध का निचोड़ ये है कि आठवीं सदी ईस्वी में इस्लामी देशों में ईरानियों का साम्राज्य सबसे अधिक था और ईरानी चूंकि भारतीय सिद्धांतों से प्रभावित थे, इसलिए इस्लामी तसव्वुफ पर भी सबसे अधिक प्रभावशाली होने का अवसर भारतीय दृष्टिकोण को ही मिला।
हार्टमन तसव्वुफ के हिन्दुस्तानी उद्गम से बहस करते हुए ऐतिहासिक प्रमाण के साथ कहता है कि तसव्वुफ का आरम्भ खुरासान से हुआ। तसव्वुफ की बुजुर्गतरीन शख्सियतें जैसे इब्राहीम बिन अद्धम, शफ़ीक़ बल्ख़ी, ज़लनैन मिसरी, बायज़ीद बिस्तानी, यहिया बिन मआज़ राज़ी खुरासां और आस पास के इलाकों से ताल्लुक रखती थीं जिनके सांस्कृतिक परिवेश में भारतीय दर्शन सक्रिय थे। तुर्किस्तान के इस्लामी शहर में दाखिल होने के बाद हिन्दी और बौद्धी अनुयायियों को इस्लामी तसव्वुफ़ पर प्रभावी होने का और ज्यादा मौक़ा मिला। इन संदर्भ में डॉ. ताराचंद ने अपनी पुस्तक ‘हिन्दुस्तानी कल्चर पर इस्लाम का असर’ में तर्कपूर्ण बहस की है। वे भारतीय धार्मिक दृष्टिकोण और तसव्वुफ में जो गहरा रिश्ता है वह उनके विचार से बाकी तमाम रिश्तों से ज्यादा अहम है। उनका कहना है कि हिन्दुस्तान और फारस की खाड़ियों के मध्य व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से रहा है। उस समय व्यापार के साथ साथ विचारों का आदान-प्रदान भी होता था।
सच तो ये है कि आर्याई सोच को तसव्वुफ से स्वाभाविक लगाव है। तसव्वुफ़ की उत्पत्ति और विकास से अरबों से कहीं ज्यादा ईरानियों ने हिस्सा लिया। हिन्दुस्तान तो अंतःकरण का गहवारा रहा है, अतः जब इस्लामी तसव्वुफ हिन्दुस्तान पहुंचा तो यहां के लोगों को उसमें आध्यात्मिक आस्था की झलक पहचानने में देर न लगी। यूं तो तसव्वुफ मुसलमानों के साथ इस्लामी शहरों के हर हिस्से में बीसियों मुल्कों में गया लेकिन उसे जो लोकप्रियता और प्रसिद्धि हिन्दुस्तान में नसीब हुई उसका उदाहरण कहीं और नहीं मिलता है। लगता है जब दो मिलते-जुलते विचारों का आमना-सामना हुआ तो दोनों को एक दूसरे को पहचानने में देर न लगी और भक्ति आंदोलन, सुन्नत मत, सूफ़ीवाद आग की तरह देखते ही देखते उन विचारों को पूरे हिन्दुस्तान में फैला दिया।
सातवीं सदी ईस्वी में जब हिन्दु धर्म का साबिका इस्लाम से हुआ तो उसकी मूल आत्मा परम्पराओं और रूढ़ियों में धुंध में छुपकर जनसाधारण की नज़रों से गायब थी और विभिन्न समुदायों की आस्थाओं से असम्बद्धता और अज्ञानता पायी जाती थी। इसके विपरीत इस्लाम अपने साथ मज़हब का एक जांरबव्श और जीता जागता विचार लाया था जो ऊंच-नीच के भेदभाव और सत्ता से मुक्त था। इस्लाम गहरा मज़हबी एहसास रखता था और उसके धार्मिक सिद्धांत भी सीधे सादे थे, अतः हिन्दुओं की एक बड़ी संख्या उसकी तरफ खिंचने लगी। उधर ज़िंदा रहने के लिए नैसर्गिक इच्छा के अधीन हिन्दूधर्म में भी सुधान व नवीनीकरण का जोश व ख़रोश पैदा हुआ और इस्लाम की तरह गहरी धार्मिक भावना और धार्मिक एकता पर ज़ोर दिया जाने लगा। दक्षिण भारत में ही आठवी सदी ईस्वी के अन्त में शंकराचार्य ने अपनी उत्कृष्ट व्याख्या से हिन्दुओं के समस्त दार्शनिक सिद्धांतों और धार्मिक आस्थाओं को एक ही चिंतन व दर्शन से सम्मिलित करने के साथ अद्वैत नाम से एक ऐसी टीका लिखी जिसमें हिन्दुस्तानियों के तरीके मारीफत की रूह जलवहगर हो गयी। इसके अलावा भक्ति आन्दोलन भी जो शुरु में सूफी और भक्ति कवियों की नीजी हृदय संबंधी घटनाओं से थी, रामानुज के दर्शन के रूप में पूर्णता को पहुंच कर देश के विस्तृत क्षेत्र में लोकप्रिय होने लगी।
उत्तर भारत में भक्ति जो वैष्णव मत के रूप में राजपूत रियासतों में पहले ही मौजूद थी, तेरहवीं सदी ईस्वी के आरम्भ में मुसलमानों की सत्ता स्थापित होने के बाद तेज़ी से लोकप्रिय होने लगी। ग्याहरवीं सदी में रामानुज ने भक्ति को पूर्ण रूप से एक मज़हब की हैसियत दे दी। रामानुज ने भी एकेश्वरवाद के सिद्धांत के आधार वेदांत पर रखा लेकिन उसकी व्याख्या इस तरह की भक्ति के उन रूझानों के लिए गुंजाइश निकल आयी जो इस्लाम से मेल जोल के बाद और गहरे हो गये थे।
रामानुज के अलावा भक्ति परम्परा को आगे बढ़ाने में माधव और निम्बार्क ने भी अहम हिस्सा लिया। भक्ति को दक्षिण की अपेक्षा उत्तर भारत में अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। इसका एक कारण तो ये था कि वहां भक्ति की आस्था वैष्णव मत में पहले से थी और दूसरे ये कि हिन्दुओं और मुसलमानों का मेल-मिलाप दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर में कहीं ज्यादा भरपूर और परिपूर्ण था। उत्तर भारत में भक्ति के विकास को बाकायदा रामानन्द से सम्बद्ध किया जाता है। ये रामानुज के आध्यात्मिक श्रृंखला के चौथे भक्त थे। रामानन्द के ज़माने से भक्ति आंदोलन के दो अलग-अलग धारे नज़र आते हैं, एक पुरातनपंथियों का और दूसरा प्रगतिवादी भक्तों का। पहले के अगुवा तुलसीदास है और दूसरे के कबीर। दोनों ही रामानन्द के शिष्य थे। तुलसी ने रामचरित मानस की रचना कर हिन्दुओ और मुसलमानों को इतना करीब कर दिया कि उन दोनों की साझेदारी से सांस्कृतिक मेल-जोल का एक नया अध्याय शुरु हुआ।
रामानन्द से पहले महाराष्ट्र में संत नामदेव (1270-1350) के द्वारा कृष्ण भक्ति का आन्दोलन आरम्भ हो चुका था। बाद में बंगाल के एक और भक्त में संत नामदेव (1456-1524) ने भी श्री कृष्ण को भक्ति का माध्यम बनाकर नृत्य व गायन पर बल देते हुए ईश्वर के ज्ञान का माध्यम बनाया।
हिन्दुओं के अतिरिक्त मुसलमानों के एक वर्ग ने भी जो शासक वर्ग से ही नहीं संसार और सांसारिक माया से भी दूर था, इस्लाम के अक़ीदए तौहीद (एकेश्वरवाद) को हिन्दुओं के सामने वदहतुल वजूद के रंग में पेश किया। आम हिन्दुओं को उसमें अपने वेदांत के सिद्धांत की झलक नज़र आयी, इसके अतिरिक्त इस्लाम के सशक्त लोकतांत्रिक सिद्धांत और आर्थिक समानता ने भी उन्हें प्रभावित किया और उनमें थोड़े बहुत मुसलमान भी हुए लेकिन ज्यादातर अपने धर्म पर कायम रहते हुए इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों से भयभीत होने के बजाय उनके पास आने लगे।
एक ऐसे मुल्क में जहां दो मज़हब ही नहीं, एक ही मज़हब के दो या अधिक वैचारिक सिद्धांतों में भी टकराव के कारण मौजूद रहे हैं, प्रेम व सद्भाव का वातारण पैदा करना मामूली काम नहीं था, मगर सूफियों ने यह मुश्किल काम बड़ी आसानी से पूरा कर लिया। खास तौर से उन सूफियों ने जिन्होंने जनसाधारण की बोलियों में जनसाधारण को जागृत करते और अपने मीठे बोल से मुर्दा दिलों में नयी ज़िंदगी दौड़ाने का काम किया। वे साहिबे दिल तो थे ही, उनमें अधिकतर शाइर हिन्दुस्तानी और फ़ारसी की साझा काव्य परम्परा के संरक्षक भी थे।
कबीर ने सूफियों से गहरा असर कबूल किया था, वे कहते हैः
कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाय
वा चढ़ मुल्ला बांग दे का बहरा भयो खुदाय
यद्यपि कबीर कभी,
निर्गुण आगे सरगुण नाचे बाजे सोहंग तोरा
और कभी
निराकार निर्गुण अबनासी, करवाही को संग
का नारए मस्ताना लगाते हुए निर्गुण भक्ति का राग या एक ईश्वर की मुहब्बत का नग़म-ए-दिलनवाज बुलंद करते रहे, मगर गुरु और गोविंद में गुरु को प्राथमिकता और गुरु भक्ति को वहदानियत का आधार घोषित कर कह उठे,
गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाय
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय
उन्हीं से मंसुब एक और दोहाः
ला इलाह का ताना इल्लल्लाह का बाना
दास कबीर बटने को बैठा उलझा सूत पुराना
इसलिए नतीजा यही निकलता है कि कबीर ने सूफियों से गहरा असर कबूल किया था। डॉ. ताराचन्द का कथन है कि कबीर ने सृष्टि के उद्गम का जो सिद्धांत रामायणी में प्रस्तुत किया है बदरुद्दीन शहीद और अब्दुल करीम जेली की आस्थाओं से मिलता जुलता है। कबीर भी सत्य के ज्ञान की मंजिल तक पहुंचने के लिए मुसलमान सूफियों की तरह विभिन्न हालतों से गुज़रना ज़रूरी समझते हैं। कबीर ने अपने इन मिले जुले नज़रियात की मदद से हिन्दु धर्म और इस्लाम की अस्ल रुह को बेनकाब किया और एक ऐसी साझी राह का संकेत दिया जो उस मंज़िल को ले जाती है जहां काबा और काशी या राम और रहीम की कल्पनाओं में भेद नहीं रहता।
उत्तर भारत में भक्ति के दूसरे बड़े अलमबरदार गुरुनानक को माना जाता है। उन्होंने भी कबीर की तरह हिन्दुओ और मुसलमानों के आन्तरिक आस्था को समोकर मज़हब की अस्ल रुह को अवाम तक पहुंचाने की कोशिश की। कबीर की तरह नानक मज़हब के आध्यात्मिक पहलू पर उतना नहीं जितना नैतिक और व्यवहारिक पहलू पर ज़ोर देते हैं।
सूफ़ियों और भक्तों का सारा ध्यान प्रेम पर रहा है और मौलाना रूमी के नज़दीक दीन का जौहर ही इश्क़ है। यही नहीं शेख़ अकबर मुहिउद्दीन इब्न अल अरबी के अनुसारः
“मेरा दिल हर एक रूप से लगाव रखता है, वह
चरागाह है हिरनों के लिए, ख़ानकाह है ईसाई
राहिबों के लिए, मन्दिर है बुतों के लिए, काबा
है हज का सफ़र करने वालों के लिए, और
तख़्ती है तौरेत की, मुसहफ है कुरान का, मैं
मज़हबे इश्क़ का पैरू हूं, ख्वाह किसी रास्ते
पर इसका किनारा मुझे ले जाये मेरा मज़हब
और मेरा अकीदा एक सच्चा मज़हब है।”
वजही
ताकत नहीं दूरी की अब तो बेगी आ मिल रे पिया
तुज बिन मंजे जीना बहोत होता है मुश्किल रे पिया
मुहम्मद क़ुली क़ुतुब शाह
पिया बाज प्याला पिया जाये ना
पिया बाज यक तिल जिया जाये ना !
कहते हैं कि हिन्दुस्तान की धरती जिसके कण कण से संगीत फूटता है, अत्तार व रूमी की सूफ़ियाना चिंतन के लिए बड़ी उपजाऊ साबित हुई, ख़ास तौर से उत्तर भारत में। सूफियों की काव्य रचना का मूल शब्द ‘प्रेम’ है। उन्होंने अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और लोक कथाओं के मूल पात्रों के प्रेम (कृत्रिम) के माध्यम से वास्तविक प्रेम की सीख दी है। उनके समस्त इश्किया दास्तानों में ईश्वर प्रेमिका (माशूक़) और बटोही आशिक है । आशिक को माशूक का सुराग लगता है और वह उससे मिलने के लिए इश्क की पगडण्डी पर चल पड़ता है। हालांकि राह में तरह तरह की मुश्किलें और मुसीबतें रुकावटे खड़ी होती हैं । अंततः सारी रुकावटें दूर हो जाती है और वह ज्ञान और सत्य की मंज़िल पा लेता है।
इश्क़ की मंज़िल में तरीक़त सिर्फ इज़हार है। इस इज़ाहर की शिद्दत में इश्क़ हकीक़ी का कुछ पहलू छुपा होता है। इससे रू-ब-रू होने की चाहत ही वह कैफियत है, जिसे किसी शायर ने ‘हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे’ के तौर पर बयां किया है।
अमीर खुसरों ने इश्क में तरीक़त की पहली पायदान को ‘छाप तिलक सब छीनी रे मो से नयना मिलायके’ से बयान किया। राबिया बसरी ने इसी तरीक़त को बयान करने के लिए लोगों से सवाल किया कि तुम में से कौन है, जिसके ज़ेहन में सिर्फ एक मुहब्बत का ख़्याल है। लोगों ने उनसे सावल किया कि आपने शादी नहीं की, फिर आपको मुहब्बत का इल्म कैसे हुआ। राबिया ने कहा कि मैंने अल्लाह से मुहब्बत कर ली है। लोगों ने फिर भी न छोड़ा और पूछा कि क्या आपको शैतान से नफ़रत है? राबिया ने कहा कि जिस के दिल में किसी के लिए मौहब्बत पैदा हो गई हो, वह भला किसी से भी नफ़रत कैसे कर सकता है।
सूफीज़्म का दर्शन कहता है कि कुछ लोग दुनिया के लिए मरते हैं और कुछ आख़िरत के लिए। मगर जो लोग मुहब्बत करते हैं, वे सिर्फ जीते है, कभी मरते नहीं।
मलिक मुहम्मद जायसी इश्क़िया दास्तान बयान करने वाले सबसे अहम कवि है। जायसी की भाषा अवधि है और उसमें कहीं कहीं अरबी-फारसी शब्दों का प्रयोग भी हुआ है किंतु प्रभावशाली रंग हिन्दुस्तानी है। उनकी पद्मावत का रचना काल 1530-1540 है। इससे पूर्व कुत्बन की मृगावती (1501), मंझन की मधुमालती (1493-1538) और बाद में उस्मान की चित्रावली (1631) और नूर मुहम्मद की इन्द्रावती (1744) इसी रंग और मिज़ाज की कविता का नमूना है।
साहिब सर शाह मुहम्मद काज़िम कलन्दर (1745-1857) और उनके पुत्र व वारिस शाह तुराब अळी कलन्दर (1768-1857) ने अठारहवीं सदी ईस्वी में अध्यात्म की वह जोत जलायी कि जिसकी तपिश ने हज़ारों मुर्दा दिलों में जान डाल दी। साहिब सर शाह मुहम्मद काजिम कलन्दर के बृज भाषा के कलाम का संग्रह ‘शांतरस’ की हज़रत मौलाना शाह हाफिज़ मुज्तबा हैदर कलन्दर ने उर्दू में जो टीका लिखी वह खुद उत्कृष्ट साहित्य का एक नमूना है। उसे पढ़ने से एक आम आदमी भी समझ सकता है कि शुद्ध भारतीय शब्दावलियों के बावजूद उन शेरों में कोई एक बार भी गैर इस्लामी नहीं है। इसके बावजूद हिन्दुस्तान की अवामी और कृष्ण भक्ति परम्परा से पूरी तरह हम आहगं है।
कृष्ण जी की सुरीली बांसुरी की तानों ने गोपियों के धैर्य व सहनशीलता को जलाकर फूंक डाला था, वृंदावन और गोकुल के जंगलों में वह शोखी व शरारत से मासूम व सादा गोपियों के दिलों में इश्क के शरारे भड़का रहे थे। कभी पनघट से वापस आते हुए अपने निर्भीक प्रदर्शन से उन्हें बेखुद करते, कभी उनके साथ होली खेलते और उनकी चुनरी शराबोर कर देते, फिर एक वक्त आया कि वृंदावन से द्वारका चले गये और हर प्रकार के बंधनों और आवश्यकताओं से मुख मोड़ लिया। इस विरह के संताप ने दिलों में जो आग लगायी है उसका वर्णन इस ढंग से किया है कि मालूम होता है कि कोई जला हुआ दिल आर्तनाद में व्यस्त हैः
मनमोहन हो कहां जाय बसे
केल करत रहे जो उन कुंजन
बिछुड़े फिर न मिले दरसन
धीरे-धीरे मन बिरहन को कब
हुए बिछुड़े बरसन बरसन
बहुत दिन उनके संग खेले
जिव सुख पायो रघुबर बरसन
मधुबन दिखे जरूहिया हमरो
रक्त लगे आंखें बरसन
शाह मुहम्मद काज़िम कलन्दर को बजा तौर पर ‘साहिबे सर’ कहा गया है। आपने भलाई के राह में बड़ी कठोर तपस्या की और मुर्शिद की तवज्जोह से उच्च स्थान पर स्थापित हुए। आपने तसव्वुफ के नाजुक मसअलों को पानी की तरह हल कर दिया है। देखिये वहदतुल वजुद के मस्अले को कितने सुन्दर ढंग से हल किया हैः
घर बाहर अब वही है ‘काज़िम’
हम नांहि हम नांहि हम नांहि
अपने पीतम संग मिलके होय गये वाके रंग
हम वा के वो हमरे रंग मिल दोऊ भये एके रंग
सृष्टि की उलझनों से यकसू हो कर आशिक़ उस स्थान पर पहुंचता है जहां दुख का शूल, सुख का अमृत, मिलन का स्वाद और विरह का संताप सब घुल मिल जाते हैं तो वह सत्य को सत्य की दृष्टि से देखता है, जहां अच्छाई और बुराई एक ही तस्वीर के दो रुख दिखाई देते हैं, हर्ष व उन्माद की आख़िरी मंज़िल यही है, यहां पहुंच कर इंसान पूर्ण हो जाता हैः
कौन करे अब हमरे तीरथ को तिरबेनी काशी जाय
ठौर ठौर दरसन है हमका इस बिन आयो ढंग
शाह तुराब अली क़लन्दर का ब्रजभाषा का कलाम भी जिसका एक भाग ‘अमृत रस’ के नाम से प्रकाशित हो चुका है, का एक शे’र हैः
किस मुब्तला की हाय मुझे बद्दुओ लगी
उस शोख़े चश्म से जो मेरी आंख जा लगी
इस सिलसिले में वाकया ये है कि आरम्भिक अवस्था में वालिदे मोहतरम से इश्क़ व मस्ती और गीत गायन के संदर्भ में आपत्ति की कोई बात निकल गयी थी जिसे सुनकर साहिब सर शाह मुहम्मद काज़िम क़लन्दर ने मुस्कराकर फ़रमायाः
जब लिखीये तब जनिहे
पिताश्री के इस वाक्य ने उनकी दुनिया ही बदल दी और उसके बाद क्या उर्दू-फ़ारसी में और क्या ब्रजभाषा में आपके मुख से निकला हुआ कलाम यानी उनकी पूरी शे’री कायनात सोज़ व तड़प के लाफ़ानी रंग में इस तरह रंग गयी कि आज जो भी पढ़ता या सुनता, तड़प उठता हैः
होरी खेलत है श्याम बिहारी
हाथ मलत है राधा गोरी
देखे जरत हों न देखे मरत हो
ब्रज में का इक हमही बसत है
एक से तोड़े एक से जोड़े
आपके पिता श्री शाह मुहम्मद काज़िम क़लन्दर जिनसे आपको इश्के हक़ीकी को शुद्ध हिन्दुस्तानी रंग में पेश करने का गुण मिला, के कलाम में संगीत की कई शब्दावलियों का प्रयोग भी हुआ है, जैसे दादरा, सोरठ, शहाना, कहरा आदि।


मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने जो खुद भी विद्वान और साहिबे दीवान शायर थे, ‘मुस्तलहाते दीवाने हाफिज़’ के अलावा फ़ारसी में ‘हक़ाइके हिन्दी’ के नाम से हिन्दी कविताओं और गीतों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की विद्वतापूर्ण व्याख्या करके इस परम्परा का आरम्भ किया था। सैयद शाह बरकतुल्लाह मारहरवी, अरबी, फ़ारसी के अतिरिक्त स्थानीय बोली में भी शे’र कहते थे, यह स्थानीय बोली ब्रजभाषा है। मगर उसका संजीदगी से अध्ययन करने पर यह राज खुलता है कि उसमें अवधी, पांचाली और बुन्देली बोलियों के प्रभाव भी है। इसका कारण ये है कि आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा मारहरा में गुज़रा जिसके आम बोलचाल की भाषा ब्रजभाषा थी लेकिन आप बिलग्राम (अवध) में भी रहे है। इसलिए उन क्षेत्रों की भाषाओं के प्रभाव भी आपकी शायरी पर दिखता है। ‘प्रेम प्रकाश’ आपके हिंदी कलाम का संग्रह है।
हमारे समाज और संस्कृति को कई सदियों में ऋषियों-मुनियों और सूफियों-मुर्शीदों ने पोसा। प्रेम और मुहब्बत का पैग़ाम दिया है। हालात के तमाम उतार-चढ़ाव के बावजदू प्रेम और मुहब्बत की हमारी परम्परा क़ायम है। इश्क़ की इसी परम्परा को एक शायर ने कुछ यूं आवाज़ दी हैः
काबे से, बुतकदे से,
कभी बज़्मे-यार से,
आवाज़ दे रहा हूँ तुझे
हर मुक़ाम से।।
Guest Authors
- Aatif Kazmi
- Absar Balkhi
- Afzal Muhammad Farooqui Safvi
- Ahmad Raza Ashrafi
- Ahmer Raza
- Akhlaque Ahan
- Arun Prakash Ray
- Balram Shukla
- Dr. Kabeeruddin Khan Warsi
- Faiz Ali Shah
- Farhat Ehsas
- Iltefat Amjadi
- Jabir Khan Warsi
- Junaid Ahmad Noor
- Kaleem Athar
- Khursheed Alam
- Mazhar Farid
- Meher Murshed
- Mustaquim Pervez
- Qurban Ali
- Raiyan Abulolai
- Rekha Pande
- Saabir Raza Rahbar Misbahi
- Shamim Tariq
- Sharid Ansari
- Shashi Tandon
- Sufinama Archive
- Syed Ali Nadeem Rezavi
- Syed Moin Alvi
- Syed Rizwanullah Wahidi
- Syed Shah Shamimuddin Ahmad Munemi
- Syed Shah Tariq Enayatullah Firdausi
- Umair Husami
- Yusuf Shahab
- Zafarullah Ansari
- Zunnoorain Alavi